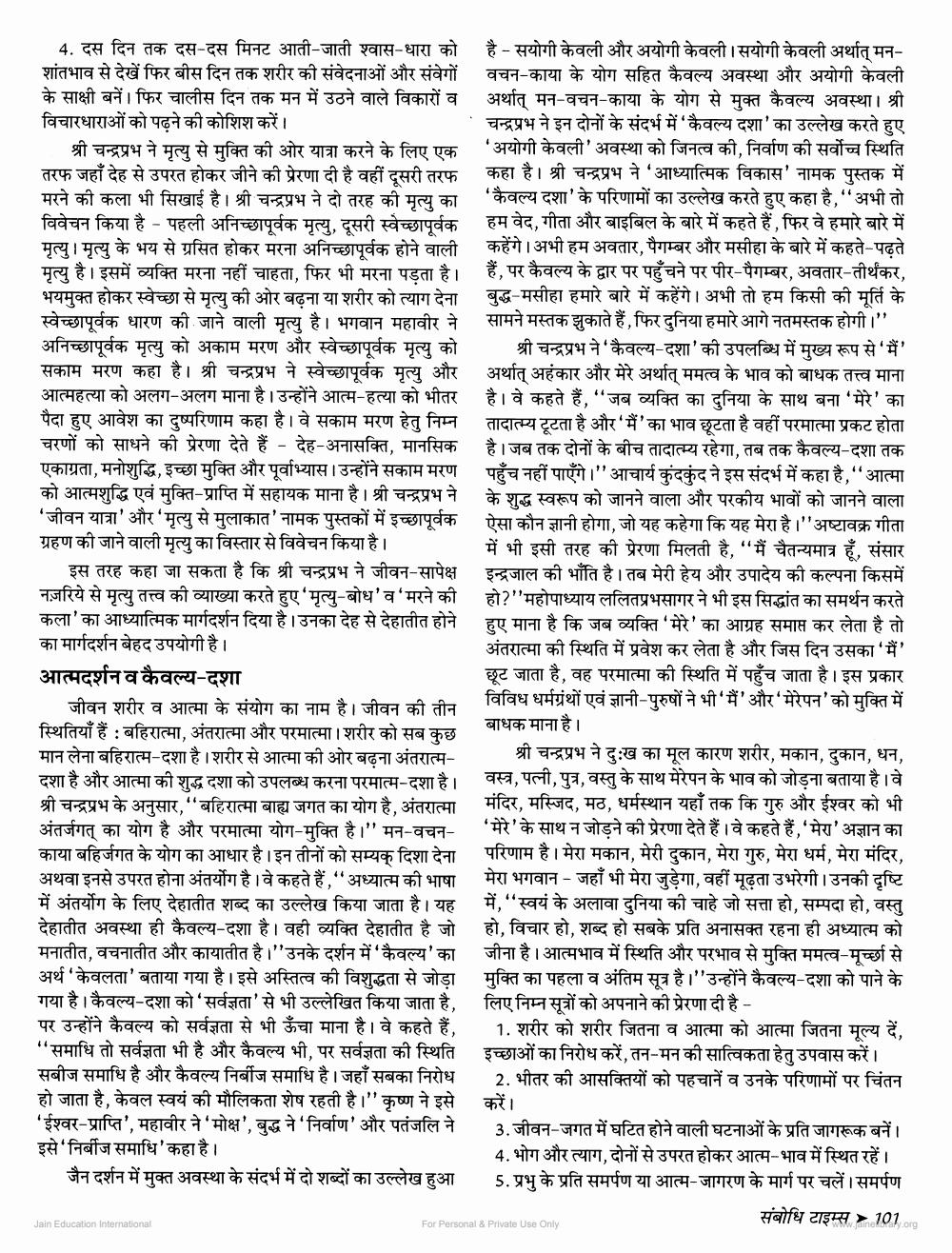________________
4. दस दिन तक दस-दस मिनट आती-जाती श्वास-धारा को है-सयोगी केवली और अयोगी केवली।सयोगी केवली अर्थात् मनशांतभाव से देखें फिर बीस दिन तक शरीर की संवेदनाओं और संवेगों वचन-काया के योग सहित कैवल्य अवस्था और अयोगी केवली के साक्षी बनें। फिर चालीस दिन तक मन में उठने वाले विकारों व अर्थात् मन-वचन-काया के योग से मुक्त कैवल्य अवस्था। श्री विचारधाराओं को पढ़ने की कोशिश करें।।
' चन्द्रप्रभ ने इन दोनों के संदर्भ में कैवल्य दशा' का उल्लेख करते हुए श्री चन्द्रप्रभ ने मृत्यु से मुक्ति की ओर यात्रा करने के लिए एक 'अयोगी केवली' अवस्था को जिनत्व की, निर्वाण की सर्वोच्च स्थिति तरफ जहाँ देह से उपरत होकर जीने की प्रेरणा दी है वहीं दूसरी तरफ कहा है। श्री चन्द्रप्रभ ने 'आध्यात्मिक विकास' नामक पुस्तक में मरने की कला भी सिखाई है। श्री चन्द्रप्रभ ने दो तरह की मृत्यु का 'कैवल्य दशा' के परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा है, "अभी तो विवेचन किया है - पहली अनिच्छापर्वक मत्य. दसरी स्वेच्छापर्वक हम वेद, गीता और बाइबिल के बारे में कहते हैं, फिर वे हमारे बारे में मृत्यु। मृत्यु के भय से ग्रसित होकर मरना अनिच्छापूर्वक होने वाली कहेंगे। अभी हम अवतार, पैगम्बर और मसीहा के बारे में कहते-पढ़ते मृत्यु है। इसमें व्यक्ति मरना नहीं चाहता, फिर भी मरना पड़ता है। हैं, पर कैवल्य के द्वार पर पहुँचने पर पीर-पैगम्बर, अवतार-तीर्थंकर, भयमक्त होकर स्वेच्छा से मत्य की ओर बढना या शरीर को त्याग देना बुद्ध-मसीहा हमारे बारे में कहेंगे। अभी तो हम किसी की मर्ति के स्वेच्छापूर्वक धारण की जाने वाली मृत्यु है। भगवान महावीर ने सामने मस्तक झुकाते हैं, फिर दुनिया हमारे आगे नतमस्तक होगी।" अनिच्छापूर्वक मृत्यु को अकाम मरण और स्वेच्छापूर्वक मृत्यु को श्री चन्द्रप्रभ ने कैवल्य-दशा' की उपलब्धि में मुख्य रूप से 'मैं' सकाम मरण कहा है। श्री चन्द्रप्रभ ने स्वेच्छापूर्वक मृत्यु और अर्थात् अहंकार और मेरे अर्थात् ममत्व के भाव को बाधक तत्त्व माना आत्महत्या को अलग-अलग माना है। उन्होंने आत्म-हत्या को भीतर है। वे कहते हैं, "जब व्यक्ति का दुनिया के साथ बना 'मेरे' का पैदा हुए आवेश का दुष्परिणाम कहा है। वे सकाम मरण हेतु निम्न तादात्म्य टूटता है और 'मैं' का भाव छूटता है वहीं परमात्मा प्रकट होता चरणों को साधने की प्रेरणा देते हैं - देह-अनासक्ति, मानसिक है। जब तक दोनों के बीच तादात्म्य रहेगा, तब तक कैवल्य-दशा तक एकाग्रता, मनोशुद्धि, इच्छा मुक्ति और पूर्वाभ्यास। उन्होंने सकाम मरण पहँच नहीं पाएँगे।" आचार्य कुंदकुंद ने इस संदर्भ में कहा है, "आत्मा को आत्मशुद्धि एवं मुक्ति-प्राप्ति में सहायक माना है। श्री चन्द्रप्रभ ने के शद्ध स्वरूप को जानने वाला और परकीय भावों को जानने वाला 'जीवन यात्रा' और 'मृत्यु से मुलाकात' नामक पुस्तकों में इच्छापूर्वक ऐसा कौन ज्ञानी होगा. जो यह कहेगा कि यह मेरा है।"अष्टावक्र गीता ग्रहण की जाने वाली मृत्यु का विस्तार से विवेचन किया है।
में भी इसी तरह की प्रेरणा मिलती है, "मैं चैतन्यमात्र हूँ, संसार इस तरह कहा जा सकता है कि श्री चन्द्रप्रभ ने जीवन-सापेक्ष इन्द्रजाल की भाँति है। तब मेरी हेय और उपादेय की कल्पना किसमें नज़रिये से मृत्यु तत्त्व की व्याख्या करते हुए मृत्यु-बोध' व 'मरने की । हो?"महोपाध्याय ललितप्रभसागर ने भी इस सिद्धांत का समर्थन करते कला' का आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया है। उनका देह से देहातीत होने हुए माना है कि जब व्यक्ति 'मेरे' का आग्रह समाप्त कर लेता है तो का मार्गदर्शन बेहद उपयोगी है।
अंतरात्मा की स्थिति में प्रवेश कर लेता है और जिस दिन उसका 'मैं' आत्मदर्शनवकैवल्य-दशा
छूट जाता है, वह परमात्मा की स्थिति में पहुँच जाता है। इस प्रकार जीवन शरीर व आत्मा के संयोग का नाम है। जीवन की तीन
विविध धर्मग्रंथों एवं ज्ञानी-पुरुषों ने भी 'मैं' और 'मेरेपन' को मुक्ति में स्थितियाँ हैं : बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। शरीर को सब कुछ
बाधक माना है। मान लेना बहिरात्म-दशा है। शरीर से आत्मा की ओर बढ़ना अंतरात्म
श्री चन्द्रप्रभ ने दु:ख का मूल कारण शरीर, मकान, दुकान, धन, दशा है और आत्मा की शद्ध दशा को उपलब्ध करना परमात्म-दशा है। वस्त्र, पत्नी, पुत्र, वस्तु के साथ मेरेपन के भाव को जोड़ना बताया है। वे श्री चन्द्रप्रभ के अनुसार, "बहिरात्मा बाह्य जगत का योग है, अंतरात्मा मंदिर, मस्जिद, मठ, धर्मस्थान यहाँ तक कि गुरु और ईश्वर को भी अंतर्जगत् का योग है और परमात्मा योग-मुक्ति है।" मन-वचन- 'मेरे' के साथ न जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, 'मेरा' अज्ञान का काया बहिर्जगत के योग का आधार है। इन तीनों को सम्यक दिशा देना परिणाम है। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा गुरु, मेरा धर्म, मेरा मंदिर, अथवा इनसे उपरत होना अंतर्योग है। वे कहते हैं, "अध्यात्म की भाषा मेरा भगवान - जहाँ भी मेरा जुड़ेगा, वहीं मूढ़ता उभरेगी। उनकी दृष्टि में अंतर्योग के लिए देहातीत शब्द का उल्लेख किया जाता है। यह में, "स्वयं के अलावा दुनिया की चाहे जो सत्ता हो, सम्पदा हो, वस्तु देहातीत अवस्था ही कैवल्य-दशा है। वही व्यक्ति देहातीत है जो हो, विचार हो, शब्द हो सबके प्रति अनासक्त रहना ही अध्यात्म को मनातीत, वचनातीत और कायातीत है।"उनके दर्शन में कैवल्य' का जीना है। आत्मभाव में स्थिति और परभाव से मुक्ति ममत्व-मूर्छा से अर्थ 'केवलता' बताया गया है। इसे अस्तित्व की विशुद्धता से जोड़ा मुक्ति का पहला व अंतिम सूत्र है।" उन्होंने कैवल्य-दशा को पाने के गया है। कैवल्य-दशा को 'सर्वज्ञता' से भी उल्लेखित किया जाता है, लिए निम्न सूत्रों को अपनाने की प्रेरणा दी है - पर उन्होंने कैवल्य को सर्वज्ञता से भी ऊँचा माना है। वे कहते हैं, 1. शरीर को शरीर जितना व आत्मा को आत्मा जितना मूल्य दें, "समाधि तो सर्वज्ञता भी है और कैवल्य भी, पर सर्वज्ञता की स्थिति इच्छाओं का निरोध करें,तन-मन की सात्विकता हेतु उपवास करें। सबीज समाधि है और कैवल्य निर्बीज समाधि है। जहाँ सबका निरोध 2. भीतर की आसक्तियों को पहचानें व उनके परिणामों पर चिंतन हो जाता है, केवल स्वयं की मौलिकता शेष रहती है।" कृष्ण ने इसे करें। 'ईश्वर-प्राप्ति', महावीर ने 'मोक्ष', बुद्ध ने 'निर्वाण' और पतंजलि ने 3.जीवन-जगत में घटित होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक बनें। इसे 'निर्बीज समाधि' कहा है।
4.भोग और त्याग, दोनों से उपरत होकर आत्म-भाव में स्थित रहें। जैन दर्शन में मुक्त अवस्था के संदर्भ में दो शब्दों का उल्लेख हुआ 5.प्रभु के प्रति समर्पण या आत्म-जागरण के मार्ग पर चलें। समर्पण
संबोधि टाइम्स > 101 Jain Education International
For Personal & Private Use Only