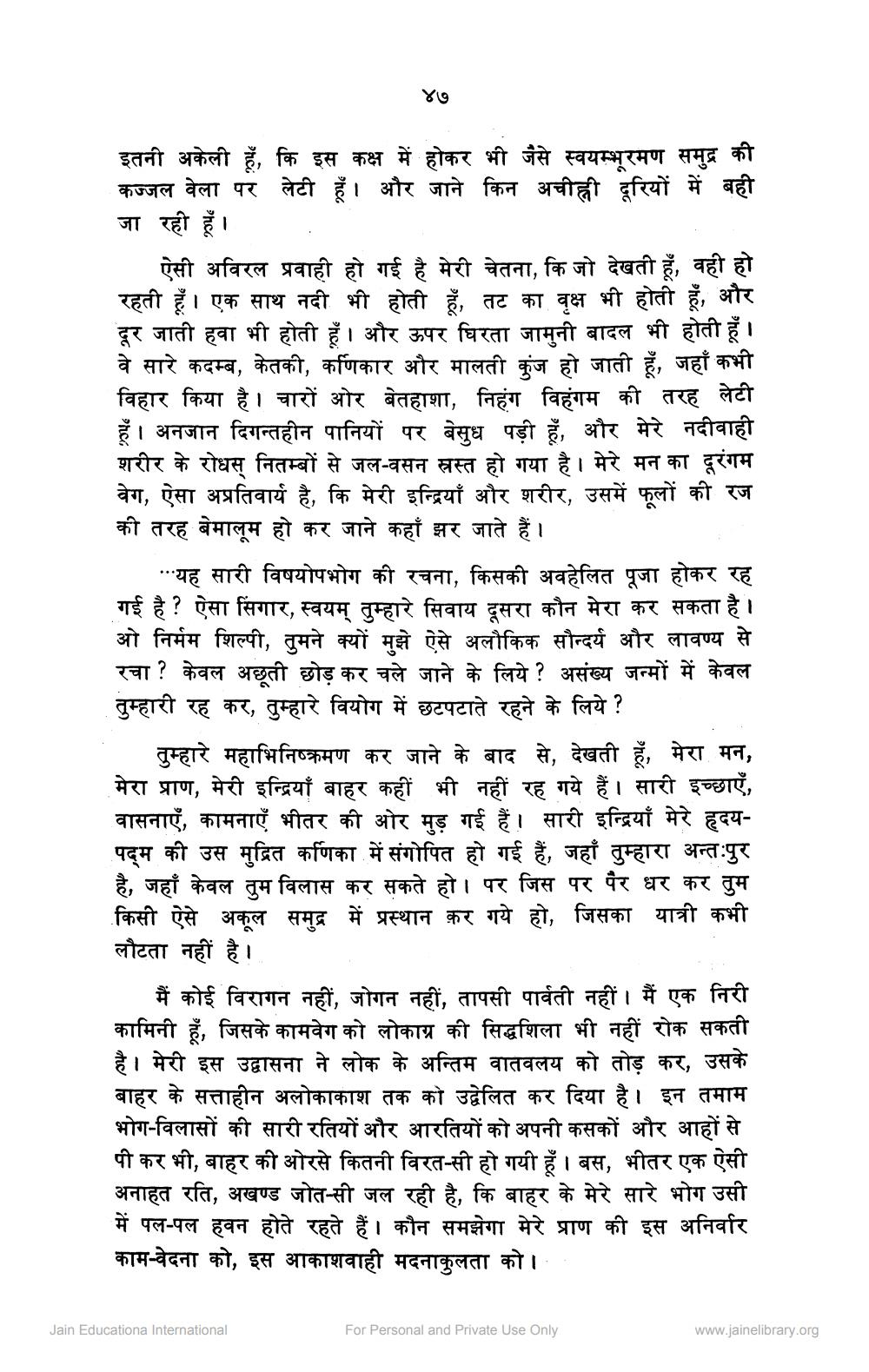________________
इतनी अकेली हूँ, कि इस कक्ष में होकर भी जैसे स्वयम्भरमण समुद्र की कज्जल वेला पर लेटी हूँ। और जाने किन अचीह्नी दूरियों में बही जा रही हूँ।
ऐसी अविरल प्रवाही हो गई है मेरी चेतना, कि जो देखती हूँ, वही हो रहती हूँ। एक साथ नदी भी होती हूँ, तट का वृक्ष भी होती हूँ, और दूर जाती हवा भी होती । और ऊपर घिरता जामुनी बादल भी होती हूँ। वे सारे कदम्ब, केतकी, कर्णिकार और मालती कुंज हो जाती हूँ, जहाँ कभी विहार किया है। चारों ओर बेतहाशा, निहंग विहंगम की तरह लेटी हूँ। अनजान दिगन्तहीन पानियों पर बेसुध पड़ी हूँ, और मेरे नदीवाही शरीर के रोधस् नितम्बों से जल-वसन स्रस्त हो गया है। मेरे मन का दूरंगम वेग, ऐसा अप्रतिवार्य है, कि मेरी इन्द्रियाँ और शरीर, उसमें फूलों की रज की तरह बेमालूम हो कर जाने कहाँ झर जाते हैं।
"यह सारी विषयोपभोग की रचना, किसकी अवहेलित पूजा होकर रह गई है ? ऐसा सिंगार, स्वयम् तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन मेरा कर सकता है। ओ निर्मम शिल्पी, तुमने क्यों मुझे ऐसे अलौकिक सौन्दर्य और लावण्य से रचा ? केवल अछूती छोड़ कर चले जाने के लिये ? असंख्य जन्मों में केवल तुम्हारी रह कर, तुम्हारे वियोग में छटपटाते रहने के लिये ?
तुम्हारे महाभिनिष्क्रमण कर जाने के बाद से, देखती हूँ, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरी इन्द्रियाँ बाहर कहीं भी नहीं रह गये हैं। सारी इच्छाएँ, वासनाएँ, कामनाएँ भीतर की ओर मुड़ गई हैं। सारी इन्द्रियाँ मेरे हृदयपद्म की उस मुद्रित कर्णिका में संगोपित हो गई हैं, जहाँ तुम्हारा अन्तःपुर है, जहाँ केवल तुम विलास कर सकते हो। पर जिस पर पैर धर कर तुम किसी ऐसे अकूल समुद्र में प्रस्थान कर गये हो, जिसका यात्री कभी लौटता नहीं है।
मैं कोई विरागन नहीं, जोगन नहीं, तापसी पार्वती नहीं। मैं एक निरी कामिनी हूँ, जिसके कामवेग को लोकाग्र की सिद्धशिला भी नहीं रोक सकती है। मेरी इस उद्वासना ने लोक के अन्तिम वातवलय को तोड़ कर, उसके बाहर के सत्ताहीन अलोकाकाश तक को उद्वेलित कर दिया है। इन तमाम भोग-विलासों की सारी रतियों और आरतियों को अपनी कसकों और आहों से पी कर भी, बाहर की ओरसे कितनी विरत-सी हो गयी हूँ। बस, भीतर एक ऐसी अनाहत रति, अखण्ड जोत-सी जल रही है, कि बाहर के मेरे सारे भोग उसी में पल-पल हवन होते रहते हैं। कौन समझेगा मेरे प्राण की इस अनिर्वार काम-वेदना को, इस आकाशवाही मदनाकुलता को।
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org