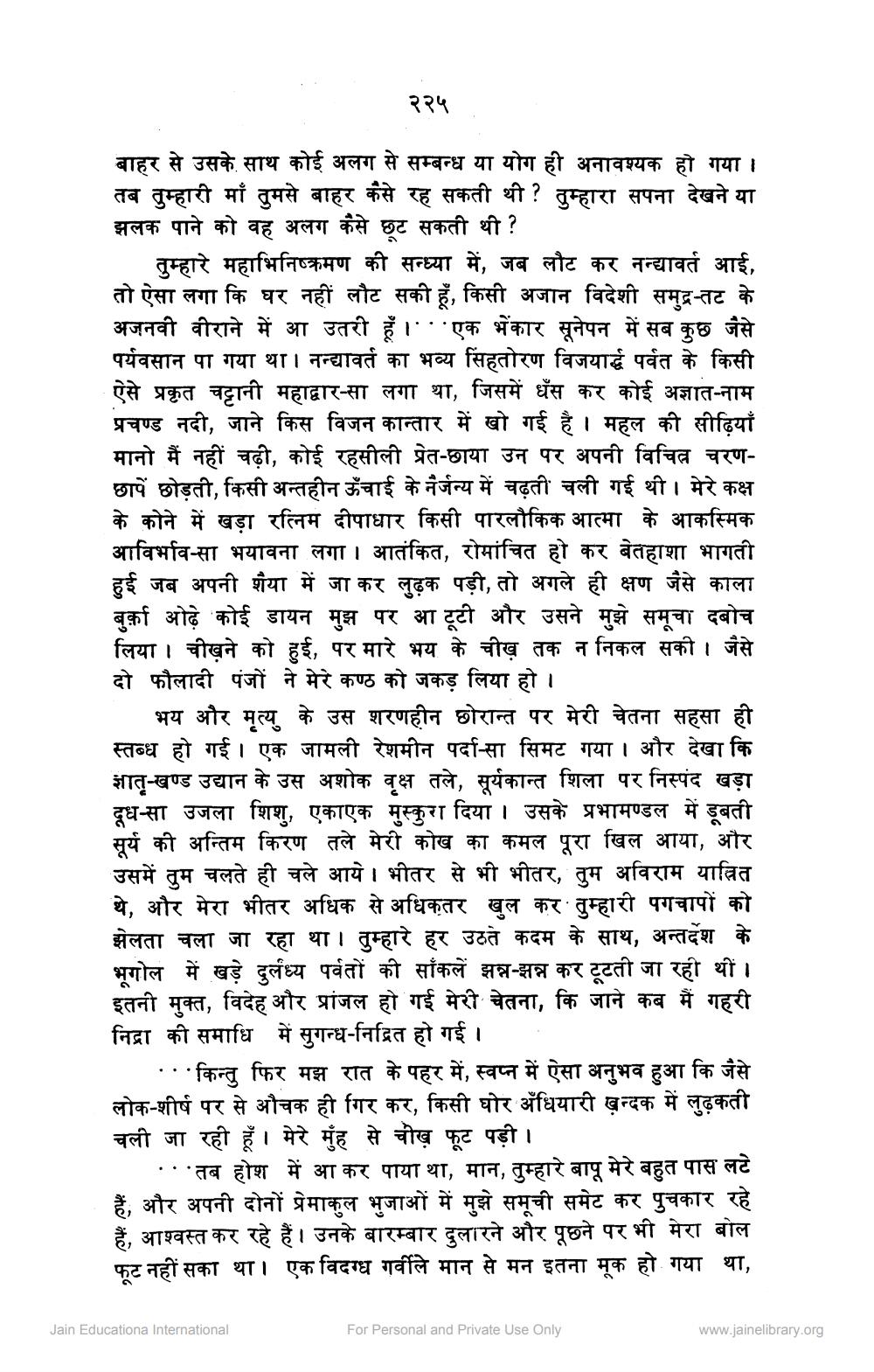________________
२२५
बाहर से उसके साथ कोई अलग से सम्बन्ध या योग ही अनावश्यक हो गया । तब तुम्हारी माँ तुमसे बाहर कैसे रह सकती थी ? तुम्हारा सपना देखने या झलक पाने को वह अलग कैसे छूट सकती थी ?
तुम्हारे महाभिनिष्क्रमण की सन्ध्या में, जब लौट कर नन्द्यावर्त आई, तो ऐसा लगा कि घर नहीं लौट सकी हूँ, किसी अजान विदेशी समुद्र-तट के अजनवी वीराने में आ उतरी हूँ । एक भेंकार सूनेपन में सब कुछ जैसे पर्यवसान पा गया था । नन्द्यावर्त का भव्य सिंहतोरण विजयार्द्ध पर्वत के किसी ऐसे प्रकृत चट्टानी महाद्वार-सा लगा था, जिसमें धँस कर कोई अज्ञात - नाम प्रचण्ड नदी, जाने किस विजन कान्तार में खो गई है । महल की सीढ़ियाँ मानो मैं नहीं चढ़ी, कोई रहसीली प्रेत-छाया उन पर अपनी विचित्र चरणछापें छोड़ती, किसी अन्तहीन ऊँचाई के नैर्जन्य में चढ़ती चली गई थी । मेरे कक्ष के कोने में खड़ा रत्निम दीपाधार किसी पारलौकिक आत्मा के आकस्मिक आविर्भाव-सा भयावना लगा । आतंकित, रोमांचित हो कर बेतहाशा भागती हुई जब अपनी शैया जाकर लुढ़क पड़ी, तो अगले ही क्षण जैसे काला बुर्का ओढ़े कोई डायन मुझ पर आ टूटी और उसने मुझे समूचा दबोच लिया । चीखने को हुई, पर मारे भय के चीख तक न निकल सकी । जैसे दो फौलादी पंजों ने मेरे कण्ठ को जकड़ लिया हो ।
भय और मृत्यु के उस शरणहीन छोरान्त पर मेरी चेतना सहसा ही स्तब्ध हो गई । एक जामली रेशमीन पर्दा-सा सिमट गया । और देखा कि ज्ञातृ-खण्ड उद्यान के उस अशोक वृक्ष तले, सूर्यकान्त शिला पर निस्पंद खड़ा दूध-सा उजला शिशु, एकाएक मुस्कुरा दिया । उसके प्रभामण्डल में डूबती सूर्य की अन्तिम किरण तले मेरी कोख का कमल पूरा खिल आया, और उसमें तुम चलते ही चले आये । भीतर से भी भीतर, तुम अविराम यात्रित थे, और मेरा भीतर अधिक से अधिकतर खुल कर तुम्हारी पगचापों को झेलता चला जा रहा था । तुम्हारे हर उठते कदम के साथ, अन्तर्देश के भूगोल में खड़े दुर्लध्य पर्वतों की साँकले झन्न झन्न कर टूटती जा रही थीं । इतनी मुक्त, विदेह और प्रांजल हो गई मेरी चेतना, कि जाने कब मैं गहरी निद्रा की समाधि में सुगन्ध-निद्रित हो गई ।
- किन्तु फिर मझ रात के पहर में, स्वप्न में ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे लोक-शीर्ष पर से औचक ही गिर कर किसी घोर अँधियारी ख़न्दक में लुढ़कती चली जा रही हूँ। मेरे मुँह से चीख फूट पड़ी।
"तब होश में आकर पाया था, मान, तुम्हारे बापू मेरे बहुत पास लटे हैं, और अपनी दोनों प्रेमाकुल भुजाओं में मुझे समूची समेट कर पुचकार रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं। उनके बारम्बार दुलारने और पूछने पर भी मेरा बोल फूट नहीं सका था । एक विदग्ध गर्वीले मान से मन इतना मूक हो गया था,
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org