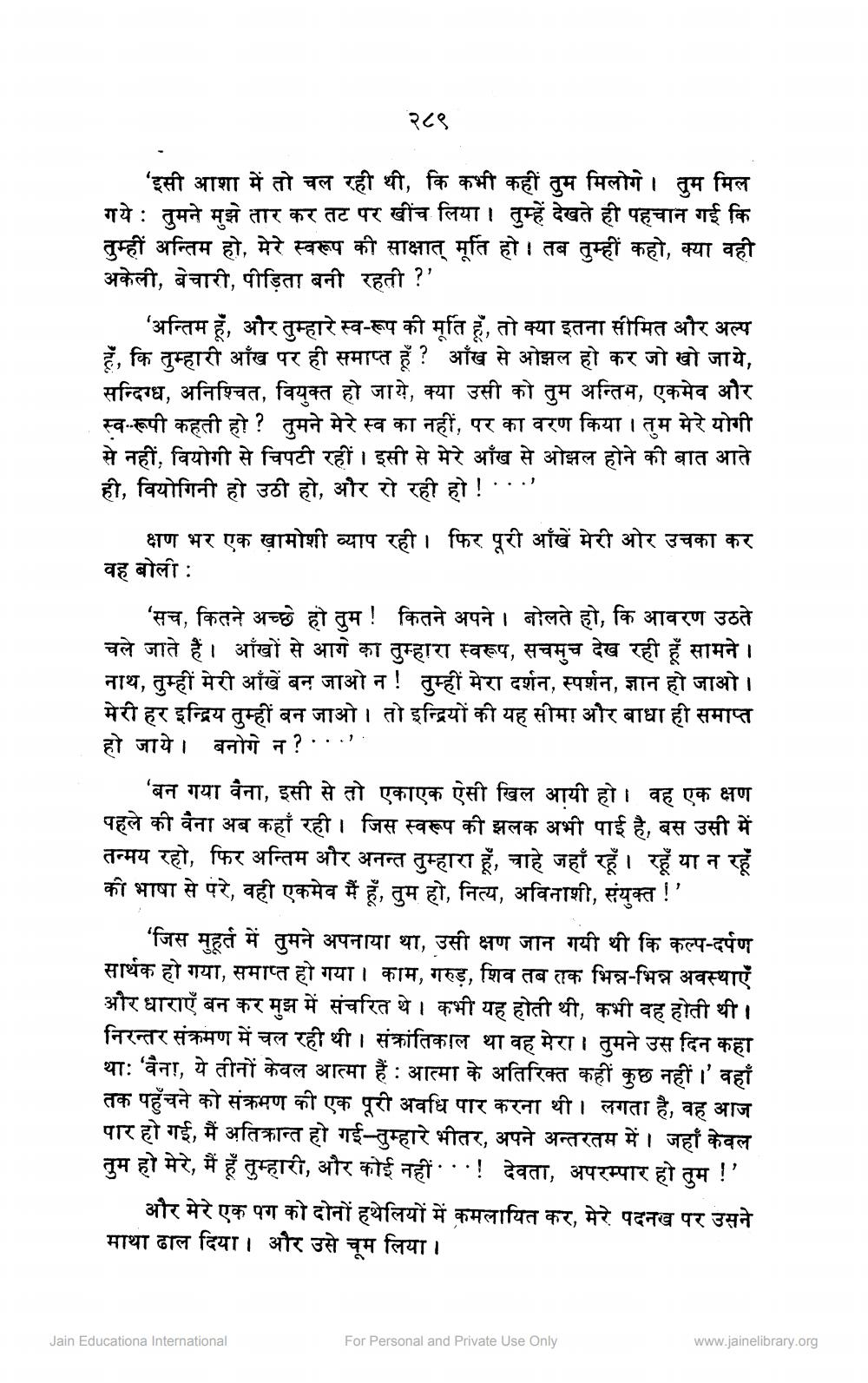________________
२८९
'इसी आशा में तो चल रही थी, कि कभी कहीं तुम मिलोगे। तुम मिल गये : तुमने मुझे तार कर तट पर खींच लिया । तुम्हें देखते ही पहचान गई कि तुम्हीं अन्तिम हो, मेरे स्वरूप की साक्षात् मूर्ति हो । तब तुम्हीं कहो, क्या वही अकेली, बेचारी, पीड़िता बनी रहती ?"
'अन्तिम हूँ, और तुम्हारे स्व-रूप की मूर्ति हूँ, तो क्या इतना सीमित और अल्प हूँ, कि तुम्हारी आँख पर ही समाप्त हूँ ? आँख से ओझल हो कर जो खो जाये, सन्दिग्ध, अनिश्चित, वियुक्त हो जाये, क्या उसी को तुम अन्तिम, एकमेव और स्व-रूपी कहती हो ? तुमने मेरे स्व का नहीं, पर का वरण किया । तुम मेरे योगी से नहीं, वियोगी से चिपटी रहीं । इसी से मेरे आँख से ओझल होने की बात आते ही, वियोगिनी हो उठी हो, और रो रही हो !
...)
क्षण भर एक ख़ामोशी व्याप रही। फिर पूरी आँखें मेरी ओर उचका कर वह बोली :
'सच, कितने अच्छे हो तुम ! कितने अपने । बोलते हो, कि आवरण उठते चले जाते हैं । आँखों से आगे का तुम्हारा स्वरूप, सचमुच देख रही हूँ सामने । नाथ, तुम्हीं मेरी आँखें बन जाओ न ! तुम्हीं मेरा दर्शन, स्पर्शन, ज्ञान हो जाओ । मेरी हर इन्द्रिय तुम्हीं बन जाओ । तो इन्द्रियों की यह सीमा और बाधा ही समाप्त हो जाये । बनोगे न
' बन गया वैना, इसी से तो एकाएक ऐसी खिल आयी हो। वह एक क्षण पहले की वैना अब कहाँ रही । जिस स्वरूप की झलक अभी पाई है, बस उसी में तन्मय रहो, फिर अन्तिम और अनन्त तुम्हारा हूँ, चाहे जहाँ रहूँ । रहूँ या न रहूँ की भाषा से परे, वही एकमेव मैं हूँ, तुम हो, नित्य, अविनाशी, संयुक्त !'
'जिस मुहूर्त में तुमने अपनाया था, उसी क्षण जान गयी थी कि कल्प- दर्पण सार्थक हो गया, समाप्त हो गया। काम, गरुड़, शिव तब तक भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ और धाराएँ बन कर मुझ में संचरित थे । कभी यह होती थी, कभी वह होती थी । निरन्तर संक्रमण में चल रही थी । संक्रांतिकाल था वह मेरा । तुमने उस दिन कहा था: 'वैना, ये तीनों केवल आत्मा हैं : आत्मा के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं ।' वहाँ तक पहुँचने को संक्रमण की एक पूरी अवधि पार करना थी । लगता है, वह आज पार हो गई, मैं अतिक्रान्त हो गई- तुम्हारे भीतर अपने अन्तरतम में । जहाँ केवल तुम हो मेरे, मैं हूँ तुम्हारी, और कोई नहीं ! देवता, अपरम्पार हो तुम !' और मेरे एक पग को दोनों हथेलियों में कमलायित कर, मेरे पदनख पर उसने माथा ढाल दिया । और उसे चूम लिया ।
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org