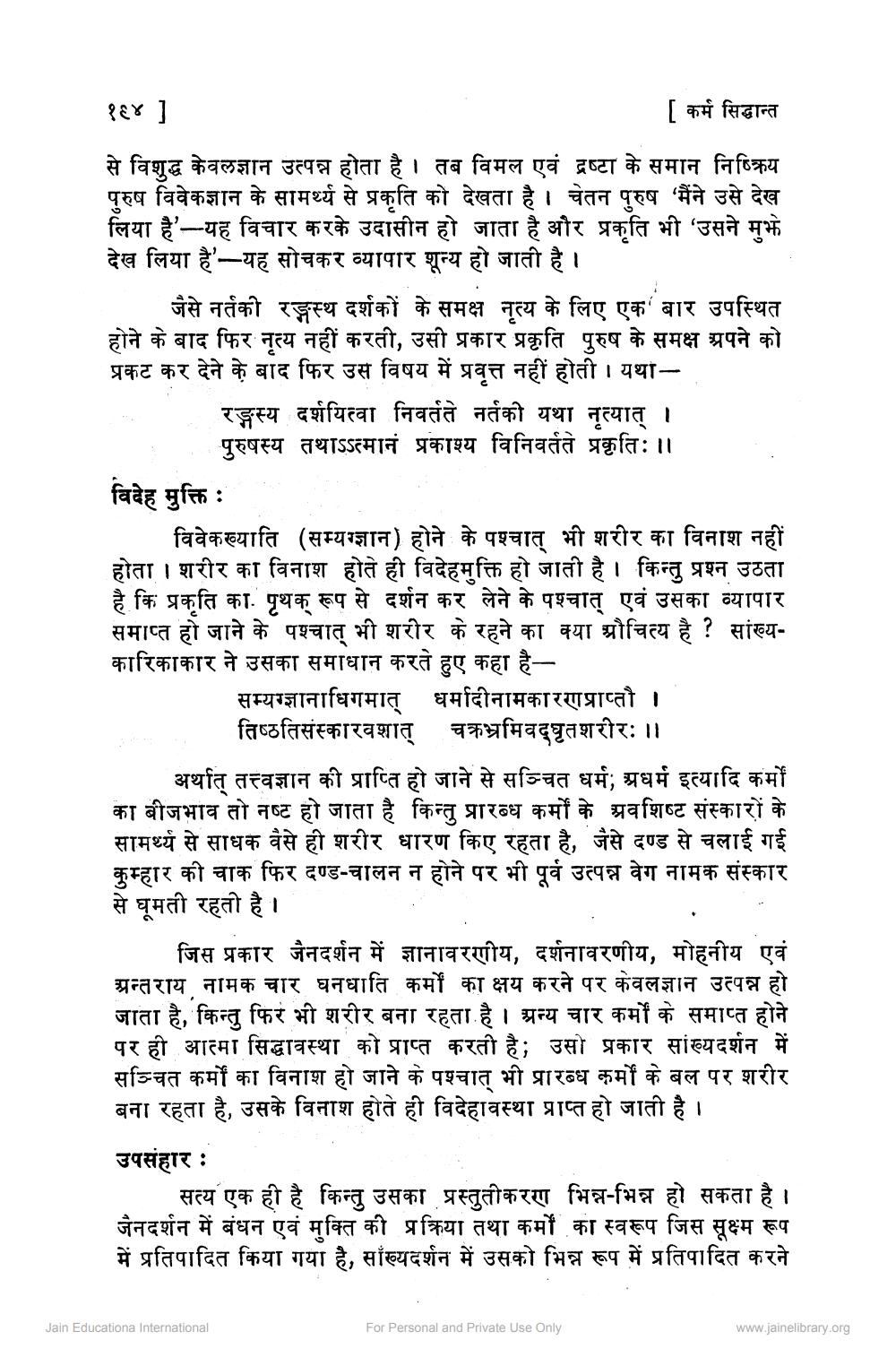________________
१६४ ]
[ कर्म सिद्धान्त
से विशुद्ध केवलज्ञान उत्पन्न होता है। तब विमल एवं द्रष्टा के समान निष्क्रिय पुरुष विवेकज्ञान के सामर्थ्य से प्रकृति को देखता है। चेतन पुरुष 'मैंने उसे देख लिया है'-यह विचार करके उदासीन हो जाता है और प्रकृति भी 'उसने मुझे देख लिया है'-यह सोचकर व्यापार शून्य हो जाती है ।
__ जैसे नर्तकी रङ्गस्थ दर्शकों के समक्ष नृत्य के लिए एक बार उपस्थित होने के बाद फिर नृत्य नहीं करती, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को प्रकट कर देने के बाद फिर उस विषय में प्रवृत्त नहीं होती। यथा
रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् ।
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः ।। विदेह मुक्ति :
विवेकख्याति (सम्यग्ज्ञान) होने के पश्चात् भी शरीर का विनाश नहीं होता । शरीर का विनाश होते ही विदेहमुक्ति हो जाती है। किन्तु प्रश्न उठता है कि प्रकृति का. पृथक् रूप से दर्शन कर लेने के पश्चात् एवं उसका व्यापार समाप्त हो जाने के पश्चात् भी शरीर के रहने का क्या औचित्य है ? सांख्यकारिकाकार ने उसका समाधान करते हुए कहा है
सम्यग्ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनामकारणप्राप्तौ ।
तिष्ठतिसंस्कारवशात् चक्रभ्रमिवद्धृत शरीरः ।। अर्थात् तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो जाने से सञ्चित धर्म; अधर्म इत्यादि कर्मों का बीजभाव तो नष्ट हो जाता है किन्तु प्रारब्ध कर्मों के अवशिष्ट संस्कारों के सामर्थ्य से साधक वैसे ही शरीर धारण किए रहता है, जैसे दण्ड से चलाई गई कुम्हार की चाक फिर दण्ड-चालन न होने पर भी पूर्व उत्पन्न वेग नामक संस्कार से घूमती रहती है।
जिस प्रकार जैनदर्शन में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय एवं अन्त राय नामक चार घनधाति कर्मों का क्षय करने पर केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है, किन्तु फिर भी शरीर बना रहता है। अन्य चार कर्मों के समाप्त होने पर ही आत्मा सिद्धावस्था को प्राप्त करती है; उसो प्रकार सांख्यदर्शन में सञ्चित कर्मों का विनाश हो जाने के पश्चात् भी प्रारब्ध कर्मों के बल पर शरीर बना रहता है, उसके विनाश होते ही विदेहावस्था प्राप्त हो जाती है । उपसंहार :
___सत्य एक ही है किन्तु उसका प्रस्तुतीकरण भिन्न-भिन्न हो सकता है। जैनदर्शन में बंधन एवं मुक्ति की प्रक्रिया तथा कर्मों का स्वरूप जिस सूक्ष्म रूप में प्रतिपादित किया गया है, साँख्यदर्शन में उसको भिन्न रूप में प्रतिपादित करने
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org