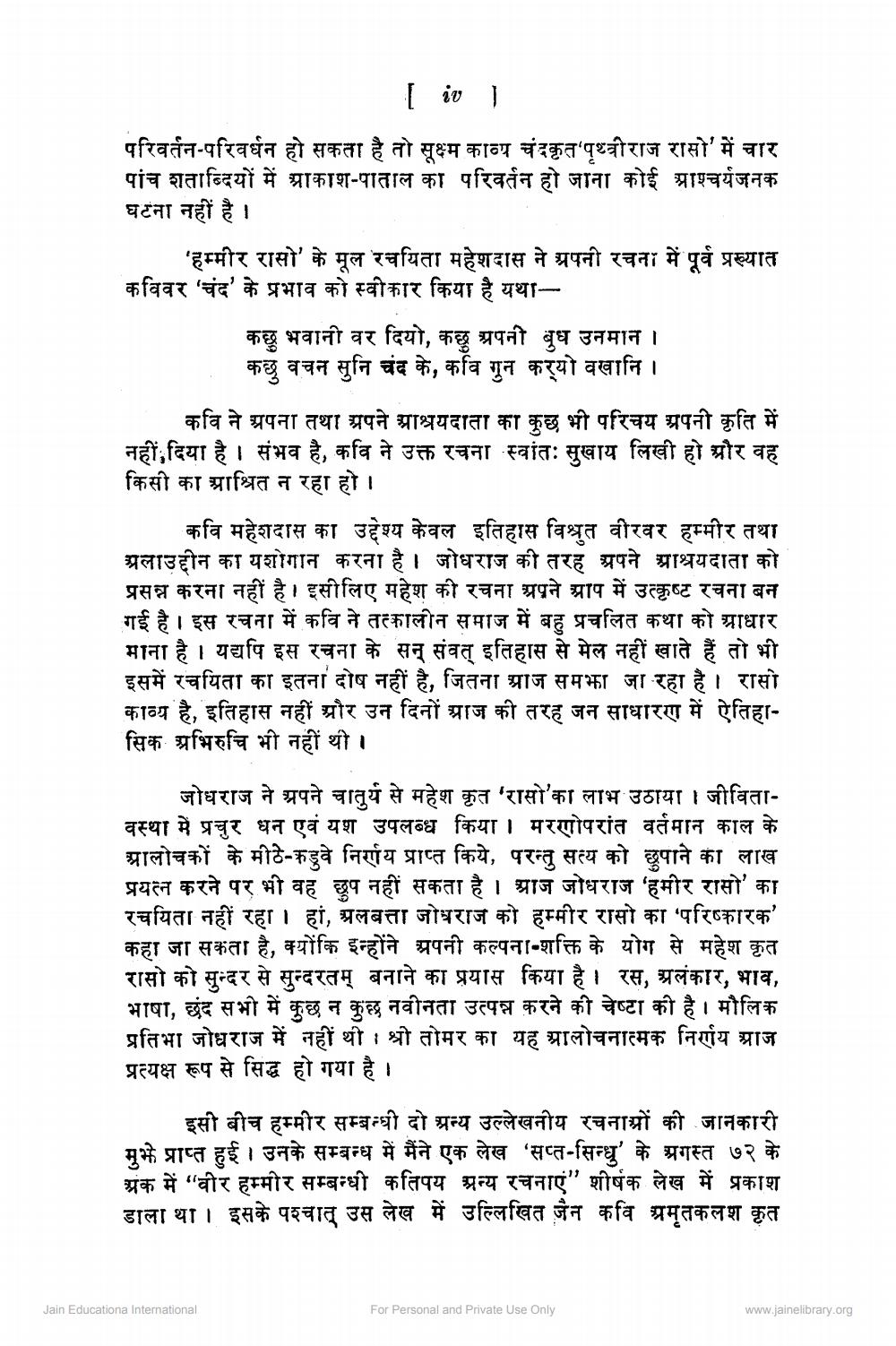________________
[
v
]
परिवर्तन-परिवर्धन हो सकता है तो सूक्ष्म काव्य चंदकृत पृथ्वीराज रासो' में चार पांच शताब्दियों में आकाश-पाताल का परिवर्तन हो जाना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है।
___ 'हम्मीर रासो' के मूल रचयिता महेशदास ने अपनी रचना में पूर्व प्रख्यात कविवर 'चंद' के प्रभाव को स्वीकार किया है यथा
कछु भवानी वर दियो, कछु अपनी बुध उनमान । कछु वचन सुनि चंद के, कवि गुन कर्यो वखानि ।
कवि ने अपना तथा अपने आश्रयदाता का कुछ भी परिचय अपनी कृति में नहीं दिया है। संभव है, कवि ने उक्त रचना स्वांतः सुखाय लिखी हो और वह किसी का आश्रित न रहा हो।
कवि महेशदास का उद्देश्य केवल इतिहास विश्रुत वीरवर हम्मीर तथा अलाउद्दीन का यशोगान करना है। जोधराज की तरह अपने प्राश्रयदाता को प्रसन्न करना नहीं है। इसीलिए महेश की रचना अपने आप में उत्कृष्ट रचना बन गई है। इस रचना में कवि ने तत्कालीन समाज में बहु प्रचलित कथा को आधार माना है । यद्यपि इस रचना के सन् संवत् इतिहास से मेल नहीं खाते हैं तो भी इसमें रचयिता का इतना दोष नहीं है, जितना आज समझा जा रहा है। रासो काव्य है, इतिहास नहीं और उन दिनों आज की तरह जन साधारण में ऐतिहासिक अभिरुचि भी नहीं थी।
जोधराज ने अपने चातुर्य से महेश कृत 'रासो'का लाभ उठाया । जीवितावस्था में प्रचुर धन एवं यश उपलब्ध किया। मरणोपरांत वर्तमान काल के आलोचकों के मीठे-कडवे निर्णय प्राप्त किये, परन्तु सत्य को छुपाने का लाख प्रयत्न करने पर भी वह छुप नहीं सकता है। आज जोधराज 'हमीर रासो' का रचयिता नहीं रहा। हां, अलबत्ता जोधराज को हम्मीर रासो का 'परिष्कारक' कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अपनी कल्पना-शक्ति के योग से महेश कृत रासो को सुन्दर से सुन्दरतम् बनाने का प्रयास किया है। रस, अलंकार, भाव, भाषा, छंद सभी में कुछ न कुछ नवीनता उत्पन्न करने की चेष्टा की है। मौलिक प्रतिभा जोधराज में नहीं थी। श्री तोमर का यह आलोचनात्मक निर्णय आज प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो गया है ।
इसी बीच हम्मीर सम्बन्धी दो अन्य उल्लेखनीय रचनाओं की जानकारी मुझे प्राप्त हुई। उनके सम्बन्ध में मैंने एक लेख 'सप्त-सिन्धु' के अगस्त ७२ के अक में “वीर हम्मीर सम्बन्धी कतिपय अन्य रचनाएं" शीर्षक लेख में प्रकाश डाला था। इसके पश्चात् उस लेख में उल्लिखित जैन कवि अमृतकलश कृत
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org