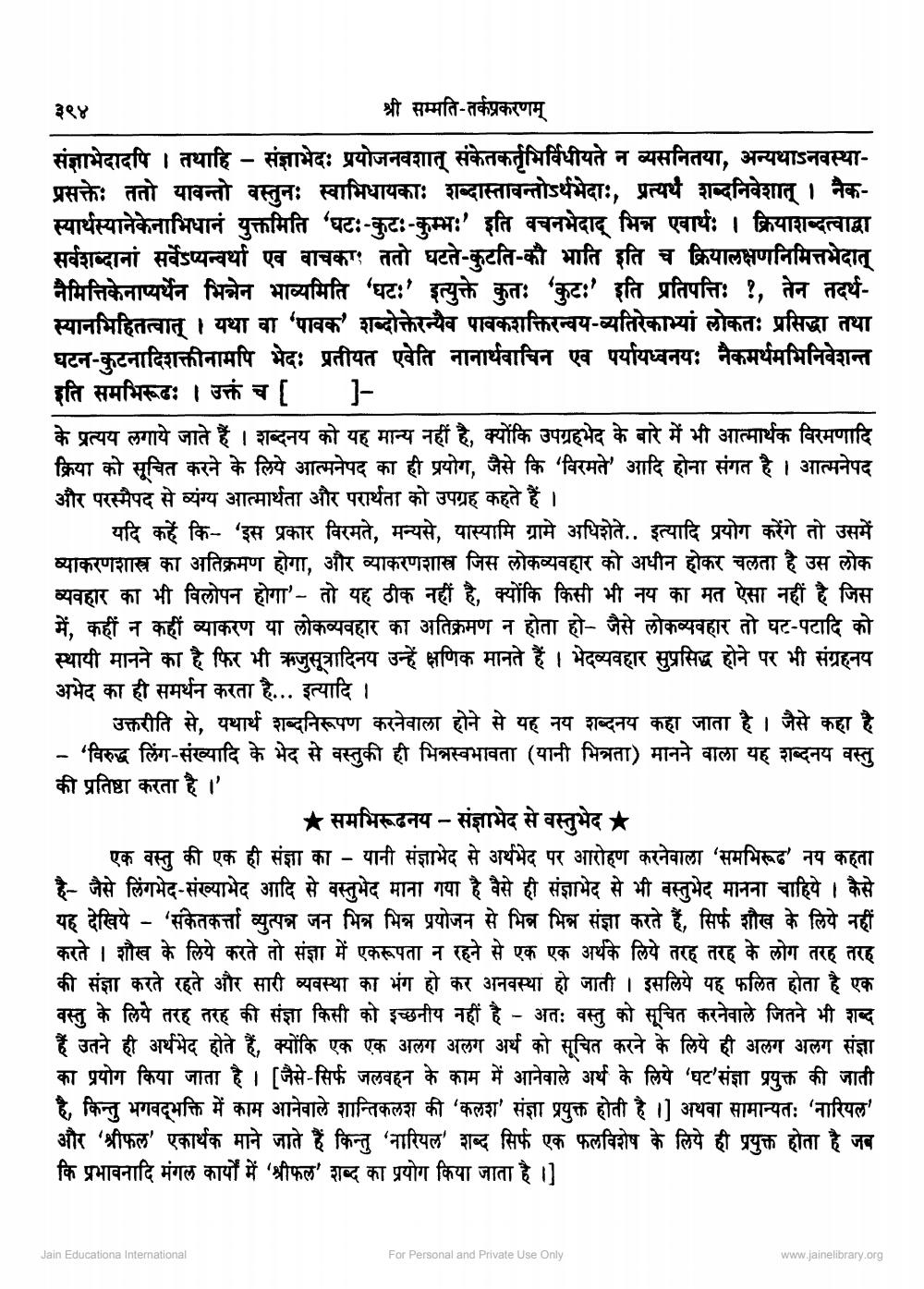________________
श्री सम्मति - तर्कप्रकरणम्
३९४
संज्ञाभेदादपि । तथाहि - संज्ञाभेदः प्रयोजनवशात् संकेतकर्तृभिर्विधीयते न व्यसनितया, अन्यथाऽनवस्थाप्रसक्तेः ततो यावन्तो वस्तुनः स्वाभिधायकाः शब्दास्तावन्तोऽर्थभेदाः, प्रत्यर्थं शब्दनिवेशात् । नैकस्यार्थस्यानेकेनाभिधानं युक्तमिति 'घट:- कुटः - कुम्भः' इति वचनभेदाद् भिन्न एवार्थः । क्रियाशब्दत्वाद्वा सर्वशब्दानां सर्वेऽप्यन्वर्था एव वाचकाः ततो घटते कुटति - कौ भाति इति च क्रियालक्षणनिमित्तभेदात् नैमित्तिकेनाप्यर्थेन भिन्नेन भाव्यमिति 'घटः' इत्युक्ते कुतः 'कुट:' इति प्रतिपत्तिः ?, तेन तदर्थ - स्यानभिहितत्वात् । यथा वा 'पावक' शब्दोक्तेरन्यैव पावकशक्तिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां लोकतः प्रसिद्धा तथा घटन - कुटनादिशक्तीनामपि भेदः प्रतीयत एवेति नानार्थवाचिन एव पर्यायध्वनयः नैकमर्थमभिनिवेशन्त इति समभिरूढः । उक्तं च [ ]
प्रत्यय लगाये जाते हैं । शब्दनय को यह मान्य नहीं है, क्योंकि उपग्रहभेद के बारे में भी आत्मार्थक विरमणादि क्रिया को सूचित करने के लिये आत्मनेपद का ही प्रयोग, जैसे कि 'विरमते' आदि होना संगत है । आत्मनेपद और परस्मैपद से व्यंग्य आत्मार्थता और परार्थता को उपग्रह कहते हैं ।
यदि कहें कि - ' इस प्रकार विरमते, मन्यसे, यास्यामि ग्रामे अधिशेते.. इत्यादि प्रयोग करेंगे तो उसमें व्याकरणशास्त्र का अतिक्रमण होगा, और व्याकरणशास्त्र जिस लोकव्यवहार को अधीन होकर चलता है उस लोक व्यवहार का भी विलोपन होगा' - तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी नय का मत ऐसा नहीं है जिस में, कहीं न कहीं व्याकरण या लोकव्यवहार का अतिक्रमण न होता हो- जैसे लोकव्यवहार तो घटपटादि को स्थायी मानने का है फिर भी ऋजुसूत्रादिनय उन्हें क्षणिक मानते हैं । भेदव्यवहार सुप्रसिद्ध होने पर भी संग्रहनय अभेद का ही समर्थन करता है... इत्यादि ।
उक्तरीति से, यथार्थ शब्दनिरूपण करनेवाला होने से यह नय शब्दनय कहा जाता है। जैसे कहा है - 'विरुद्ध लिंग-संख्यादि के भेद से वस्तुकी ही भिन्नस्वभावता (यानी भिन्नता) मानने वाला यह शब्दनय वस्तु की प्रतिष्ठा करता है ।'
-
★ समभिरूढनय - संज्ञाभेद से वस्तुभेद★
एक वस्तु की एक ही संज्ञा का - यानी संज्ञाभेद से अर्थभेद पर आरोहण करनेवाला 'समभिरूढ' नय कहता है- जैसे लिंगभेद - संख्याभेद आदि से वस्तुभेद माना गया है वैसे ही संज्ञाभेद से भी वस्तुभेद मानना चाहिये । कैसे यह देखिये - 'सकतकर्त्ता व्युत्पन्न जन भिन्न भिन्न प्रयोजन से भिन्न भिन्न संज्ञा करते हैं, सिर्फ शौख के लिये नहीं करते । शौख के लिये करते तो संज्ञा में एकरूपता न रहने से एक एक अर्थके लिये तरह तरह के लोग तरह तरह की संज्ञा करते रहते और सारी व्यवस्था का भंग हो कर अनवस्था हो जाती । इसलिये यह फलित होता है एक के लिये तरह तरह की संज्ञा किसी को इच्छनीय नहीं है वस्तु अतः वस्तु को सूचित करनेवाले जितने भी शब्द हैं उतने ही अर्थभेद होते हैं, क्योंकि एक एक अलग अलग अर्थ को सूचित करने के लिये ही अलग अलग संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। [ जैसे सिर्फ जलवहन के काम में आनेवाले अर्थ के लिये 'घट' संज्ञा प्रयुक्त की जाती है, किन्तु भगवद्भक्ति में काम आनेवाले शान्तिकलश की 'कलश' संज्ञा प्रयुक्त होती है ।] अथवा सामान्यतः 'नारियल ' और 'श्रीफल' एकार्थक माने जाते हैं किन्तु 'नारियल' शब्द सिर्फ एक फलविशेष के लिये ही प्रयुक्त होता है जब कि प्रभावनादि मंगल कार्यों में 'श्रीफल' शब्द का प्रयोग किया जाता है । ]
Jain Educationa International
-
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org