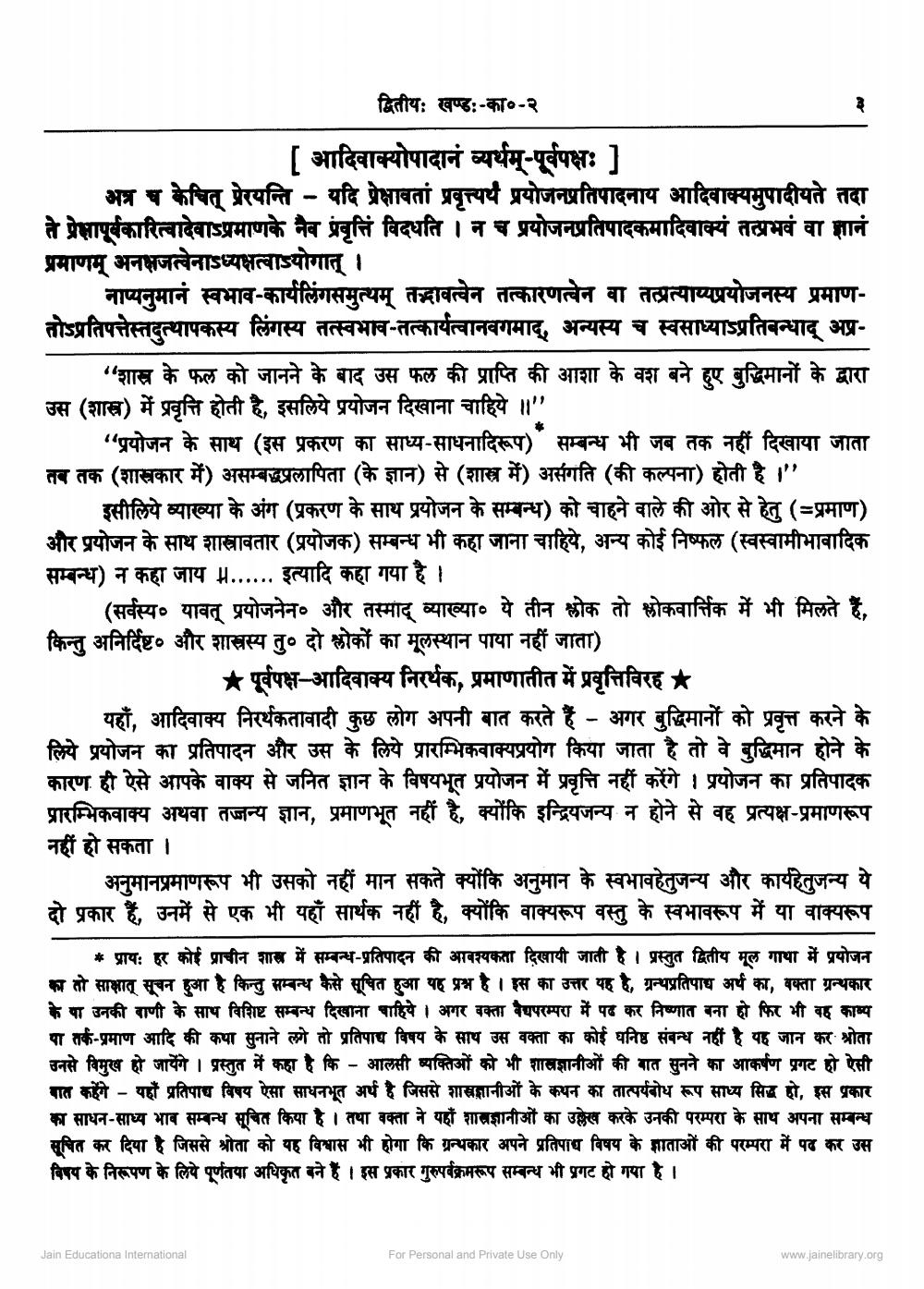________________
द्वितीयः खण्ड:-का०-२
[ आदिवाक्योपादानं व्यर्थम्-पूर्वपक्षः ] अत्र च केचित् प्रेरयन्ति - यदि प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यर्य प्रयोजनप्रतिपादनाय आदिवाक्यमुपादीयते तदा ते प्रेक्षापूर्वकारित्वादेवाप्रमाणके नैव प्रवृत्तिं विदधति । न च प्रयोजनप्रतिपादकमादिवाक्यं तत्रभवं वा ज्ञानं प्रमाणम् अनक्षजत्वेनाऽध्यक्षत्वाऽयोगात् ।।
___ नाप्यनुमानं स्वभाव-कार्यलिंगसमुत्यम् तद्भावत्वेन तत्कारणत्वेन वा तत्प्रत्याय्यप्रयोजनस्य प्रमाणतोऽप्रतिपत्तेस्तदुत्थापकस्य लिंगस्य तत्स्वभाव-तत्कार्यत्वानवगमाद्, अन्यस्य च स्वसाध्या प्रतिबन्धाद् अप्र
"शास्र के फल को जानने के बाद उस फल की प्राप्ति की आशा के वश बने हुए बुद्धिमानों के द्वारा उस (शास्र) में प्रवृत्ति होती है, इसलिये प्रयोजन दिखाना चाहिये ॥"
"प्रयोजन के साथ (इस प्रकरण का साध्य-साधनादिरूप) सम्बन्ध भी जब तक नहीं दिखाया जाता तब तक (शास्रकार में) असम्बद्धप्रलापिता (के ज्ञान) से (शास्त्र में) असंगति (की कल्पना) होती है।"
इसीलिये व्याख्या के अंग (प्रकरण के साथ प्रयोजन के सम्बन्ध) को चाहने वाले की ओर से हेतु (=प्रमाण) और प्रयोजन के साथ शास्त्रावतार (प्रयोजक) सम्बन्ध भी कहा जाना चाहिये, अन्य कोई निष्फल (स्वस्वामीभावादिक सम्बन्ध) न कहा जाय H...... इत्यादि कहा गया है ।
(सर्वस्य० यावत् प्रयोजनेन० और तस्माद् व्याख्या० ये तीन श्लोक तो श्लोकवार्तिक में भी मिलते हैं, किन्तु अनिर्दिष्ट. और शास्त्रस्य तु० दो श्लोकों का मूलस्थान पाया नहीं जाता)
★ पूर्वपक्ष-आदिवाक्य निरर्थक, प्रमाणातीत में प्रवृत्तिविरह ★ यहाँ, आदिवाक्य निरर्थकतावादी कुछ लोग अपनी बात करते हैं - अगर बुद्धिमानों को प्रवृत्त करने के लिये प्रयोजन का प्रतिपादन और उस के लिये प्रारम्भिकवाक्यप्रयोग किया जाता है तो वे बुद्धिमान होने के कारण ही ऐसे आपके वाक्य से जनित ज्ञान के विषयभूत प्रयोजन में प्रवृत्ति नहीं करेंगे । प्रयोजन का प्रतिपादक प्रारम्भिकवाक्य अथवा तजन्य ज्ञान, प्रमाणभूत नहीं है, क्योंकि इन्द्रियजन्य न होने से वह प्रत्यक्ष-प्रमाणरूप नहीं हो सकता।
अनुमानप्रमाणरूप भी उसको नहीं मान सकते क्योंकि अनुमान के स्वभावहेतुजन्य और कार्यहेतुजन्य ये दो प्रकार हैं, उनमें से एक भी यहाँ सार्थक नहीं है, क्योंकि वाक्यरूप वस्तु के स्वभावरूप में या वाक्यरूप
* प्राय: हर कोई प्राचीन शास्त्र में सम्बन्ध-प्रतिपादन की आवश्यकता दिखायी जाती है। प्रस्तुत द्वितीय मूल गाथा में प्रयोजन का तो साक्षात् सूचन हुआ है किन्तु सम्बन्ध कैसे सूचित हुआ यह प्रश्न है। इस का उत्तर यह है, ग्रन्थप्रतिपाद्य अर्थ का, बक्ता ग्रन्थकार के या उनकी वाणी के साथ विशिष्ट सम्बन्ध दिखाना चाहिये। अगर वक्ता वैधपरम्परा में पढ कर निष्णात बना हो फिर भी वह काव्य पा तर्क-प्रमाण आदि की कथा सुनाने लगे तो प्रतिपाद्य विषय के साथ उस वक्ता का कोई घनिष्ठ संबन्ध नहीं है यह जान कर श्रोता उनसे विमुख हो जायेंगे । प्रस्तुत में कहा है कि - आलसी व्यक्तिओं को भी शास्त्रज्ञानीओं की बात सुनने का आकर्षण प्रगट हो ऐसी बात कहेंगे - यहाँ प्रतिपाद्य विषय ऐसा साधनभूत अर्थ है जिससे शास्त्रज्ञानीओं के कथन का तात्पर्यबोध रूप साध्य सिद्ध हो, इस प्रकार का साधन-साध्य भाव सम्बन्ध सूचित किया है। तथा वक्ता ने यहाँ शास्त्रज्ञानीओं का उल्लेख करके उनकी परम्परा के साथ अपना सम्बन्ध सचित कर दिया है जिससे श्रोता को यह विश्वास भी होगा कि ग्रन्थकार अपने प्रतिपाद्य विषय के ज्ञाताओं की परम्परा में प विषय के निरूपण के लिये पूर्णतया अधिकृत बने हैं। इस प्रकार गुरुपर्वक्रमरूप सम्बन्ध भी प्रगट हो गया है।
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org