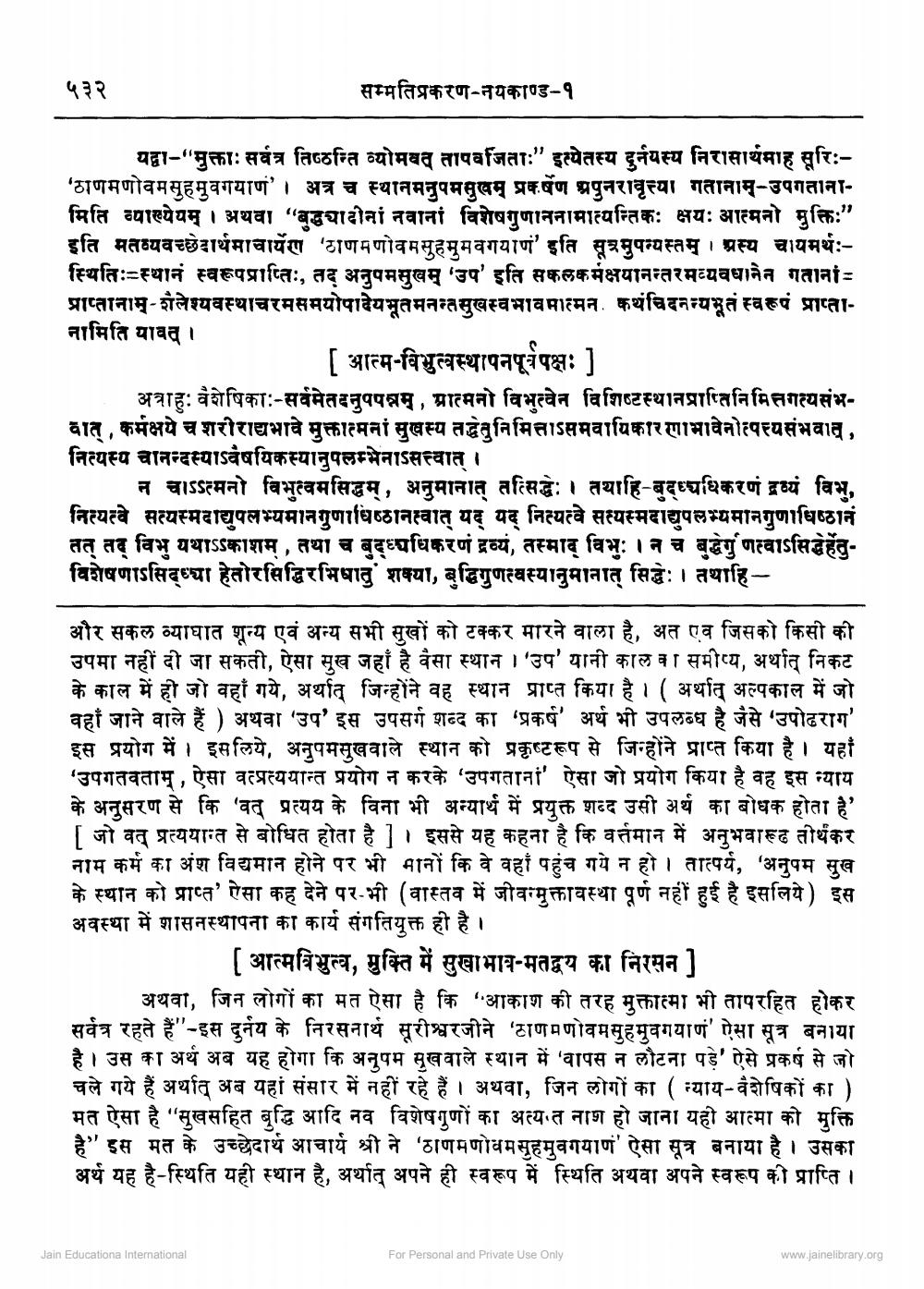________________
५३२
सम्मतिप्रकरण-नयकाण्ड-१
यद्वा-"मुक्ताः सर्वत्र तिष्ठन्ति व्योमवत तापजिताः" इत्येतस्य दुर्नयस्य निरासार्थमाह सूरि:'ठाणमणोवमसुहमुवगयाणं'। अत्र च स्थानमनुपमसुखम् प्रकर्षेण अपुनरावृत्त्या गतानाम-उपगतानामिति व्याख्येयम् । अथवा "बुद्धयादीनां नवानां विशेषगुणाननामात्यन्तिकः क्षयः आत्मनो मुक्तिः" इति मतव्यवच्छेदार्थमाचार्येण 'ठाणमणोवमसुहमुमवगयाणं' इति सूत्रमुपन्यस्तम् । अस्य चायमर्थःस्थितिः-स्थानं स्वरूपप्राप्तिः, तद अनुपमसुखम् 'उप' इति सकलकर्मक्षयानन्तरमव्यवधानेन गतानां: प्राप्तानाम्-शैलेश्यवस्थाचरमसमयोपादेयभूतमनन्तसुखस्वभावमात्मन. कथंचिदनन्यभूतं स्वरूप प्राप्तानामिति यावत् ।
[ आत्म-विभुत्वस्थापनपूर्वपक्षः ] अत्राहुः वैशेषिका:-सर्वमेतदनुपपन्नम् , प्रात्मनो विभुत्वेन विशिष्ट स्थानप्राप्तिनिमित्तगत्यसंभवात् , कर्मक्षये च शरीराद्यभावे मुक्तात्मनां सुखस्य तद्धेतुनिमित्ताऽसमवायिकारणाभावेनोत्पत्त्यसंभवात , नित्यस्य चानन्दस्याऽवैषयिकस्यानुपलम्भेनाऽसत्त्वात् ।
___ न चाऽऽत्मनो विभुत्वमसिद्धम् , अनुमानात् तत्सिद्धेः । तथाहि-बुद्ध्यधिकरणं द्रव्यं विभु, नित्यत्वे सत्यस्मदाधुपलभ्यमानगुणाधिष्ठानत्वात् यद् यद् नित्यत्वे सत्यस्मदाद्युपलभ्यमानगुणाधिष्ठानं तत् तद् विभु यथाऽऽकाशम् , तथा च बुद्ध्यधिकरणं द्रव्यं, तस्मात् विभुः । न च बुद्धगुणत्वाऽसिद्धेहेतुविशेषणाऽसिद्ध्या हेतोरसिद्धिरभिधातु शक्या, बुद्धिगुणत्वस्यानुमानात् सिद्धेः । तथाहि
और सकल व्याघात शून्य एवं अन्य सभी सुखों को टक्कर मारने वाला है, अत एव जिसको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा सुख जहाँ है वैसा स्थान । 'उप' यानी काल का समीप्य, अर्थात् निकट के काल में ही जो वहाँ गये, अर्थात् जिन्होंने वह स्थान प्राप्त किया है । ( अर्थात् अल्पकाल में जो वहाँ जाने वाले हैं ) अथवा 'उप' इस उपसर्ग शब्द का 'प्रकर्ष' अर्थ भी उपलब्ध है जैसे 'उपोढराग' इस प्रयोग में। इसलिये, अनुपमसुखवाले स्थान को प्रकृष्टरूप से जिन्होंने प्राप्त किया है। यहाँ 'उपगतवताम् , ऐसा वत्प्रत्ययान्त प्रयोग न करके 'उपगतानां' ऐसा जो प्रयोग किया है वह इस न्याय के अन से कि 'वत् प्रत्यय के विना भी अन्यार्थ में प्रयुक्त शब्द उसी अर्थ का बोधक होता है [जो वत प्रत्ययान्त से बोधित होता है। इससे यह कहना है कि वर्तमान में अनभवारूद तीर्थकर नाम कर्म का अंश विद्यमान होने पर भी मानों कि वे वहाँ पहुंच गये न हो । तात्पर्य, 'अनुपम सुख के स्थान को प्राप्त' ऐसा कह देने पर भी (वास्तव में जीवन्मुक्तावस्था पूर्ण नहीं हुई है इसलिये) इस अवस्था में शासनस्थापना का कार्य संगतियुक्त ही है।
[आत्मविभुत्व, मुक्ति में सुखाभाव-मतद्वय का निरसन ] अथवा, जिन लोगों का मत ऐसा है कि "आकाश की तरह मुक्तात्मा भी तापरहित होकर सर्वत्र रहते हैं"-इस दुर्नय के निरसनार्थ सूरीश्वरजीने 'ठाण मणोवमसुहमुवगयाणं' ऐसा सूत्र बनाया है। उस का अर्थ अब यह होगा कि अनुपम सुखवाले स्थान में वापस न लौटना पड़े' ऐसे प्रकर्ष से जो चले गये हैं अर्थात् अब यहां संसार में नहीं रहे हैं। अथवा, जिन लोगों का ( न्याय-वैशेषिकों का ) मत ऐसा है "सुखसहित बुद्धि आदि नव विशेषगुणों का अत्यन्त नाश हो जाना यही आत्मा को मुक्ति है" इस मत के उच्छेदार्थ आचार्य श्री ने 'ठाणमणोवम सुहमुवगयाणं' ऐसा सूत्र बनाया है। उसका अर्थ यह है-स्थिति यही स्थान है, अर्थात् अपने ही स्वरूप में स्थिति अथवा अपने स्वरूप की प्राप्ति ।
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org