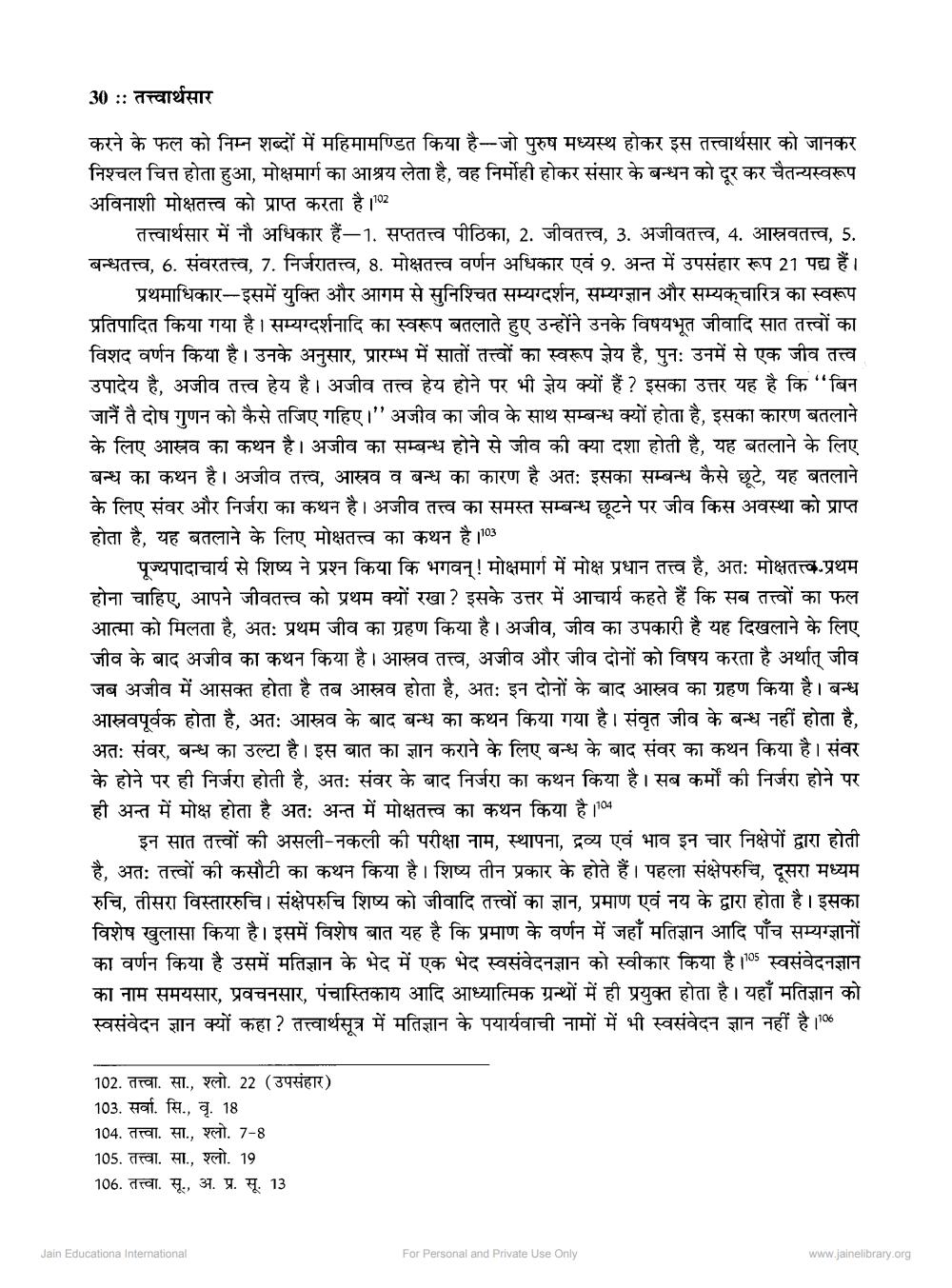________________
30 :: तत्त्वार्थसार
करने के फल को निम्न शब्दों में महिमामण्डित किया है जो पुरुष मध्यस्थ होकर इस तत्त्वार्थसार को जानकर निश्चल चित्त होता हुआ, मोक्षमार्ग का आश्रय लेता है, वह निर्मोही होकर संसार के बन्धन को दूर कर चैतन्यस्वरूप अविनाशी मोक्षतत्त्व को प्राप्त करता है।102
तत्त्वार्थसार में नौ अधिकार हैं-1. सप्ततत्त्व पीठिका, 2. जीवतत्त्व, 3. अजीवतत्त्व, 4. आस्रवतत्त्व, 5. बन्धतत्त्व, 6. संवरतत्त्व, 7. निर्जरातत्त्व, 8. मोक्षतत्त्व वर्णन अधिकार एवं 9. अन्त में उपसंहार रूप 21 पद्य हैं।
प्रथमाधिकार-इसमें युक्ति और आगम से सुनिश्चित सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। सम्यग्दर्शनादि का स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने उनके विषयभूत जीवादि सात तत्त्वों का विशद वर्णन किया है। उनके अनुसार, प्रारम्भ में सातों तत्त्वों का स्वरूप ज्ञेय है, पुन: उनमें से एक जीव तत्त्व उपादेय है, अजीव तत्त्व हेय है। अजीव तत्त्व हेय होने पर भी ज्ञेय क्यों हैं? इसका उत्तर यह है कि "बिन जानैं तै दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए।" अजीव का जीव के साथ सम्बन्ध क्यों होता है, इसका कारण बतलाने के लिए आस्रव का कथन है। अजीव का सम्बन्ध होने से जीव की क्या दशा होती है, यह बतलाने के लिए बन्ध का कथन है। अजीव तत्त्व, आस्रव व बन्ध का कारण है अत: इसका सम्बन्ध कैसे छूटे, यह बतलाने के लिए संवर और निर्जरा का कथन है। अजीव तत्त्व का समस्त सम्बन्ध छूटने पर जीव किस अवस्था को प्राप्त होता है, यह बतलाने के लिए मोक्षतत्त्व का कथन है।03
पूज्यपादाचार्य से शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवन् ! मोक्षमार्ग में मोक्ष प्रधान तत्त्व है, अत: मोक्षतत्त्व.प्रथम होना चाहिए, आपने जीवतत्त्व को प्रथम क्यों रखा? इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि सब तत्त्वों का फल आत्मा को मिलता है, अत: प्रथम जीव का ग्रहण किया है। अजीव, जीव का उपकारी है यह दिखलाने के लिए जीव के बाद अजीव का कथन किया है। आस्रव तत्त्व, अजीव और जीव दोनों को विषय करता है अर्थात् जीव जब अजीव में आसक्त होता है तब आस्रव होता है, अतः इन दोनों के बाद आस्रव का ग्रहण किया है। बन्ध आस्रवपूर्वक होता है, अत: आस्रव के बाद बन्ध का कथन किया गया है। संवृत जीव के बन्ध नहीं होता है, अतः संवर, बन्ध का उल्टा है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए बन्ध के बाद संवर का कथन किया है। संवर के होने पर ही निर्जरा होती है, अतः संवर के बाद निर्जरा का कथन किया है। सब कर्मों की निर्जरा होने पर ही अन्त में मोक्ष होता है अतः अन्त में मोक्षतत्त्व का कथन किया है।
इन सात तत्त्वों की असली-नकली की परीक्षा नाम, स्थापना, द्रव्य एवं भाव इन चार निक्षेपों द्वारा होती है, अतः तत्त्वों की कसौटी का कथन किया है। शिष्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला संक्षेपरुचि, दूसरा मध्यम रुचि, तीसरा विस्ताररुचि। संक्षेपरुचि शिष्य को जीवादि तत्त्वों का ज्ञान, प्रमाण एवं नय के द्वारा होता है। इसका विशेष खुलासा किया है। इसमें विशेष बात यह है कि प्रमाण के वर्णन में जहाँ मतिज्ञान आदि पाँच सम्यग्ज्ञानों का वर्णन किया है उसमें मतिज्ञान के भेद में एक भेद स्वसंवेदनज्ञान को स्वीकार किया है।105 स्वसंवेदनज्ञान का नाम समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों में ही प्रयुक्त होता है। यहाँ मतिज्ञान को स्वसंवेदन ज्ञान क्यों कहा? तत्त्वार्थसूत्र में मतिज्ञान के पयार्यवाची नामों में भी स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है।106
102. तत्त्वा. सा., श्लो. 22 (उपसंहार) 103. सर्वा. सि., वृ. 18 104. तत्त्वा . सा., श्लो . 7-8 105. तत्त्वा . सा., श्लो. 19 106. तत्त्वा . सू., अ. प्र. सू. 13
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org