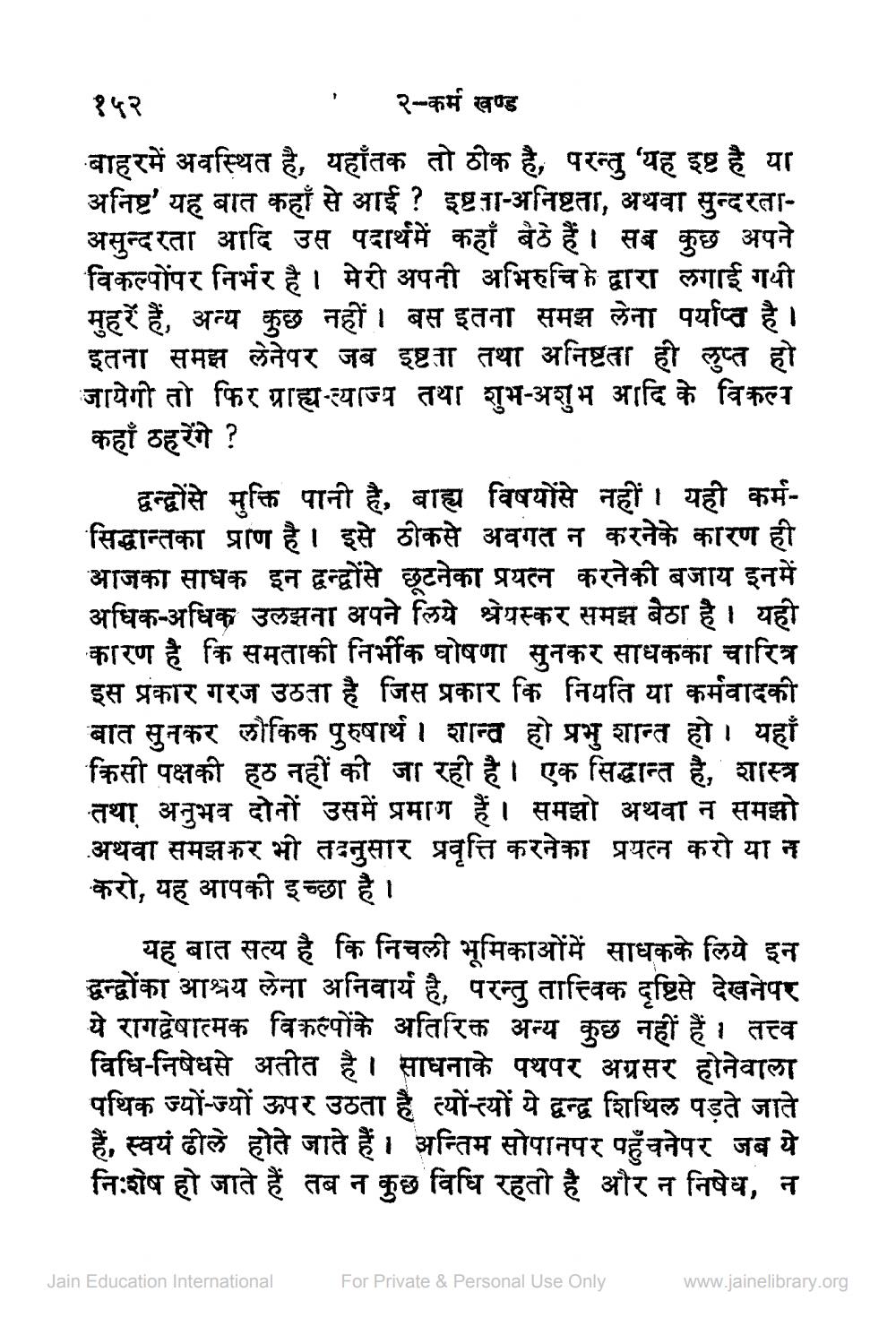________________
१५२
' २-कर्म खण्ड बाहरमें अवस्थित है, यहाँतक तो ठीक है, परन्तु 'यह इष्ट है या अनिष्ट' यह बात कहाँ से आई ? इष्टता-अनिष्टता, अथवा सुन्दरताअसुन्दरता आदि उस पदार्थमें कहाँ बैठे हैं। सब कुछ अपने विकल्पोंपर निर्भर है। मेरी अपनी अभिरुचि के द्वारा लगाई गयी मुहरें हैं, अन्य कुछ नहीं। बस इतना समझ लेना पर्याप्त है। इतना समझ लेनेपर जब इष्टता तथा अनिष्टता ही लुप्त हो जायेगी तो फिर ग्राह्य-त्याज्य तथा शुभ-अशुभ आदि के विकल कहाँ ठहरेंगे ?
द्वन्द्वोंसे मुक्ति पानी है, बाह्य विषयोंसे नहीं। यही कर्मसिद्धान्तका प्राण है। इसे ठीकसे अवगत न करनेके कारण ही आजका साधक इन द्वन्द्वोंसे छूटनेका प्रयत्न करनेकी बजाय इनमें अधिक-अधिक उलझना अपने लिये श्रेयस्कर समझ बैठा है। यही कारण है कि समताकी निर्भीक घोषणा सुनकर साधकका चारित्र इस प्रकार गरज उठता है जिस प्रकार कि नियति या कर्मवादकी बात सुनकर लौकिक पुरुषार्थ । शान्त हो प्रभु शान्त हो। यहाँ किसी पक्षकी हठ नहीं की जा रही है। एक सिद्धान्त है, शास्त्र तथा अनुभव दोनों उसमें प्रमाण हैं। समझो अथवा न समझो अथवा समझकर भी तदनुसार प्रवृत्ति करनेका प्रयत्न करो या न करो, यह आपकी इच्छा है।
यह बात सत्य है कि निचली भूमिकाओं में साधकके लिये इन द्वन्द्वोंका आश्रय लेना अनिवार्य है, परन्तु तात्त्विक दृष्टिसे देखनेपर ये रागद्वेषात्मक विकल्पोंके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हैं। तत्त्व विधि-निषेधसे अतीत है। साधनाके पथपर अग्रसर होनेवाला पथिक ज्यों-ज्यों ऊपर उठता है त्यों-त्यों ये द्वन्द्व शिथिल पड़ते जाते हैं, स्वयं ढीले होते जाते हैं। अन्तिम सोपानपर पहुँचनेपर जब ये निःशेष हो जाते हैं तब न कुछ विधि रहती है और न निषेध, न
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org