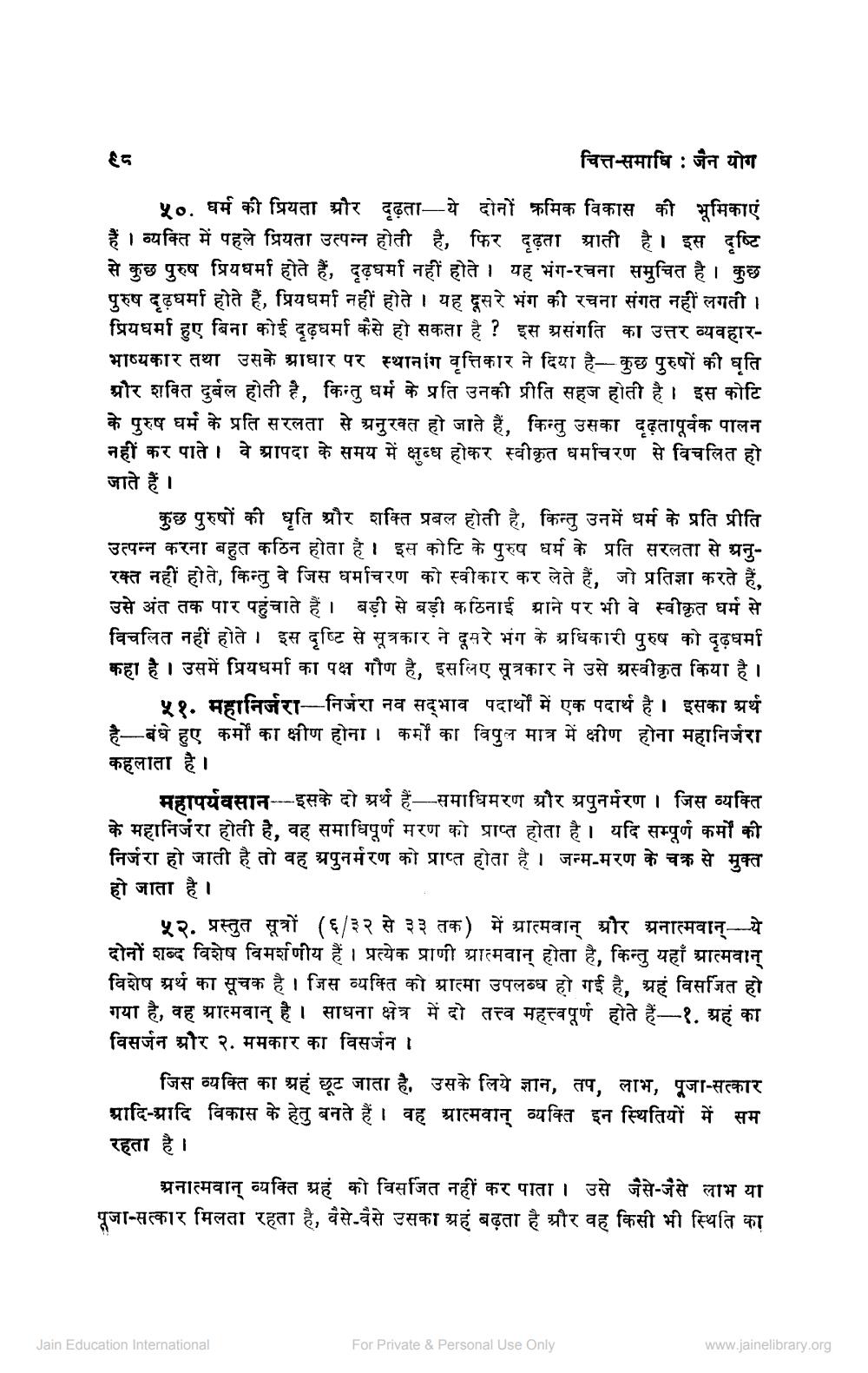________________
चित्त-समाधि : जैन योग ५०. धर्म की प्रियता और दृढ़ता—ये दोनों क्रमिक विकास की भूमिकाएं हैं । व्यक्ति में पहले प्रियता उत्पन्न होती है, फिर दृढ़ता आती है। इस दृष्टि से कुछ पुरुष प्रियधर्मा होते हैं, दृढ़धर्मा नहीं होते। यह भंग-रचना समुचित है। कुछ पुरुष दृढ़धर्मा होते हैं, प्रियधर्मा नहीं होते। यह दूसरे भंग की रचना संगत नहीं लगती। प्रियधर्मा हुए बिना कोई दृढ़धर्मा कैसे हो सकता है ? इस असंगति का उत्तर व्यवहारभाष्यकार तथा उसके आधार पर स्थानांग वृत्तिकार ने दिया है-कुछ पुरुषों की घृति
और शक्ति दुर्बल होती है, किन्तु धर्म के प्रति उनकी प्रीति सहज होती है। इस कोटि के पुरुष धर्म के प्रति सरलता से अनुरक्त हो जाते हैं, किन्तु उसका दृढ़तापूर्वक पालन नहीं कर पाते। वे आपदा के समय में क्षुब्ध होकर स्वीकृत धर्माचरण से विचलित हो जाते हैं।
कुछ पुरुषों की धृति और शक्ति प्रबल होती है, किन्तु उनमें धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करना बहुत कठिन होता है। इस कोटि के पुरुष धर्म के प्रति सरलता से अनुरक्त नहीं होते, किन्तु वे जिस धर्माचरण को स्वीकार कर लेते हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं. उसे अंत तक पार पहुंचाते हैं। बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर भी वे स्वीकृत धर्म से विचलित नहीं होते। इस दृष्टि से सूत्रकार ने दूसरे भंग के अधिकारी पुरुष को दृढ़धर्मा कहा है । उसमें प्रियधर्मा का पक्ष गौण है, इसलिए सूत्रकार ने उसे अस्वीकृत किया है।
५१. महानिर्जरा-निर्जरा नव सद्भाव पदार्थों में एक पदार्थ है। इसका अर्थ है-बंधे हुए कर्मों का क्षीण होना । कर्मों का विपुल मात्र में क्षीण होना महानिर्जरा कहलाता है।
महापर्यवसान----इसके दो अर्थ हैं—समाधिमरण और अपुनर्मरण । जिस व्यक्ति के महानिर्जरा होती है, वह समाधिपूर्ण मरण को प्राप्त होता है। यदि सम्पूर्ण कर्मों की निर्जरा हो जाती है तो वह अपुनर्मरण को प्राप्त होता है । जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है।
५२. प्रस्तुत सूत्रों (६/३२ से ३३ तक) में प्रात्मवान् और अनात्मवान्--ये दोनों शब्द विशेष विमर्शणीय हैं। प्रत्येक प्राणी प्रात्मवान् होता है, किन्तु यहाँ आत्मवान् विशेष अर्थ का सूचक है । जिस व्यक्ति को प्रात्मा उपलब्ध हो गई है, अहं विसर्जित हो गया है, वह आत्मवान् है। साधना क्षेत्र में दो तत्त्व महत्त्वपूर्ण होते हैं-१. अहं का विसर्जन और २. ममकार का विसर्जन ।
जिस व्यक्ति का अहं छूट जाता है, उसके लिये ज्ञान, तप, लाभ, पूजा-सत्कार प्रादि-आदि विकास के हेतु बनते हैं। वह आत्मवान् व्यक्ति इन स्थितियों में सम रहता है।
अनात्मवान् व्यक्ति अहं को विजित नहीं कर पाता। उसे जैसे-जैसे लाभ या पूजा-सत्कार मिलता रहता है, वैसे-वैसे उसका अहं बढ़ता है और वह किसी भी स्थिति का
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org