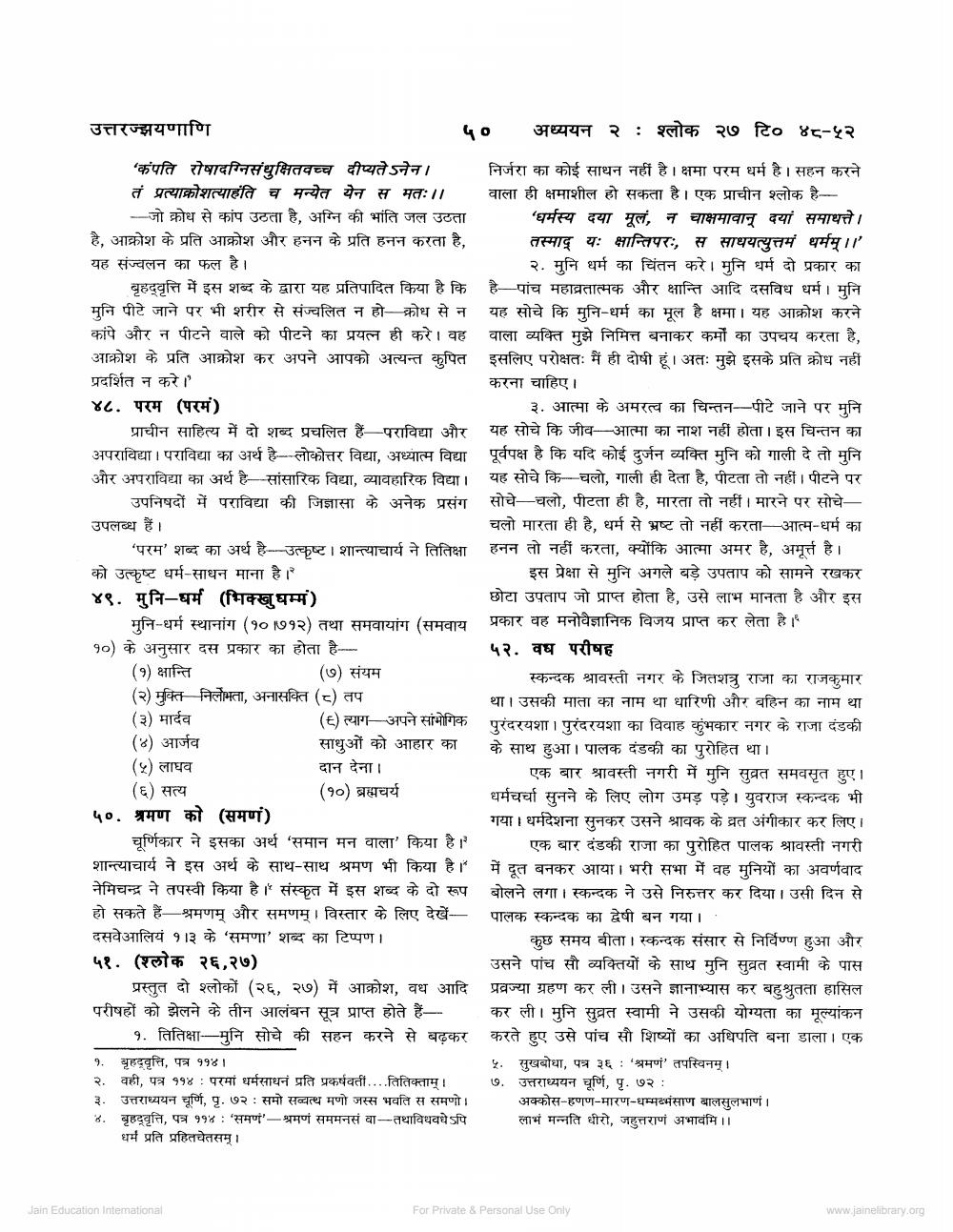________________
उत्तरज्झयणाणि
'कपति रोषादग्निसंयुक्षितवच्च दीप्यते ऽनेन । तं प्रत्याक्रोशत्याहंति च मन्येत येन स मतः ।। -जो क्रोध से कांप उठता है, अग्नि की भांति जल उठता है, आक्रोश के प्रति आक्रोश और हनन के प्रति हनन करता है, यह संज्वलन का फल है ।
बृहद्वृत्ति में इस शब्द के द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि मुनि पीटे जाने पर भी शरीर से संज्वलित न हो— क्रोध से न कांपे और न पीटने वाले को पीटने का प्रयत्न ही करे। वह आक्रोश के प्रति आक्रोश कर अपने आपको अत्यन्त कुपित प्रदर्शित न करे।'
४८. परम (परमं )
प्राचीन साहित्य में दो शब्द प्रचलित हैं—–पराविद्या और अपराविद्या । पराविद्या का अर्थ है-लोकोत्तर विद्या, अध्यात्म विद्या और अपराविद्या का अर्थ है सांसारिक विद्या, व्यावहारिक विद्या । उपनिषदों में पराविद्या की जिज्ञासा के अनेक प्रसंग उपलब्ध हैं।
५०
'परम' शब्द का अर्थ है-उत्कृष्ट । शान्त्याचार्य ने तितिक्षा को उत्कृष्ट धर्म-साधन माना है।
४९. मुनि धर्म (भिक्खु धम्म)
मुनि-धर्म स्थानांग (१०।७१२) तथा समवायांग (समवाय १०) के अनुसार दस प्रकार का होता है(१) क्षान्ति
(७) संयम
(२) मुक्ति निलभता, अनासक्ति (८) तप (३) मार्दय
(४) आर्जव
(५) लाघव
(६) सत्य
५०. श्रमण को (समणं)
चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'समान मन वाला' किया है। शान्त्याचार्य ने इस अर्थ के साथ-साथ श्रमण भी किया है।* नेमिचन्द्र ने तपस्वी किया है।' संस्कृत में इस शब्द के दो रूप हो सकते हैं— श्रमणम् और समणम् । विस्तार के लिए देखेंदसवेआलियं १।३ के 'समणा' शब्द का टिप्पण । ५१. (श्लोक २६.२७)
(६) त्याग- - अपने सांभोगिक साधुओं को आहार का दान देना । (१०) ब्रह्मचर्य
प्रस्तुत दो श्लोकों (२६, २७) में आक्रोश, वध आदि परीषों को झेलने के तीन आलंबन सूत्र प्राप्त होते हैं
१. तितिक्षा -मुनि सोचे की सहन करने से बढ़कर
Jain Education International
१. बृहद्वृत्ति पत्र ११४ ।
२. वही, पत्र ११४ परमां धर्मसाधनं प्रति प्रकर्षवतीतितिक्ताम् । उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ. ७२ समो सव्वत्थ मणो जस्स भवति स समणो । ४. बृहद्वृत्ति, पत्र ११४ 'समणं' - श्रमणं सममनसं वा - तथाविधवधेऽपि
३.
धर्म प्रति प्रहितचेतसम् ।
अध्ययन २ : श्लोक २७ टि० ४८-५२ निर्जरा का कोई साधन नहीं है। क्षमा परम धर्म है। सहन करने वाला ही क्षमाशील हो सकता है। एक प्राचीन श्लोक है—
'धर्मस्य दया मूलं, न चाक्षमावान् दयां समाधत्ते । तस्माद यः क्षान्तिपरः, स साधयत्युत्तमं धर्मम् ॥' २. मुनि धर्म का चिंतन करे। मुनि धर्म दो प्रकार का है— पांच महाव्रतात्मक और क्षान्ति आदि दसविध धर्म । मुनि यह सोचे कि मुनि-धर्म का मूल है क्षमा । यह आक्रोश करने वाला व्यक्ति मुझे निमित्त बनाकर कर्मों का उपचय करता है, इसलिए परोक्षतः मैं ही दोषी हूं। अतः मुझे इसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए।
३. आत्मा के अमरत्व का चिन्तन - पीटे जाने पर मुनि यह सोचे कि जीव- -आत्मा का नाश नहीं होता। इस चिन्तन का पूर्वपक्ष है कि यदि कोई दुर्जन व्यक्ति मुनि को गाली दे तो मुनि यह सोचे किचलो, गाली ही देता है, पीटता तो नहीं। पीटने पर सोचे-चलो, पीटता ही है, मारता तो नहीं। मारने पर सोचे चलो मारता ही है, धर्म से भ्रष्ट तो नहीं करता- -आत्म-धर्म का हनन तो नहीं करता, क्योंकि आत्मा अमर है, अमूर्त है।
इस प्रेक्षा से मुनि अगले बड़े उपताप को सामने रखकर छोटा उपताप जो प्राप्त होता है, उसे लाभ मानता है और इस प्रकार वह मनोवैज्ञानिक विजय प्राप्त कर लेता है। ५२. वध परीषह
स्कन्दक श्रावस्ती नगर के जितशत्रु राजा का राजकुमार था। उसकी माता का नाम था धारिणी और बहिन का नाम था पुरंदरयशा । पुरंदरयशा का विवाह कुंभकार नगर के राजा दंडकी के साथ हुआ । पालक दंडकी का पुरोहित था ।
एक बार श्रावस्ती नगरी में मुनि सुव्रत समवसृत हुए। धर्मचर्चा सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े। युवराज स्कन्दक भी गया। धर्मदेशना सुनकर उसने श्रावक के व्रत अंगीकार कर लिए।
एक बार दंडकी राजा का पुरोहित पालक श्रावस्ती नगरी मेंदूत बनकर आया। भरी सभा में वह मुनियों का अवर्णवाद बोलने लगा । स्कन्दक ने उसे निरुत्तर कर दिया। उसी दिन से पालक स्कन्दक का द्वेषी बन गया ।
कुछ समय बीता। स्कन्दक संसार से निर्विण्ण हुआ और उसने पांच सौ व्यक्तियों के साथ मुनि सुव्रत स्वामी के पास प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। उसने ज्ञानाभ्यास कर बहुश्रुतता हासिल कर ली। मुनि सुव्रत स्वामी ने उसकी योग्यता का मूल्यांकन करते हुए उसे पांच सौ शिष्यों का अधिपति बना डाला। एक ५. सुखबोधा, पत्र ३६ 'श्रमणं' तपस्विनम् ।
७.
उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ. ७२ :
अक्कोस हणण मारण धम्मदमंसाण बालसुलभाणं ।
लाभं मन्नति धीरो, जहुत्तराणं अभावमि ।।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org