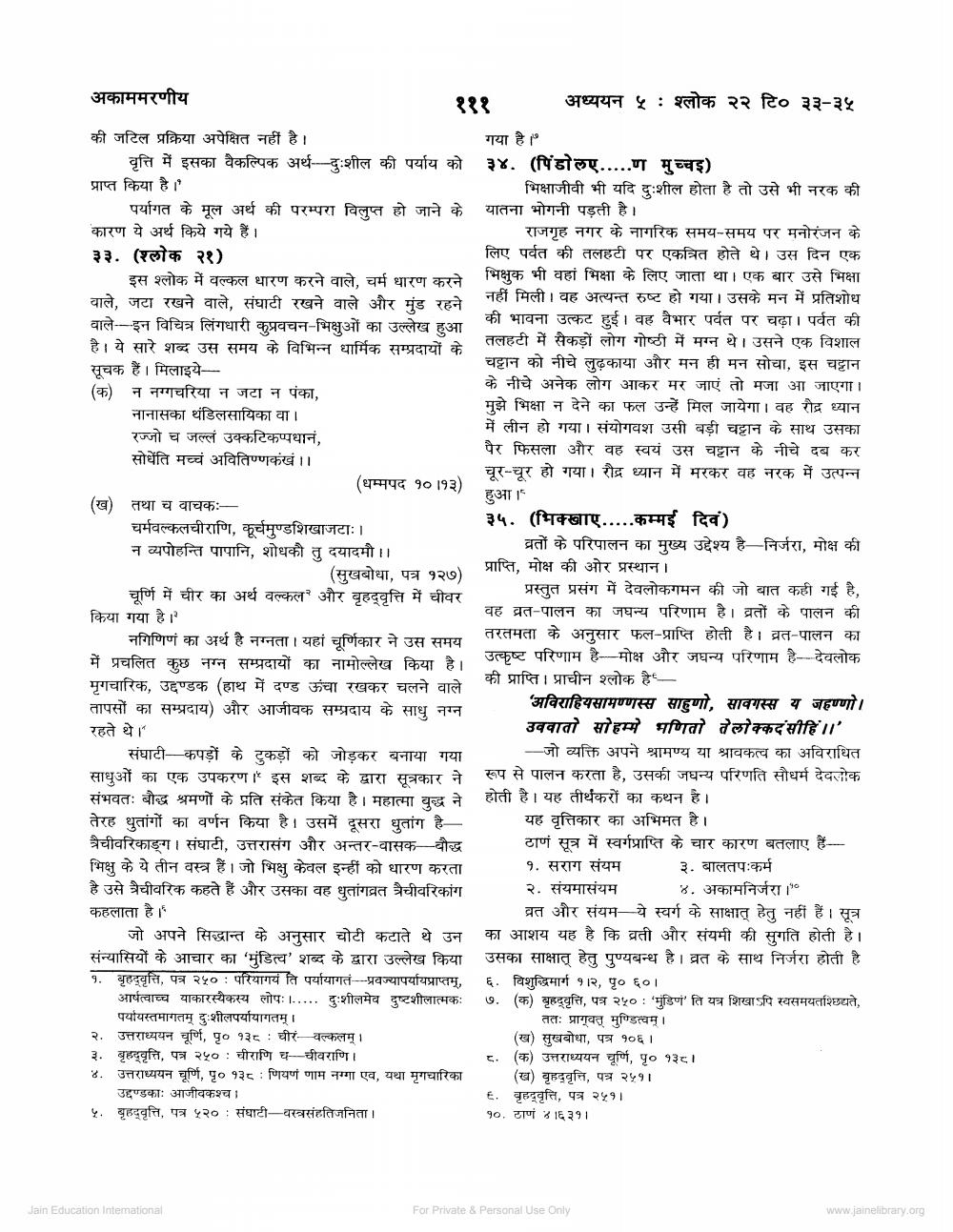________________
अकाममरणीय
१११ अध्ययन ५ : श्लोक २२ टि० ३३-३५ की जटिल प्रक्रिया अपेक्षित नहीं है।
गया है। वृत्ति में इसका वैकल्पिक अर्थ-दुःशील की पर्याय को ३४. (पिंडोलए.....ण मुच्चइ) प्राप्त किया है।'
भिक्षाजीवी भी यदि दुःशील होता है तो उसे भी नरक की पर्यागत के मूल अर्थ की परम्परा विलुप्त हो जाने के यातना भोगनी पड़ती है। कारण ये अर्थ किये गये हैं।
राजगृह नगर के नागरिक समय-समय पर मनोरंजन के ३३. (श्लोक २१)
लिए पर्वत की तलहटी पर एकत्रित होते थे। उस दिन एक इस श्लोक में वल्कल धारण करने वाले, चर्म धारण करने
भिक्षुक भी वहां भिक्षा के लिए जाता था। एक बार उसे भिक्षा वाले, जटा रखने वाले, संघाटी रखने वाले और मुंड रहने
नहीं मिली। वह अत्यन्त रुष्ट हो गया। उसके मन में प्रतिशोध वाले---इन विचित्र लिंगधारी कुप्रवचन-भिक्षुओं का उल्लेख हुआ
की भावना उत्कट हुई। वह वैभार पर्वत पर चढ़ा। पर्वत की है। ये सारे शब्द उस समय के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के
तलहटी में सैकड़ों लोग गोष्ठी में मग्न थे। उसने एक विशाल सूचक हैं। मिलाइये
चट्टान को नीचे लुढ़काया और मन ही मन सोचा, इस चट्टान
के नीचे अनेक लोग आकर मर जाएं तो मजा आ जाएगा। (क) न नग्गचरिया न जटा न पंका,
मुझे भिक्षा न देने का फल उन्हें मिल जायेगा। वह रोद्र ध्यान नानासका थंडिलसायिका वा।
में लीन हो गया। संयोगवश उसी बड़ी चट्टान के साथ उसका रज्जो च जल्लं उक्कटिकप्पधानं,
पैर फिसला और वह स्वयं उस चट्टान के नीचे दब कर सोधेति मच्चं अवितिण्णकंखं ।।
चूर-चूर हो गया। रौद्र ध्यान में मरकर वह नरक में उत्पन्न (धम्मपद १०।१३)
हुआ। (ख) तथा च वाचकःचर्मवल्कलचीराणि, कूर्चमुण्डशिखाजटाः।
३५. (भिक्खाए.....कम्मई दिवं) न व्यपोहन्ति पापानि, शोधको तु दयादमी।।
__ व्रतों के परिपालन का मुख्य उद्देश्य है—निर्जरा, मोक्ष की (सुखबोधा, पत्र १२७)
प्राप्ति, मोक्ष की ओर प्रस्थान। चूर्णि में चीर का अर्थ वल्कल और बृहवृत्ति में चीवर
प्रस्तुत प्रसंग में देवलोकगमन की जो बात कही गई है, किया गया है।
वह व्रत-पालन का जघन्य परिणाम है। व्रतों के पालन की __ नगिणिणं का अर्थ है नग्नता। यहां चूर्णिकार ने उस समय
तरतमता के अनुसार फल-प्राप्ति होती है। व्रत-पालन का में प्रचलित कुछ नग्न सम्प्रदायों का नामोल्लेख किया है।
उत्कृष्ट परिणाम है-मोक्ष और जघन्य परिणाम है-देवलोक मृगचारिक, उद्दण्डक (हाथ में दण्ड ऊंचा रखकर चलने वाले
की प्राप्ति । प्राचीन श्लोक हैतापसों का सम्प्रदाय) और आजीवक सम्प्रदाय के साधु नग्न
'अविराहियसामण्णस्स साहुणो, सावगस्स य जहण्णो। रहते थे।
उववातो सोहम्मे भणितो तेलोक्कदंसीहिं।।' ____ संघाटी—कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया -जो व्यक्ति अपने श्रामण्य या श्रावकत्व का अविराधित साधुओं का एक उपकरण।' इस शब्द के द्वारा सत्रकार ने रूप से पालन करता है, उसकी जघन्य परिणति सौधर्म देवलोक संभवतः बौद्ध श्रमणों के प्रति संकेत किया है। महात्मा बद्ध ने होती है। यह तीर्थंकरों का कथन है। तेरह धुतांगों का वर्णन किया है। उसमें दूसरा धुतांग है
यह वृत्तिकार का अभिमत है। त्रैचीवरिकाङ्ग। संघाटी, उत्तरासंग और अन्तर-वासक-बौद्ध ठाणं सूत्र में स्वर्गप्राप्ति के चार कारण बतलाए हैं--- भिक्षु के ये तीन वस्त्र हैं। जो भिक्षु केवल इन्हीं को धारण करता १. सराग संयम ३. बालतपःकर्म है उसे त्रैचीवरिक कहते हैं और उसका वह धुतांगव्रत त्रैचीवरिकांग २. संयमासंयम ४. अकामनिर्जरा।'० कहलाता है।
व्रत और संयम—ये स्वर्ग के साक्षात् हेतु नहीं हैं। सूत्र जो अपने सिद्धान्त के अनुसार चोटी कटाते थे उन का आशय यह है कि व्रती और संयमी की सुगति होती है। संन्यासियों के आचार का 'मुंडित्व' शब्द के द्वारा उल्लेख किया उसका साक्षात् हेतु पुण्यबन्ध है। व्रत के साथ निर्जरा होती है १. बृहद्वृत्ति, पत्र २५० : परियागयं ति पर्यायागतं--प्रवज्यापर्यायप्राप्तम्, ६. विशुद्धिमार्ग १२, पृ०६०।
आर्षत्वाच्च याकारस्यैकस्य लोपः ।..... दुःशीलमेव दुष्टशीलात्मकः ७. (क) बृहवृत्ति, पत्र २५० : 'मुंडिणं' ति यत्र शिखाऽपि स्वसमयतश्छिद्यते, पर्यायस्तमागतम् दुःशीलपर्यायागतम्।
ततः प्राग्वत् मुण्डित्वम्। उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३८ : चीरं—वल्कलम् ।
(ख) सुखबोधा, पत्र १०६ । ३. बृहद्वृत्ति, पत्र २५० : चीराणि च-चीवराणि।
८. (क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३८ । ४. उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३८ : णियणं णाम नग्गा एव, यथा मृगचारिका (ख) बृहद्वृत्ति, पत्र २५१। उद्दण्डकाः आजीवकश्च।
६. बृहवृत्ति, पत्र २५१। ५. बृहवृत्ति, पत्र ५२० : संघाटी-वस्त्रसंहतिजनिता।
१०. ठाणं 31६३१।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org