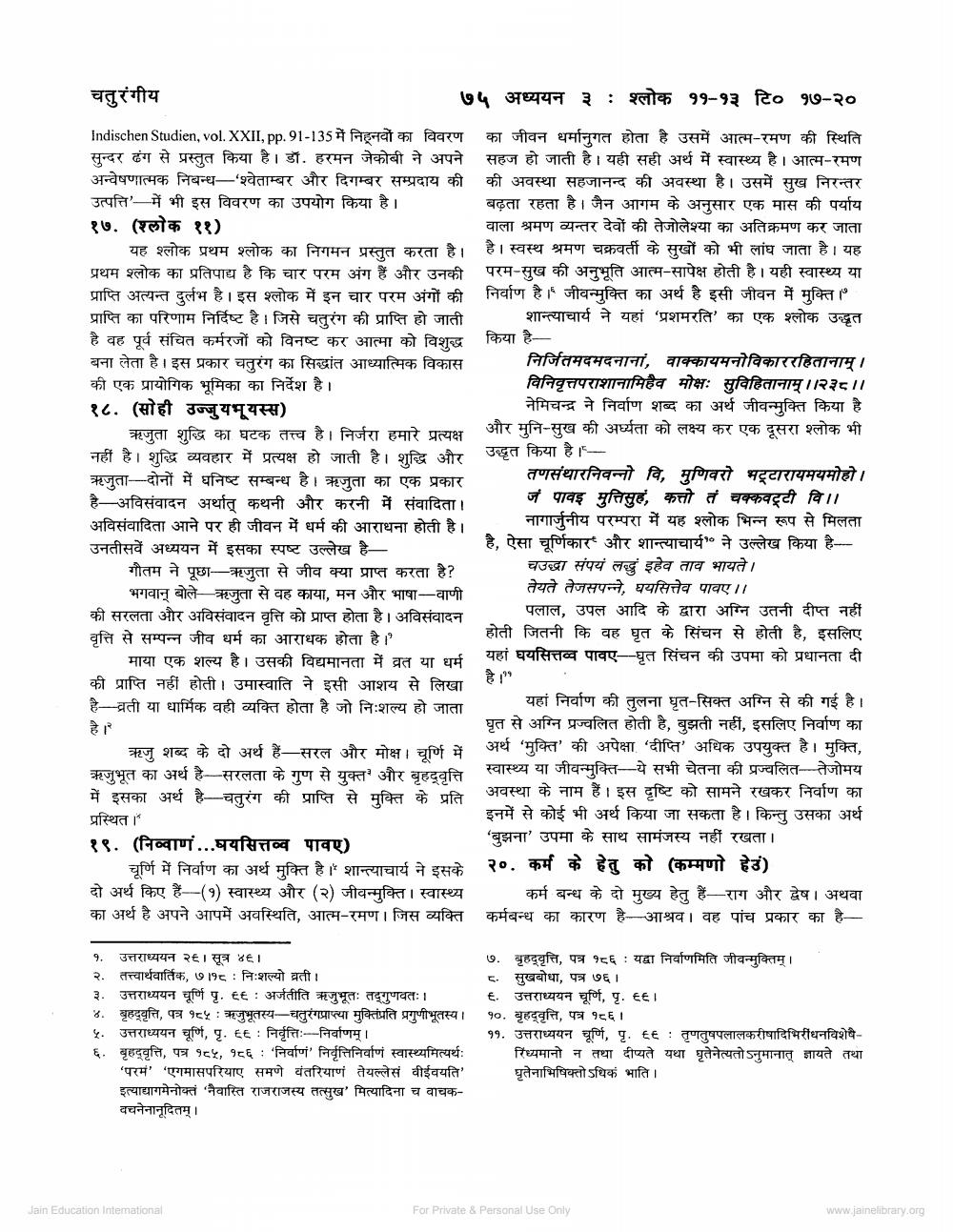________________
चतुरंगीय
Indischen Studien, vol. XXII, pp. 91-135 में निहूनवों का विवरण सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। डॉ. हरमन जेकोबी ने अपने अन्वेषणात्मक निबन्ध— 'श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति' में भी इस विवरण का उपयोग किया है। १७. (श्लोक ११)
यह श्लोक प्रथम श्लोक का निगमन प्रस्तुत करता है। प्रथम श्लोक का प्रतिपाद्य है कि चार परम अंग हैं और उनकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। इस श्लोक में इन चार परम अंगों की प्राप्ति का परिणाम निर्दिष्ट है। जिसे चतुरंग की प्राप्ति हो जाती है वह पूर्व संचित कर्मरजों को विनष्ट कर आत्मा को विशुद्ध बना लेता है। इस प्रकार चतुरंग का सिद्धांत आध्यात्मिक वि की एक प्रायोगिक भूमिका का निर्देश है।
१८. (सोही उज्जुयभूयस्स)
७५ अध्ययन ३ : श्लोक ११-१३ टि० १७-२०
का जीवन धर्मानुगत होता है उसमें आत्म-रमण की स्थिति सहज हो जाती है। यही सही अर्थ में स्वास्थ्य है। आत्म-रमण की अवस्था सहजानन्द की अवस्था है । उसमें सुख निरन्तर बढ़ता रहता है। जैन आगम के अनुसार एक मास की पर्याय वाला श्रमण व्यन्तर देवों की तेजोलेश्या का अतिक्रमण कर जाता है । स्वस्थ श्रमण चक्रवर्ती के सुखों को भी लांघ जाता है। यह परम सुख की अनुभूति आत्म-सापेक्ष होती है । यही स्वास्थ्य या निर्वाण है। जीवन्मुक्ति का अर्थ है इसी जीवन में मुक्ति ।"
शान्त्याचार्य ने यहां 'प्रशमरति' का एक श्लोक उद्धृत किया है
ऋजुता शुद्धि का घटक तत्त्व है। निर्जरा हमारे प्रत्यक्ष नहीं है। शुद्धि व्यवहार में प्रत्यक्ष हो जाती है। शुद्धि और ऋजुता — दोनों में घनिष्ट सम्बन्ध है। ऋजुता का एक प्रकार है— अविसंवादन अर्थात् कथनी और करनी में संवादिता । अविसंवादिता आने पर ही जीवन में धर्म की आराधना होती है। उनतीसवें अध्ययन में इसका स्पष्ट उल्लेख है
गौतम ने पूछा- ऋजुता से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान् बोले- ऋजुता से वह काया, मन और भाषा - वाणी की सरलता और अविसंवादन वृत्ति को प्राप्त होता है। अविसंवादन वृत्ति से सम्पन्न जीव धर्म का आराधक होता है।'
माया एक शल्य है। उसकी विद्यमानता में व्रत या धर्म की प्राप्ति नहीं होती । उमास्वाति ने इसी आशय से लिखा है—व्रती या धार्मिक वही व्यक्ति होता है जो निःशल्य हो जाता है ।
ऋजु शब्द के दो अर्थ हैं— सरल और मोक्ष । चूर्णि में ऋजुभूत का अर्थ है- सरलता के गुण युक्त' और बृहद्वृत्ति में इसका अर्थ है चतुरंग की प्राप्ति से मुक्ति के प्रति प्रस्थित ।*
१९. (निव्वाणं... पयसित्तव्य पावए)
चूर्णि में निर्वाण का अर्थ मुक्ति है। शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं— (१) स्वास्थ्य और (२) जीवन्मुक्ति । स्वास्थ्य का अर्थ है अपने आपमें अवस्थिति, आत्म-रमण। जिस व्यक्ति
9.
उत्तराध्ययन २६ । सूत्र ४६ ।
२. तत्त्वार्थवार्तिक, ७।१८ : निःशल्यो व्रती ।
३. उत्तराध्ययन चूर्णि पृ. ६६ अर्जतीति ऋजुभूतः तद्गुणवतः ।
४. बृहद्वृत्ति, पत्र १८५ ऋजुभूतस्य चतुरंगप्राप्त्या मुक्तिंप्रति प्रगुणीभूतस्य । ५. उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ. ६६ : निर्वृत्तिः निर्वाणम् ।
६. बृहद्वृत्ति, पत्र १८५, १८६ : 'निर्वाणं' निर्वृत्तिनिर्वाणं स्वास्थ्यमित्यर्थः 'परम' 'एगमासपरियाए समणे वंतरियाणं तेयल्लेसं वीईवयति' इत्याद्यागमेनोक्तं 'नैवास्ति राजराजस्य तत्सुख' मित्यादिना च वाचकवचनेनानूदितम् ।
Jain Education International
निर्जितमदभवनानां वाक्कायमनोविकाररहितानाम् । विनिवृत्तपराशानामिहैव मोक्षः सुविहितानाम् ।।२३८ ।। नेमिचन्द्र ने निर्वाण शब्द का अर्थ जीवन्मुक्ति किया है। और मुनि-सुख की अर्घ्यता को लक्ष्य कर एक दूसरा श्लोक भी उद्धृत किया है। -
तणसंधारनिवन्नो वि, मुणिवरी भट्टारायमयमोहो। जं पावह मुत्तिसुहं, कत्तो तं चक्कवटी वि। नागार्जुनीय परम्परा में यह श्लोक भिन्न रूप से मिलता है, ऐसा चूर्णिकार और शान्त्वाचार्य ने उल्लेख किया है-
चउद्धा संपयं लद्धुं इहेव ताव भायते ।
तेयते तेजसपन्ने, घयसित्तेव पावए ।।
पलाल, उपल आदि के द्वारा अग्नि उतनी दीप्त नहीं होती जितनी कि वह घृत के सिंचन से होती है, इसलिए यहां घयसित्तव्व पाव-घृत सिंचन की उपमा को प्रधानता दी है ।"
यहां निर्वाण की तुलना घृत-सिक्त अग्नि से की गई है। घृत से अग्नि प्रज्वलित होती है, बुझती नहीं, इसलिए निर्वाण का अर्थ 'मुक्ति' की अपेक्षा 'दीप्ति' अधिक उपयुक्त है। मुक्ति, स्वास्थ्य या जीवन्मुक्ति- ये सभी चेतना की प्रज्वलित-तेजोमय अवस्था के नाम हैं। इस दृष्टि को सामने रखकर निर्वाण का इनमें से कोई भी अर्थ किया जा सकता है। किन्तु उसका अर्थ 'बुझना' उपमा के साथ सामंजस्य नहीं रखता। २०. कर्म के हेतु को (कम्मणो हेउ)
कर्म बन्ध के दो मुख्य हेतु हैं- -राग और द्वेष अथवा कर्मबन्ध का कारण है-आश्रव। वह पांच प्रकार का है
बृहद्वृत्ति, पत्र १८६ : यद्वा निर्वाणमिति जीवन्मुक्तिम् । सुखबोधा, पत्र ७६ ।
उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ. ६६ ।
७.
८.
६.
१०. बृहद्वृत्ति, पत्र १८६ ।
११. उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ. ६६: तृणतुषपलालकरीषादिभिरींधनविशेषरिंध्यमानो न तथा दीप्यते यथा घृतेनेत्यतोऽनुमानात् ज्ञायते तथा घृतेनाभिषिक्तोऽधिकं भाति ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org