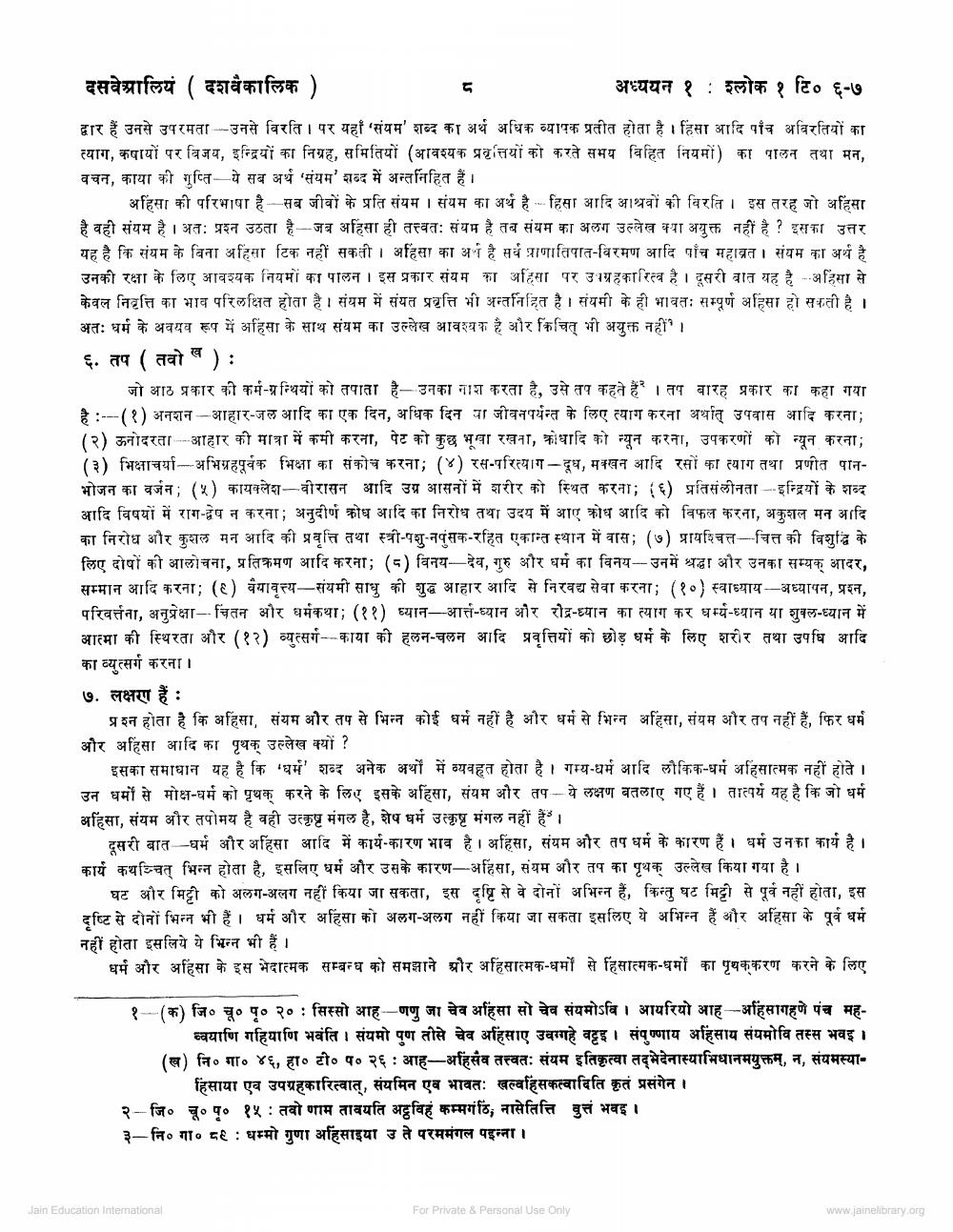________________
दसवेआलियं ( दशवकालिक )
अध्ययन १ : श्लोक १०६-७
द्वार हैं उनसे उपरमता --उनसे विरति । पर यहाँ 'संयम' शब्द का अर्थ अधिक व्यापक प्रतीत होता है । हिंसा आदि पाँच अविरतियों का त्याग, कषायों पर विजय, इन्द्रियों का निग्रह, समितियों (आवश्यक प्रवृत्तियों को करते समय विहित नियमों) का पालन तथा मन, वचन, काया की गुप्ति—ये सब अर्थ 'संयम' शब्द में अन्तनिहित हैं।
अहिंसा की परिभाषा है-सब जीवों के प्रति संयम । संयम का अर्थ है ---हिसा आदि आश्रवों की विरति । इस तरह जो अहिंसा है वही संयम है । अत: प्रश्न उठता है-जब अहिंसा ही तत्त्वत: संयम है तब संयम का अलग उल्लेख क्या अयुक्त नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि संयम के बिना अहिंसा टिक नहीं सकती। अहिंसा का अर्थ है सर्व प्राणातिपात-विरमण आदि पाँच महाव्रत। संयम का अर्थ है उनकी रक्षा के लिए आवश्यक नियमों का पालन । इस प्रकार संयम का अहिंसा पर उपग्रहकारित्व है। दूसरी बात यह है ...अहिंसा से केवल निवृत्ति का भाव परिलक्षित होता है। संयम में संयत प्रवृत्ति भी अन्तनिहित है। संयमी के ही भावतः सम्पूर्ण अहिंसा हो सकती है। अतः धर्म के अवयव रूप में अहिंसा के साथ संयम का उल्लेख आवश्यक है और किंचित् भी अयुक्त नहीं। ६. तप ( तवो ख ):
जो आठ प्रकार की कर्म-ग्रन्थियों को तपाता है-उनका नाश करता है, उसे तप कहते हैं । तप बारह प्रकार का कहा गया है :---(१) अनशन -आहार-जल आदि का एक दिन, अधिक दिन वा जीवनपर्यन्त के लिए त्याग करना अर्थात् उपवास आदि करना; (२) ऊनोदरता...-आहार की मात्रा में कमी करना, पेट को कुछ भूखा रखना, क्रोधादि को न्यून करना, उपकरणों को न्यून करना; (३) भिक्षाचर्या-अभिग्रहपूर्वक भिक्षा का संकोच करना; (४) रस-परित्याग-दूध, मक्खन आदि रसों का त्याग तथा प्रणीत पानभोजन का वर्जन; (५) कायक्लेश-वीरासन आदि उग्र आसनों में शरीर को स्थित करना; (६) प्रतिसंलीनता --इन्द्रियों के शब्द आदि विषयों में राग-द्वेष न करना; अनुदीर्ण क्रोध आदि का निरोध तथा उदय में आए क्रोध आदि को विफल करना, अकुशल मन आदि का निरोध और कुशल मन आदि की प्रवृत्ति तथा स्त्री-पशु-नपुंसक-रहित एकान्त स्थान में वास; (७) प्रायश्चित्त-चित्त की विशुद्धि के लिए दोषों की आलोचना, प्रतिक्रमण आदि करना; (८) विनय-देव, गुरु और धर्म का विनय- उनमें श्रद्धा और उनका सम्यक् आदर, सम्मान आदि करना; (६) वयावृत्त्य-संयमी साधु की शुद्ध आहार आदि से निरवद्य सेवा करना; (१०) स्वाध्याय-अध्यापन, प्रश्न, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा--चिंतन और धर्मकथा; (११) ध्यान—आर्त्त-ध्यान और रौद्र-ध्यान का त्याग कर धर्म्य-ध्यान या शुक्ल-ध्यान में आत्मा की स्थिरता और (१२) व्युत्सर्ग--काया की हलन-चलन आदि प्रवृत्तियों को छोड़ धर्म के लिए शरीर तथा उपधि आदि का व्युत्सर्ग करना। ७. लक्षरण हैं :
प्रश्न होता है कि अहिंसा, संयम और तप से भिन्न कोई धर्म नहीं है और धर्म से भिन्न अहिंसा, संयम और तप नहीं हैं, फिर धर्म और अहिंसा आदि का पृथक् उल्लेख क्यों ?
इसका समाधान यह है कि 'धर्म' शब्द अनेक अर्थों में व्यवहुत होता है। गम्य-धर्म आदि लौकिक-धर्म अहिंसात्मक नहीं होते। उन धर्मों से मोक्ष-धर्म को पृथक् करने के लिए इसके अहिंसा, संयम और तप-ये लक्षण बतलाए गए हैं। तात्पर्य यह है कि जो धर्म अहिंसा, संयम और तपोमय है वही उत्कृष्ट मंगल है, शेष धर्म उत्कृष्ट मंगल नहीं हैं।
दूसरी बात -धर्म और अहिंसा आदि में कार्य-कारण भाव है। अहिंसा, संयम और तप धर्म के कारण हैं। धर्म उनका कार्य है। कार्य कथञ्चित् भिन्न होता है, इसलिए धर्म और उसके कारण-अहिंसा, संयम और तप का पृथक् उल्लेख किया गया है।
घट और मिट्टी को अलग-अलग नहीं किया जा सकता, इस दृष्टि से वे दोनों अभिन्न हैं, किन्तु घट मिट्टी से पूर्व नहीं होता, इस दष्टि से दोनों भिन्न भी हैं। धर्म और अहिंसा को अलग-अलग नहीं किया जा सकता इसलिए ये अभिन्न हैं और अहिंसा के पूर्व धर्म नहीं होता इसलिये ये भिन्न भी हैं ।
धर्म और अहिंसा के इस भेदात्मक सम्बन्ध को समझाने और अहिंसात्मक-धर्मों से हिंसात्मक-धर्मों का पृथककरण करने के लिए
१-(क) जि० चू० पृ० २०: सिस्सो आह—णणु जा चेव अहिंसा सो चेव संयमोऽवि । आयरियो आह --अहिंसागहणे पंच मह
__ व्वयाणि गहियाणि भवंति । संयमो पुण तोसे चेव अहिंसाए उवग्गहे वट्टइ। संपुण्णाय अहिंसाय संयमोवि तस्स भवइ । (ख) नि० गा० ४६, हा० टी० ५० २६ : आह-अहिंसव तत्त्वतः संयम इतिकृत्वा तद्भेदेनास्याभिधानमयुक्तम्, न, संयमस्या
हिंसाया एव उपग्रहकारित्वात्, संयमिन एव भावत: खल्वहिंसकत्वादिति कृतं प्रसंगेन । २-जि० चू० पृ० १५ : तवो णाम तावयति अट्ठविहं कम्मगंठिं, नासेतित्ति वुत्तं भवइ । ३-नि० गा० ८६ : धम्मो गुणा अहिंसाइया उ ते परममंगल पइन्ना।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org