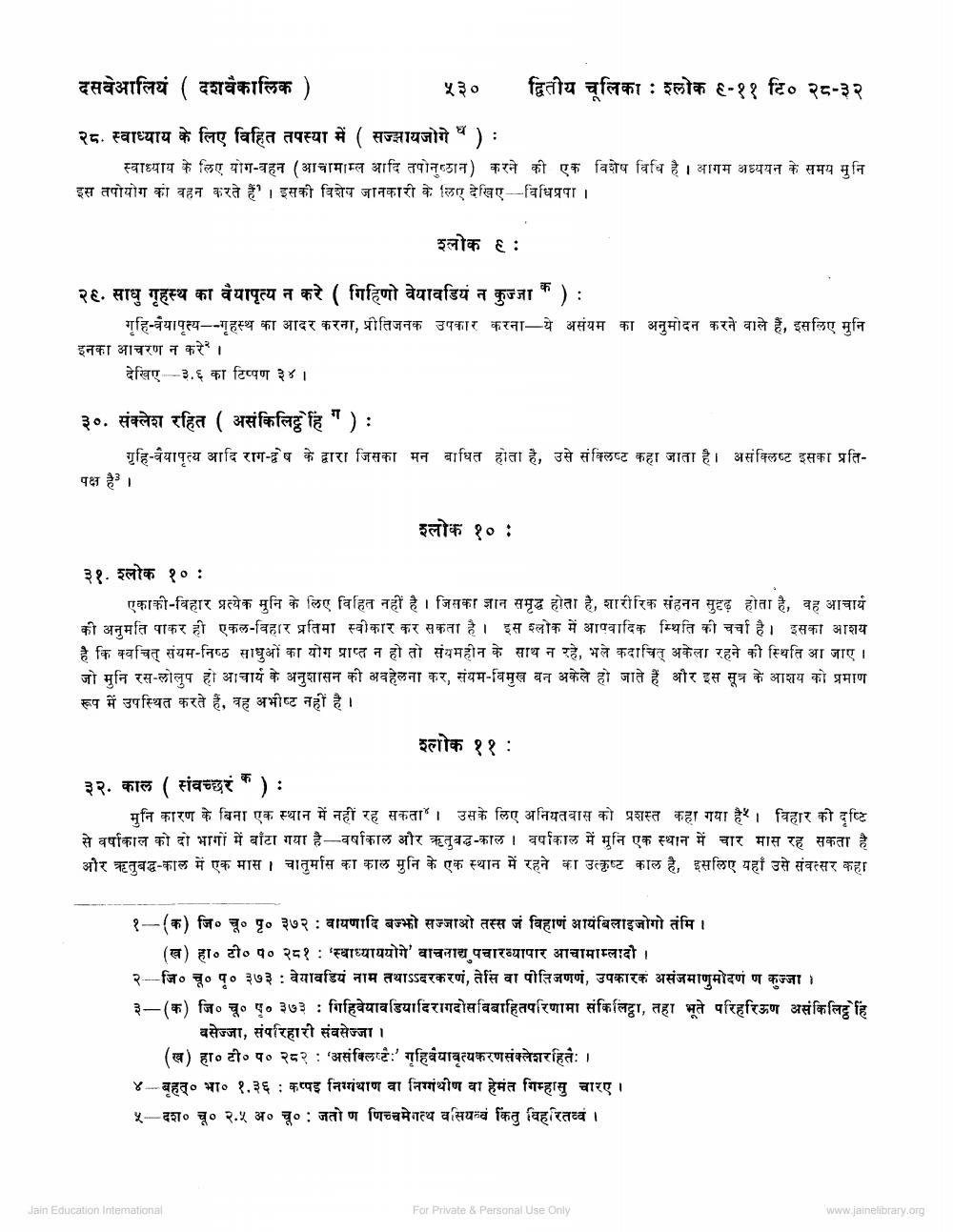________________
दसवेआलियं ( दशवैकालिक )
५३०
द्वितीय चूलिका : श्लोक ६-११ टि० २८-३२
२८. स्वाध्याय के लिए विहित तपस्या में ( सज्झायजोगे ५ ):
स्वाध्याय के लिए योग-वहन (आचामाम्ल आदि तपोनुष्ठान) करने की एक विशेष विधि है । आगम अध्ययन के समय मुनि इस तपोयोग को वहन करते हैं। इसकी विशेष जानकारी के लिए देखिए-विधिप्रपा ।
श्लोक ६:
२६. साधु गृहस्थ का वैयापृत्य न करे ( गिहिणो वेयावडियं न कुज्जा क ):
गाह-वयापत्य--गृहस्थ का आदर करना, प्रीतिजनक उपकार करना—ये असंयम का अनुमोदन करने वाले हैं, इसलिए मुनि इनका आचरण न करे।
देखिए-३.६ का टिप्पण ३४ ।
३०. संक्लेश रहित ( असंकिलि?हिंग ) :
गृहि-वयापृत्य आदि राग-द्वेष के द्वारा जिसका मन बाधित होता है, उसे संक्लिष्ट कहा जाता है। असं क्लिष्ट इसका प्रतिपक्ष है।
श्लोक १०:
३१. श्लोक १०:
एकाकी-विहार प्रत्येक मुनि के लिए विहित नहीं है । जिसका ज्ञान समृद्ध होता है, शारीरिक संहनन सुदृढ़ होता है, वह आचार्य की अनुमति पाकर ही एकल-विहार प्रतिमा स्वीकार कर सकता है। इस श्लोक में आपवादिक स्थिति की चर्चा है। इसका आशय है कि क्वचित् संयम-निष्ठ साधुओं का योग प्राप्त न हो तो संयमहीन के साथ न रहे, भले कदाचित् अकेला रहने की स्थिति आ जाए। जो मुनि रस-लोलुप हो आचार्य के अनुशासन की अवहेलना कर, संयम-विमुख बन अकेले हो जाते हैं और इस सूत्र के आशय को प्रमाण रूप में उपस्थित करते हैं, वह अभीष्ट नहीं है।
श्लोक ११:
३२. काल ( संवच्छरंक):
मुनि कारण के बिना एक स्थान में नहीं रह सकता। उसके लिए अनियतवास को प्रशस्त कहा गया है। विहार को दृष्टि से वर्षाकाल को दो भागों में बाँटा गया है-वर्षाकाल और ऋतुबद्ध-काल । वर्षाकाल में मुनि एक स्थान में चार मास रह सकता है और ऋतुबद्ध-काल में एक मास । चातुर्मास का काल मुनि के एक स्थान में रहने का उत्कृष्ट काल है, इसलिए यहाँ उसे संवत्सर कहा
१-(क) जि. चू० पृ० ३७२ : वायणादि बन्झो सज्जाओ तस्स जं विहाणं आयंबिलाइजोगो तंमि ।
(ख) हा० टी०५० २८१ : 'स्वाध्याययोगे' वाचनाद्य पचारव्यापार आचामाम्लादौ। २-जि० चू० पृ० ३७३ : वेयावडियं नाम तथाऽऽदरकरणं, तेसि वा पोलिजणणं, उपकारक असंजमाणुमोदणं ण कुज्जा । ३-(क) जि० चू० पृ. ३७३ : गिहिवयावडियादिरागदोसविबाहितपरिणामा संकिलिट्ठा, तहा भूते परिहरिऊण असंकिलिटेहि
वसेज्जा, संपरिहारी संवसेज्जा। (ख) हा० टी०प० २८२ : 'असंक्लिप्टः' गहिवंयावत्यकरणसंक्लेशरहितः । ४.-- बृहत् भा० १.३६ : कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा हेमंत गिम्हासु चारए । ५-दश० चू० २.५ अ० चू० : जतो ण णिच्चमेगत्थ वसियव्वं किंतु विहरितव्वं ।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org