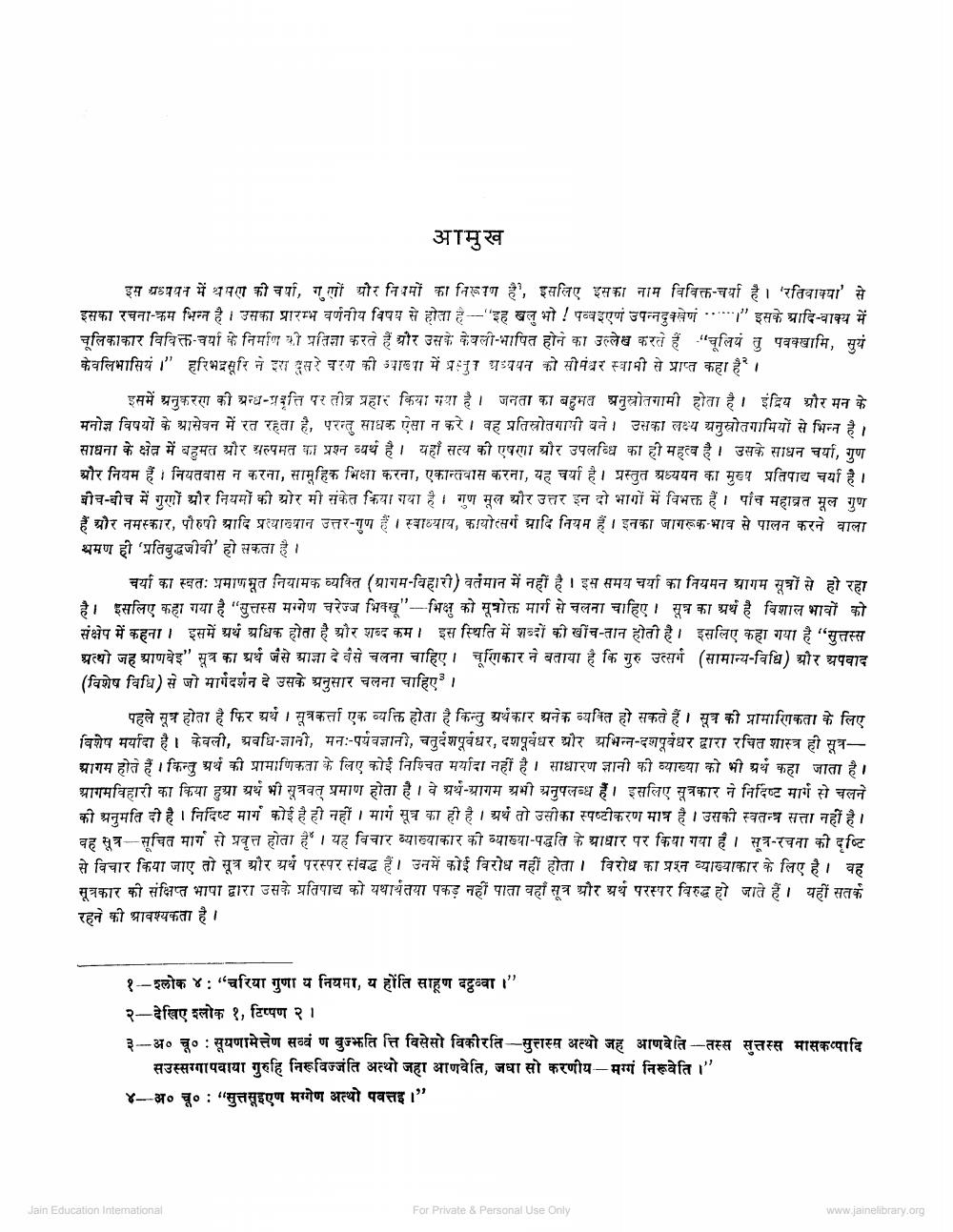________________
आमुख
इस अध्ययन में थपण की वर्षा, गुणों और नियमों का निरूपण है, इसलिए इसका नाम विविक्त-चर्या है। 'रतिवाक्या' से इसका रचना-क्रम भिन्न है । उसका प्रारम्भ वर्णनीय विषय से होता है - "इह खलु भो ! पब्वइएणं उपन्नदुक्खेणं ....।" इसके प्रादि-वाक्य में चूलिकाकार विविक्त-चर्या के निर्माण की प्रतिज्ञा करते हैं और उसके केवली-भाषित होने का उल्लेख करते हैं "चूलियं तु पवक्खामि, सुर्य केवलिभासियं ।" हरिभद्रसूरि ने इस दूसरे चरण की पापा में प्रना अध्ययन को सीमंधर स्वामी से प्राप्त कहा है।
इसमें अनुकरण की अन्ध-प्रवृत्ति पर तीव्र प्रहार किया गया है। जनता का बहुमत अनुस्रोतगामी होता है। इंद्रिय और मन के मनोज्ञ विषयों के प्रासेवन में रत रहता है, परन्तु साधक ऐसा न करे। वह प्रतिस्रोतगामी बने। उसका लक्ष्य अनुस्रोतगामियों से भिन्न है। साधना के क्षेत्र में बहुमत और अल्पमत का प्रश्न व्यर्थ है। यहाँ सत्य की एषणा और उपलब्धि का ही महत्व है। उसके साधन चर्या, गुण
और नियम हैं । नियतवास न करना, सामूहिक भिक्षा करना, एकान्तवास करना, यह चर्या है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य प्रतिपाद्य चर्या है। बीच-बीच में गुणों और नियमों की अोर मी संकेत किया गया है। गुण मूल और उत्तर इन दो भागों में विभक्त हैं। पांच महाव्रत मूल गुण हैं और नमस्कार, पौरुषी आदि प्रत्याख्यान उत्तर-गुण हैं । स्वाध्याय, कायोत्सर्ग प्रादि नियम हैं । इनका जागरूक-भाव से पालन करने वाला श्रमण ही 'प्रतिबुद्धजीवी' हो सकता है।
चर्या का स्वतः प्रमाणभूत नियामक व्यक्ति (पागम-विहारी) वर्तमान में नहीं है । इस समय चर्या का नियमन प्रागम सूत्रों से हो रहा है। इसलिए कहा गया है "सुत्तस्स मग्गेण चरेज्ज भिक्खू"--भिक्षु को सूत्रोक्त मार्ग से चलना चाहिए। सूत्र का अर्थ है विशाल भावों को संक्षेप में कहना। इसमें अर्थ अधिक होता है और शब्द कम। इस स्थिति में शब्दों की खींच-तान होती है। इसलिए कहा गया है "सुत्तस्स प्रत्थो जहाणवेइ" सूत्र का अर्थ जैसे आज्ञा दे वैसे चलना चाहिए। चूर्णिकार ने बताया है कि गुरु उत्सर्ग (सामान्य-विधि) और अपवाद (विशेष विधि) से जो मार्गदर्शन दे उसके अनुसार चलना चाहिए।
पहले सूत्र होता है फिर अर्थ । सूत्रकर्ता एक व्यक्ति होता है किन्तु अर्थकार अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। सूत्र की प्रामाणिकता के लिए विशेष मर्यादा है। केवली, अवधि-ज्ञानी, मनः-पर्यवज्ञानी, चतुर्दशपूर्वधर, दशपूर्वधर और अभिन्न-दशपूर्वधर द्वारा रचित शास्त्र ही सूत्रपागम होते हैं । किन्तु अर्थ की प्रामाणिकता के लिए कोई निश्चित मर्यादा नहीं है। साधारण ज्ञानी की व्याख्या को भी अर्थ कहा जाता है। प्रागमविहारी का किया हुअा अर्थ भी सूत्रवत् प्रमाण होता है । वे अर्थ-पागम अभी अनुपलब्ध हैं। इसलिए सूत्रकार ने निर्दिष्ट मार्ग से चलने की अनुमति दी है । निर्दिष्ट मार्ग कोई है ही नहीं । मार्ग सूत्र का ही है । अर्थ तो उसीका स्पष्टीकरण मात्र है । उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। वह सूत्र-सूचित मार्ग से प्रवृत्त होता है । यह विचार व्याख्याकार की व्याख्या-पद्धति के अाधार पर किया गया है। सूत्र-रचना की दृष्टि से विचार किया जाए तो सूत्र और अर्थ परस्पर संबद्ध हैं। उनमें कोई विरोध नहीं होता। विरोध का प्रश्न व्याख्याकार के लिए है। वह सुत्रकार की संक्षिप्त भाषा द्वारा उसके प्रतिपाद्य को यथार्थतया पकड़ नहीं पाता वहाँ सूत्र और अर्थ परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं। यहीं सतर्क रहने की आवश्यकता है।
१-श्लोक ४ : "चरिया गुणा य नियमा, य होंति साहूण दट्ठव्वा ।" २-देखिए श्लोक १, टिप्पण २। ३----अ० चु० : सूयणामेत्तेण सव्वं ण बुज्झति त्ति विसेसो विकीरति-सुत्तस्स अत्थो जह आणवेति-तस्स सुत्तस्स मासकप्पादि
सउस्सग्गापवाया गुरुहि निरूविज्जंति अत्थो जहा आणवेति, जधा सो करणीय-मग्गं निरूवेति ।" ४--अ० चू० : "सुत्तसूइएण मग्गेण अत्थो पवत्तइ।"
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org