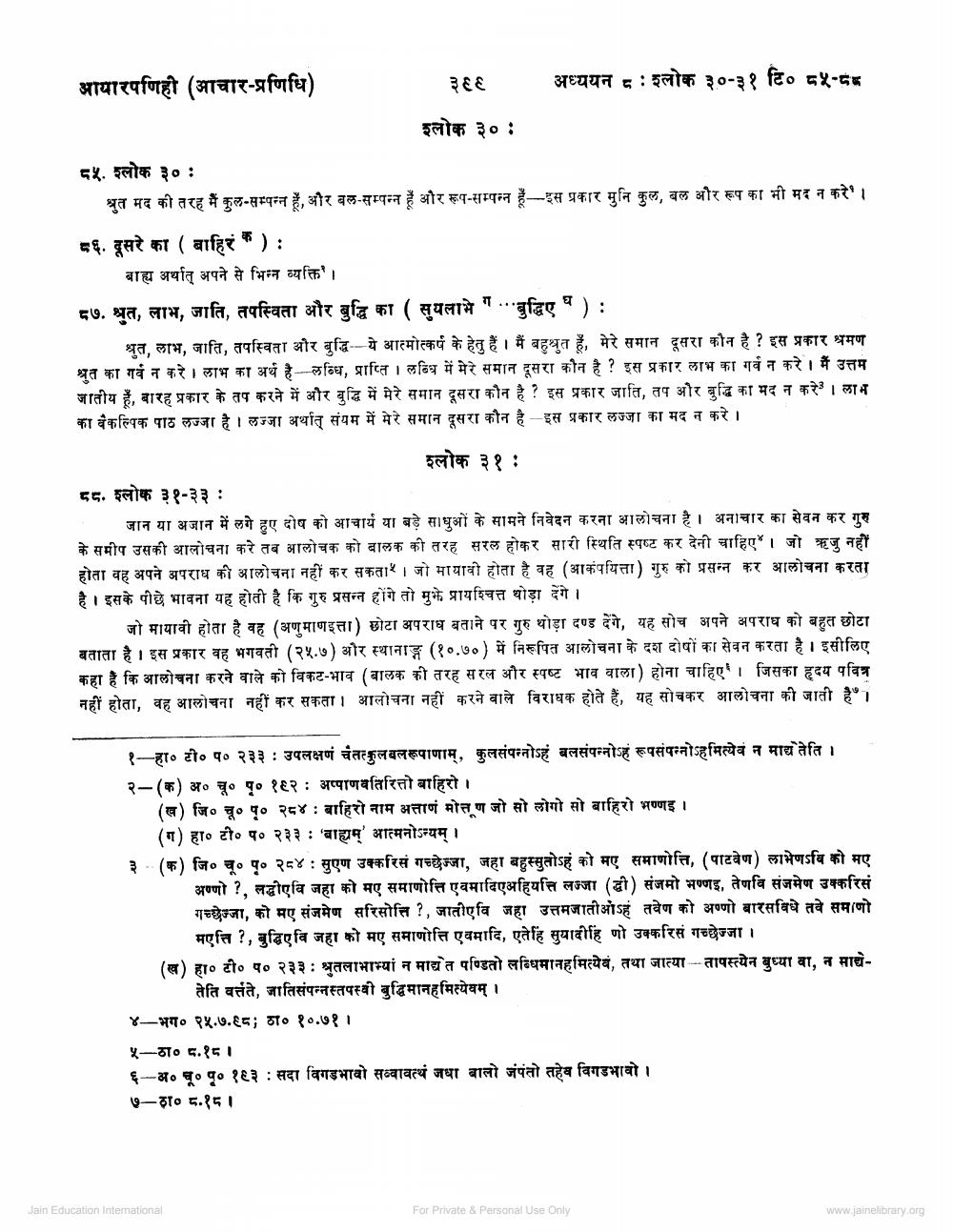________________
आयारपणिही (आचार-प्रणिधि)
३९६ अध्ययन ८ : श्लोक ३०-३१ टि० ८५-८६
श्लोक ३० ८५. श्लोक ३० ___ श्रुत मद की तरह मैं कुल-सम्पन्न हूँ, और बल-सम्पन्न हूँ और रूप-सम्पन्न हूँ-इस प्रकार मुनि कुल, बल और रूप का भी मद न करे। ८६. दूसरे का ( बाहिरं क ) :
___ बाह्य अर्थात् अपने से भिन्न व्यक्ति'। ८७. श्रुत, लाभ, जाति, तपस्विता और बुद्धि का ( सुयलाभे ग .'बुद्धिए ) :
श्रुत, लाभ, जाति, तपस्विता और बुद्धि-ये आत्मोत्कर्ष के हेतु हैं । मैं बहुश्रुत हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है ? इस प्रकार श्रमण श्रुत का गर्व न करे । लाभ का अर्थ है-लब्धि, प्राप्ति । लब्धि में मेरे समान दूसरा कौन है ? इस प्रकार लाभ का गर्व न करे । मैं उत्तम जातीय हूँ, बारह प्रकार के तप करने में और बुद्धि में मेरे समान दूसरा कौन है ? इस प्रकार जाति, तप और बुद्धि का मद न करे । लाभ का वैकल्पिक पाठ लज्जा है। लज्जा अर्थात् संयम में मेरे समान दूसरा कौन है – इस प्रकार लज्जा का मद न करे।
श्लोक ३१ ५८. श्लोक ३१-३३ :
जान या अजान में लगे हुए दोष को आचार्य या बड़े साधुओं के सामने निवेदन करना आलोचना है। अनाचार का सेवन कर गुरु के समीप उसकी आलोचना करे तब आलोचक को बालक की तरह सरल होकर सारी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। जो ऋजु नहीं होता वह अपने अपराध की आलोचना नहीं कर सकता । जो मायावी होता है वह (आकंपयित्ता) गुरु को प्रसन्न कर आलोचना करता है। इसके पीछे भावना यह होती है कि गुरु प्रसन्न होंगे तो मुझे प्रायश्चित्त थोड़ा देंगे।
जो मायावी होता है वह (अणुमाणइत्ता) छोटा अपराध बताने पर गुरु थोड़ा दण्ड देंगे, यह सोच अपने अपराध को बहुत छोटा बताता है । इस प्रकार वह भगवती (२५.७) और स्थानाङ्ग (१०.७०) में निरूपित आलोचना के दश दोषों का सेवन करता है । इसीलिए कहा है कि आलोचना करने वाले को विकट-भाव (बालक की तरह सरल और स्पष्ट भाव वाला) होना चाहिए। जिसका हृदय पवित्र नहीं होता, वह आलोचना नहीं कर सकता। आलोचना नहीं करने वाले विराधक होते हैं, यह सोचकर आलोचना की जाती है।
१-हा० टी०प० २३३ : उपलक्षणं चतत्कुलबलरूपाणाम्, कुलसंपन्नोऽहं बलसंपन्नोऽहं रूपसंपन्नोऽहमित्येवं न माद्य तेति । २-(क) अ० चू० पृ० १९२ : अप्पाणवतिरित्तो बाहिरो।।
(ख) जि० चू० पृ० २८४ : बाहिरो नाम अत्ताणं मोत्तू ण जो सो लोगो सो बाहिरो भण्णइ ।
(ग) हा० टी० प० २३३ : 'बाह्यम्' आत्मनोऽन्यम् । ३ - (क) जि० चू० पृ० २८४ : सुएण उक्करिसं गच्छेज्जा, जहा बहुस्सुतोऽहं को मए समाणोत्ति, (पाटवेण) लाभेणऽवि को मए
अण्णो ?, लद्धीएवि जहा को मए समाणोत्ति एवमादिएअहियत्ति लज्जा (द्धी) संजमो भण्णइ, तेणवि संजमेण उक्करिसं गच्छेज्जा, को मए संजमेण सरिसोत्ति ?, जातीएवि जहा उत्तमजातीओऽहं तवेण को अण्णो बारसविधे तवे समाणो
मएत्ति?, बुद्धिएवि जहा को मए समाणोत्ति एवमादि, एतेहि सुयादीहि णो उक्करिसं गच्छेज्जा । (ख) हा० टी० ५० २३३ : श्रुतलाभाभ्यां न माद्यत पण्डितो लब्धिमानहमित्येवं, तथा जात्या--तापस्त्येन बुध्या वा, न माये
तेति वर्तते, जातिसंपन्नस्तपस्वी बुद्धिमानहमित्येवम् । ४-भग० २५.७.६८; ठा० १०.७१ । ५-ठा०८.१८ । ६-००० १९३ : सदा विगडभावो सब्वावत्थं जधा बालो जंपतो तहेव विगडभावो । ७-ठा० ८.१८ ।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org