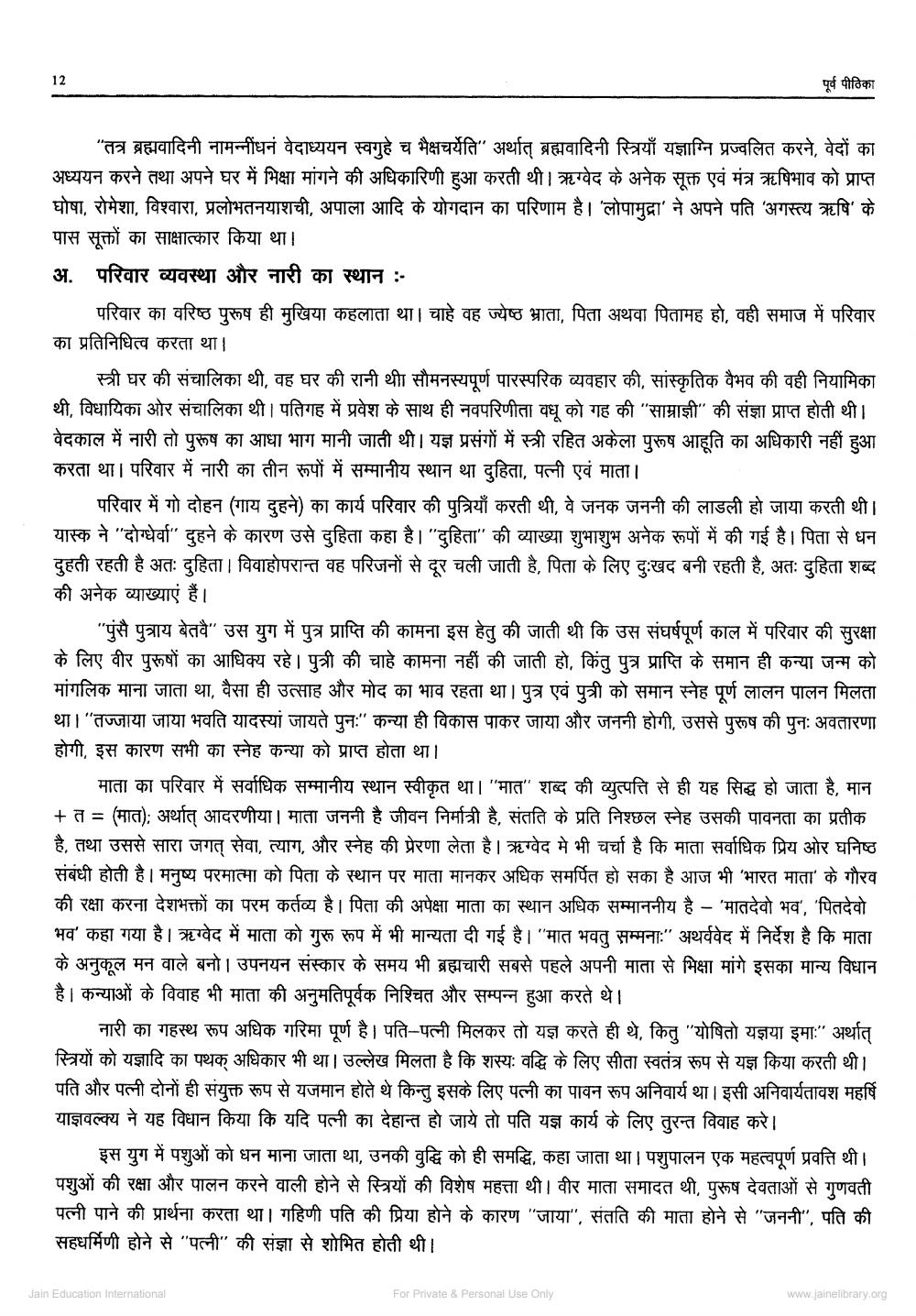________________
12
“तत्र ब्रह्मवादिनी नामन्नींधनं वेदाध्ययन स्वगुहे च भैक्षचर्येति" अर्थात् ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने, वेदों का अध्ययन करने तथा अपने घर में भिक्षा मांगने की अधिकारिणी हुआ करती थी । ऋग्वेद के अनेक सूक्त एवं मंत्र ऋषिभाव को प्राप्त घोषा, रोमेशा, विश्वारा, प्रलोभतनयाशची, अपाला आदि के योगदान का परिणाम है। 'लोपामुद्रा' ने अपने पति 'अगस्त्य ऋषि' के पास सूक्तों का साक्षात्कार किया था ।
अ. परिवार व्यवस्था और नारी का स्थान :
पूर्व पीठिका
परिवार का वरिष्ठ पुरूष ही मुखिया कहलाता था। चाहे वह ज्येष्ठ भ्राता, पिता अथवा पितामह हो, वही समाज में परिवार का प्रतिनिधित्व करता था ।
स्त्री घर की संचालिका थी, वह घर की रानी थी। सौमनस्यपूर्ण पारस्परिक व्यवहार की, सांस्कृतिक वैभव की वही नियामिका थी, विधायिका ओर संचालिका थी । पतिगह में प्रवेश के साथ ही नवपरिणीता वधू को गह की "साम्राज्ञी" की संज्ञा प्राप्त होती थी । वेदकाल में नारी तो पुरूष का आधा भाग मानी जाती थी । यज्ञ प्रसंगों में स्त्री रहित अकेला पुरूष आहूति का अधिकारी नहीं हुआ करता था । परिवार में नारी का तीन रूपों में सम्मानीय स्थान था दुहिता, पत्नी एवं माता ।
परिवार में गो दोहन (गाय दुहने) का कार्य परिवार की पुत्रियाँ करती थी, वे जनक जननी की लाडली हो जाया करती थी। यास्क ने "दोग्धेर्वा" दुहने के कारण उसे दुहिता कहा है। "दुहिता" की व्याख्या शुभाशुभ अनेक रूपों में की गई है। पिता से धन दुहती रहती है अतः दुहिता । विवाहोपरान्त वह परिजनों से दूर चली जाती है, पिता के लिए दुःखद बनी रहती है, अतः दुहिता शब्द T की अनेक व्याख्याएं हैं।
"पुंसै पुत्राय बेतवै” उस युग में पुत्र प्राप्ति की कामना इस हेतु की जाती थी कि उस संघर्षपूर्ण काल में परिवार की सुरक्षा के लिए वीर पुरूषों का आधिक्य रहे । पुत्री की चाहे कामना नहीं की जाती हो, किंतु पुत्र प्राप्ति के समान ही कन्या जन्म को मांगलिक माना जाता था, वैसा ही उत्साह और मोद का भाव रहता था । पुत्र एवं पुत्री को समान स्नेह पूर्ण लालन पालन मिलता था। "तज्जाया जाया भवति यादस्यां जायते पुनः" कन्या ही विकास पाकर जाया और जननी होगी, उससे पुरूष की पुनः अवतारणा होगी, इस कारण सभी का स्नेह कन्या को प्राप्त होता था ।
माता का परिवार में सर्वाधिक सम्मानीय स्थान स्वीकृत था । "मात" शब्द की व्युत्पत्ति से ही यह सिद्ध हो जाता है, मान + त = (मात); अर्थात् आदरणीया। माता जननी है जीवन निर्मात्री है, संतति के प्रति निश्छल स्नेह उसकी पावनता का प्रतीक है, तथा उससे सारा जगत् सेवा, त्याग, और स्नेह की प्रेरणा लेता है। ऋग्वेद मे भी चर्चा है कि माता सर्वाधिक प्रिय ओर घनिष्ठ संबंधी होती है। मनुष्य परमात्मा को पिता के स्थान पर माता मानकर अधिक समर्पित हो सका है आज भी 'भारत माता के गौरव की रक्षा करना देशभक्तों का परम कर्तव्य है। पिता की अपेक्षा माता का स्थान अधिक सम्माननीय है - 'मातदेवो भव', 'पितदेवो भव' कहा गया है। ऋग्वेद में माता को गुरू रूप में भी मान्यता दी गई है। "मात भवतु सम्मनाः" अथर्ववेद में निर्देश है कि माता के अनुकूल मन वाले बनो। उपनयन संस्कार के समय भी ब्रह्मचारी सबसे पहले अपनी माता से भिक्षा मांगे इसका मान्य विधान है। कन्याओं के विवाह भी माता की अनुमतिपूर्वक निश्चित और सम्पन्न हुआ करते थे ।
नारी का गहस्थ रूप अधिक गरिमा पूर्ण है। पति-पत्नी मिलकर तो यज्ञ करते ही थे, कितु "योषितो यज्ञया इमाः” अर्थात् स्त्रियों को यज्ञादि का पथक् अधिकार भी था। उल्लेख मिलता है कि शस्यः वद्धि के लिए सीता स्वतंत्र रूप से यज्ञ किया करती थी । पति और पत्नी दोनों ही संयुक्त रूप से यजमान होते थे किन्तु इसके लिए पत्नी का पावन रूप अनिवार्य था। इसी अनिवार्यतावश महर्षि याज्ञवल्क्य ने यह विधान किया कि यदि पत्नी का देहान्त हो जाये तो पति यज्ञ कार्य के लिए तुरन्त विवाह करे ।
इस युग में पशुओं को धन माना जाता था, उनकी वुद्धि को ही समद्धि, कहा जाता था। पशुपालन एक महत्वपूर्ण प्रवत्ति थी । पशुओं की रक्षा और पालन करने वाली होने से स्त्रियों की विशेष महत्ता थी । वीर माता समादत थी, पुरूष देवताओं से गुणवती पत्नी पाने की प्रार्थना करता था । गहिणी पति की प्रिया होने के कारण "जाया", संतति की माता होने से "जननी, पति की सहधर्मिणी होने से "पत्नी" की संज्ञा से शोभित होती थी ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org