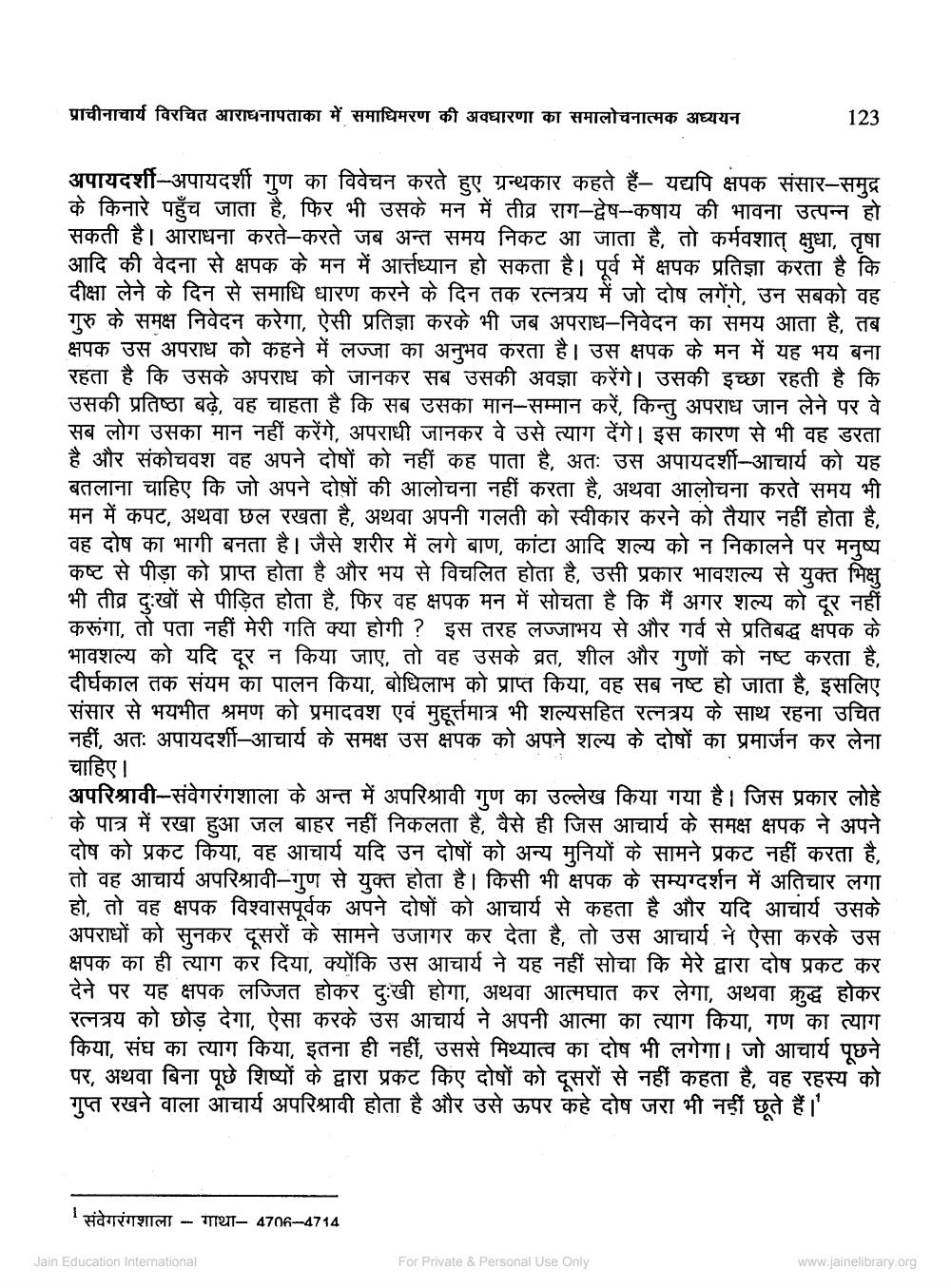________________
प्राचीनाचार्य विरचित आराधनापताका में समाधिमरण की अवधारणा का समालोचनात्मक अध्ययन
अपायदर्शी - अपायदर्शी गुण का विवेचन करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं- यद्यपि क्षपक संसार - समुद्र
किनारे पहुँच जाता है, फिर भी उसके मन में तीव्र राग-द्वेष - कषाय की भावना उत्पन्न हो सकती है। आराधना करते-करते जब अन्त समय निकट आ जाता है, तो कर्मवशात् क्षुधा, तृषा आदि की वेदना से क्षपक के मन में आर्त्तध्यान हो सकता है। पूर्व में क्षपक प्रतिज्ञा करता है कि दीक्षा लेने के दिन से समाधि धारण करने के दिन तक रत्नत्रय में जो दोष लगेंगे, उन सबको वह गुरु के समक्ष निवेदन करेगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जब अपराध - निवेदन का समय आता है, तब क्षपक उस अपराध को कहने में लज्जा का अनुभव करता है। उस क्षपक के मन में यह भय बना रहता है कि उसके अपराध को जानकर सब उसकी अवज्ञा करेंगे। उसकी इच्छा रहती है कि उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, वह चाहता है कि सब उसका मान-सम्मान करें, किन्तु अपराध जान लेने पर वे सब लोग उसका मान नहीं करेंगे, अपराधी जानकर वे उसे त्याग देंगे। इस कारण से भी वह डरता है और संकोचवश वह अपने दोषों को नहीं कह पाता है, अतः उस अपायदर्शी - आचार्य को यह बतलाना चाहिए कि जो अपने दोषों की आलोचना नहीं करता है, अथवा आलोचना करते समय भी मन में कपट, अथवा छल रखता है, अथवा अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, वह दोष का भागी बनता है। जैसे शरीर में लगे बाण, कांटा आदि शल्य को न निकालने पर मनुष्य कष्ट से पीड़ा को प्राप्त होता है और भय से विचलित होता है, उसी प्रकार भावशल्य से युक्त भिक्षु भी तीव्र दुःखों से पीड़ित होता है, फिर वह क्षपक मन में सोचता है कि मैं अगर शल्य को दूर नहीं करूंगा, तो पता नहीं मेरी गति क्या होगी ? इस तरह लज्जाभय से और गर्व से प्रतिबद्ध क्षपक के भावशल्य को यदि दूर न किया जाए, तो वह उसके व्रत, शील और गुणों को नष्ट करता है, दीर्घकाल तक संयम का पालन किया, बोधिलाभ को प्राप्त किया, वह सब नष्ट हो जाता है, इसलिए संसार से भयभीत श्रमण को प्रमादवश एवं मुहूर्त्तमात्र भी शल्यसहित रत्नत्रय के साथ रहना उचित नहीं, अतः अपायदर्शी - आचार्य के समक्ष उस क्षपक को अपने शल्य के दोषों का प्रमार्जन कर लेना चाहिए ।
अपरिश्रावी - संवेगरंगशाला के अन्त में अपरिश्रावी गुण का उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार लोहे के पात्र में रखा हुआ जल बाहर नहीं निकलता है, वैसे ही जिस आचार्य के समक्ष क्षपक ने अपने दोष को प्रकट किया, वह आचार्य यदि उन दोषों को अन्य मुनियों के सामने प्रकट नहीं करता है, तो वह आचार्य अपरिश्रावी गुण से युक्त होता है। किसी भी क्षपक के सम्यग्दर्शन में अतिचार लगा हो, तो वह क्षपक विश्वासपूर्वक अपने दोषों को आचार्य से कहता है और यदि आचार्य उसके अपराधों को सुनकर दूसरों के सामने उजागर कर देता है, तो उस आचार्य ने ऐसा करके उस क्षपक का ही त्याग कर दिया, क्योंकि उस आचार्य ने यह नहीं सोचा कि मेरे द्वारा दोष प्रकट कर देने पर यह क्षपक लज्जित होकर दुःखी होगा, अथवा आत्मघात कर लेगा, अथवा क्रुद्ध होकर रत्नत्रय को छोड़ देगा, ऐसा करके उस आचार्य ने अपनी आत्मा का त्याग किया, गण का त्याग किया, संघ का त्याग किया, इतना ही नहीं, उससे मिथ्यात्व का दोष भी लगेगा। जो आचार्य पूछने पर, अथवा बिना पूछे शिष्यों के द्वारा प्रकट किए दोषों को दूसरों से नहीं कहता है, वह रहस्य को गुप्त रखने वाला आचार्य अपरिश्रावी होता है और उसे ऊपर कहे दोष जरा भी नहीं छूते हैं।'
1
संवेगरंगशाला - गाथा- 4706 - 4714
123
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org