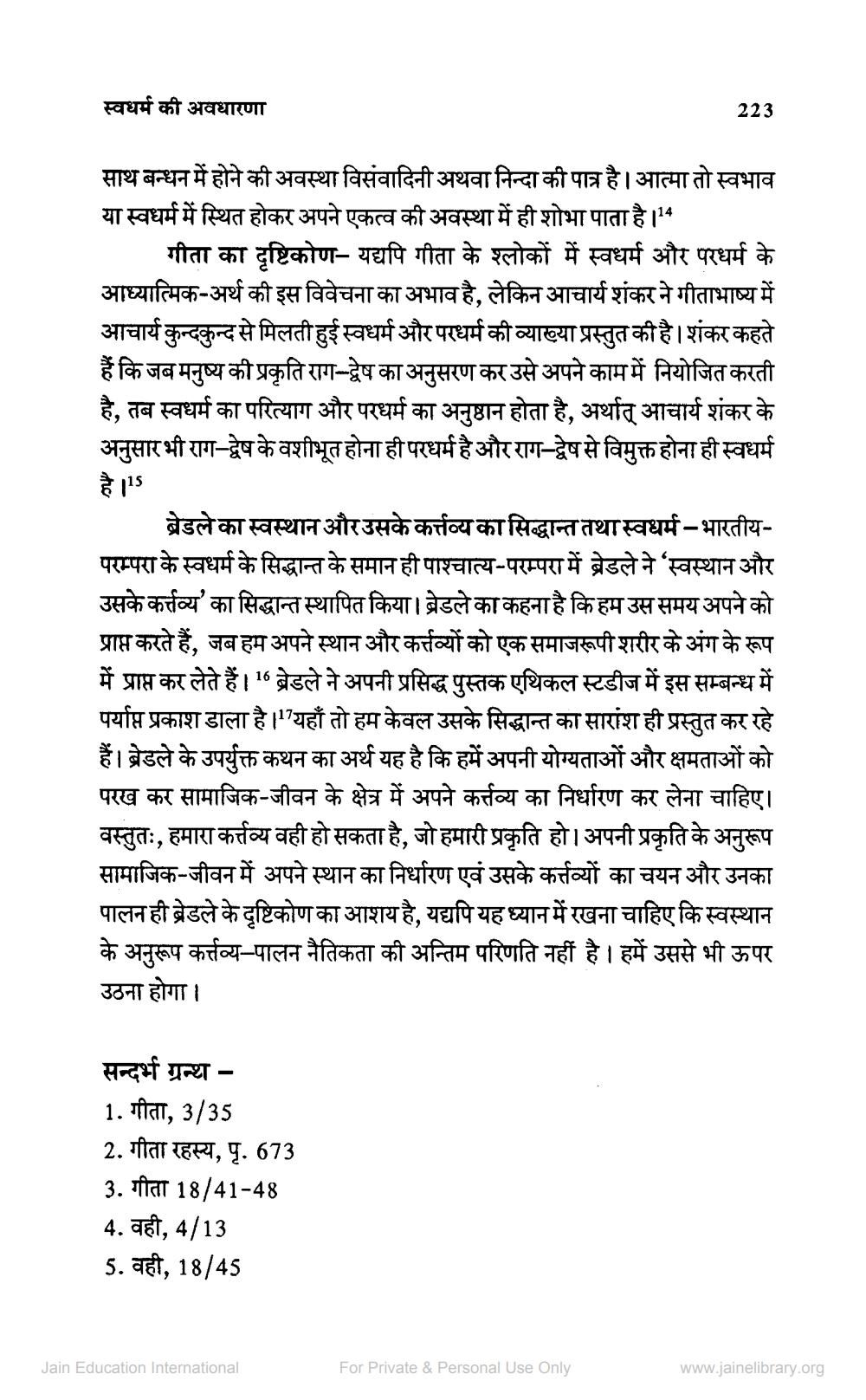________________
स्वधर्म की अवधारणा
223
साथ बन्धन में होने की अवस्था विसंवादिनी अथवा निन्दा की पात्र है। आत्मा तो स्वभाव या स्वधर्म में स्थित होकर अपने एकत्व की अवस्था में ही शोभा पाता है।
गीता का दृष्टिकोण- यद्यपि गीता के श्लोकों में स्वधर्म और परधर्म के आध्यात्मिक-अर्थ की इस विवेचना का अभाव है, लेकिन आचार्य शंकर ने गीताभाष्य में आचार्य कुन्दकुन्द से मिलती हुई स्वधर्म और परधर्म की व्याख्या प्रस्तुत की है। शंकर कहते हैं कि जब मनुष्य की प्रकृति राग-द्वेष का अनुसरण कर उसे अपने काम में नियोजित करती है, तब स्वधर्म का परित्याग और परधर्म का अनुष्ठान होता है, अर्थात् आचार्य शंकर के अनुसारभी राग-द्वेष के वशीभूत होना ही परधर्म है और राग-द्वेष से विमुक्त होना ही स्वधर्म है।15
ब्रेडले का स्वस्थान और उसके कर्तव्य का सिद्धान्त तथास्वधर्म-भारतीयपरम्परा के स्वधर्म के सिद्धान्त के समान ही पाश्चात्य-परम्परा में ब्रेडले ने स्वस्थान और उसके कर्त्तव्य' का सिद्धान्त स्थापित किया। ब्रेडले का कहना है कि हम उस समय अपने को प्राप्त करते हैं, जब हम अपने स्थान और कर्तव्यों को एक समाजरूपीशरीर के अंग के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। 16 ब्रेडले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एथिकल स्टडीज में इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डाला है। यहाँ तो हम केवल उसके सिद्धान्त का सारांश ही प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रेडले के उपर्युक्त कथन का अर्थ यह है कि हमें अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को परख कर सामाजिक-जीवन के क्षेत्र में अपने कर्त्तव्य का निर्धारण कर लेना चाहिए। वस्तुतः, हमारा कर्त्तव्य वही हो सकता है, जो हमारी प्रकृति हो। अपनी प्रकृति के अनुरूप सामाजिक-जीवन में अपने स्थान का निर्धारण एवं उसके कर्तव्यों का चयन और उनका पालनही ब्रेडले के दृष्टिकोण का आशय है, यद्यपि यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्वस्थान के अनुरूप कर्त्तव्य-पालन नैतिकता की अन्तिम परिणति नहीं है। हमें उससे भी ऊपर उठना होगा।
सन्दर्भ ग्रन्थ1. गीता, 3/35 2. गीता रहस्य, पृ. 673 3. गीता 18/41-48 4. वही, 4/13 5. वही, 18/45
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org