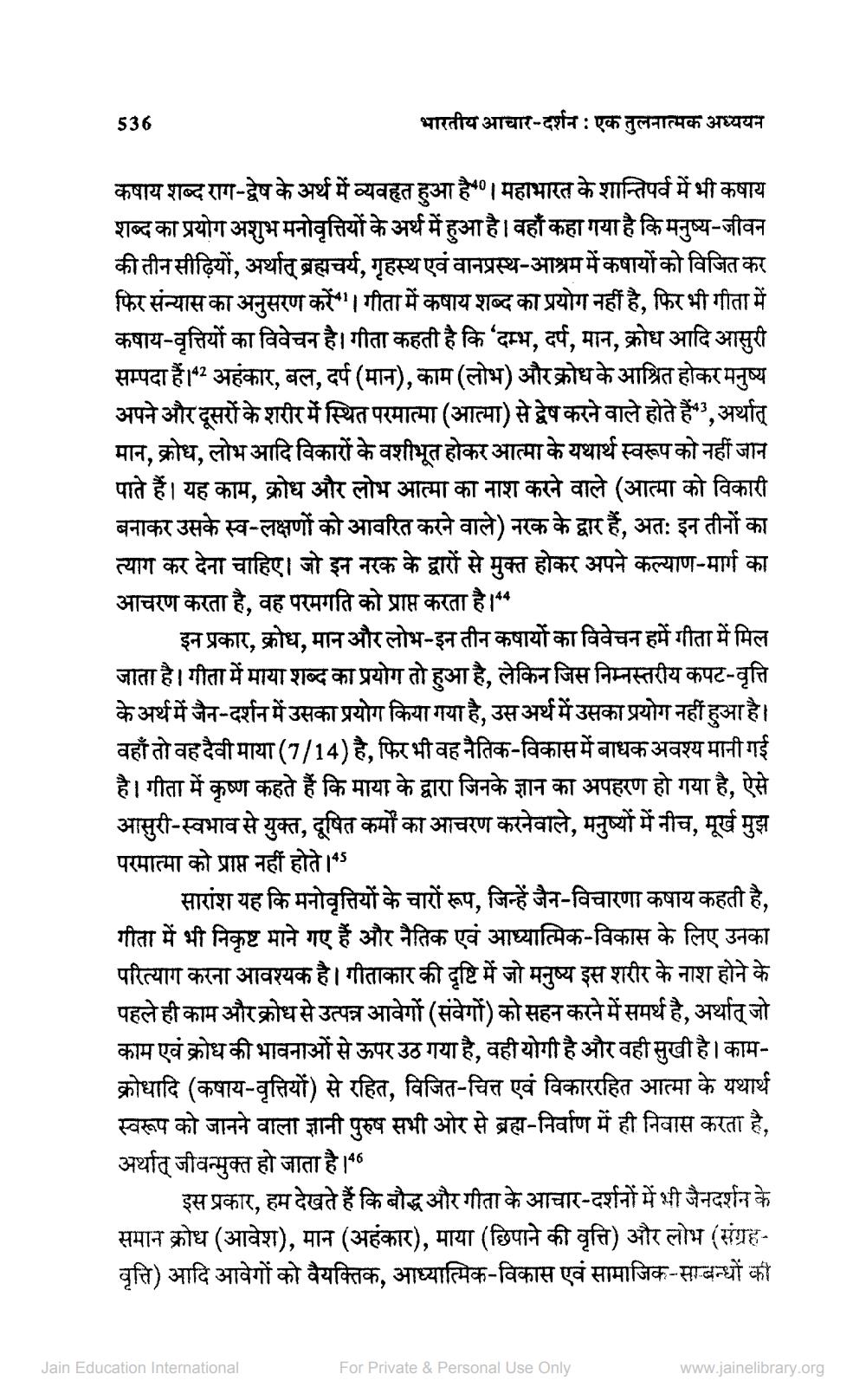________________
536
भारतीय आचार-दर्शन : एक तुलनात्मक अध्ययन
कषाय शब्द राग-द्वेष के अर्थ में व्यवहत हुआ है। महाभारत के शान्तिपर्व में भी कषाय शब्द का प्रयोग अशुभ मनोवृत्तियों के अर्थ में हुआ है। वहाँ कहा गया है कि मनुष्य-जीवन की तीन सीढ़ियों, अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ-आश्रम में कषायों को विजित कर फिर संन्यास का अनुसरण करें"। गीता में कषाय शब्द का प्रयोग नहीं है, फिर भी गीता में कषाय-वृत्तियों का विवेचन है। गीता कहती है कि 'दम्भ, दर्प, मान, क्रोध आदि आसुरी सम्पदा हैं। 2 अहंकार, बल, दर्प (मान), काम (लोभ) और क्रोध के आश्रित होकर मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में स्थित परमात्मा (आत्मा) से द्वेष करने वाले होते हैं, अर्थात् मान, क्रोध, लोभ आदि विकारों के वशीभूत होकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। यह काम, क्रोध और लोभ आत्मा का नाश करने वाले (आत्मा को विकारी बनाकर उसके स्व-लक्षणों को आवरित करने वाले) नरक के द्वार हैं, अत: इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जो इन नरक के द्वारों से मुक्त होकर अपने कल्याण-मार्ग का आचरण करता है, वह परमगति को प्राप्त करता है।
इन प्रकार, क्रोध, मान और लोभ-इन तीन कषायों का विवेचन हमें गीता में मिल जाता है। गीता में माया शब्द का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन जिस निम्नस्तरीय कपट-वृत्ति के अर्थ में जैन-दर्शन में उसका प्रयोग किया गया है, उसअर्थ में उसका प्रयोग नहीं हुआ है। वहाँ तो वह दैवी माया (7/14) है, फिर भी वह नैतिक-विकास में बाधक अवश्य मानी गई है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, ऐसे आसुरी-स्वभाव से युक्त, दूषित कर्मों का आचरण करनेवाले, मनुष्यों में नीच, मूर्ख मुझ परमात्मा को प्राप्त नहीं होते।
सारांश यह कि मनोवृत्तियों के चारों रूप, जिन्हें जैन-विचारणा कषाय कहती है, गीता में भी निकृष्ट माने गए हैं और नैतिक एवं आध्यात्मिक-विकास के लिए उनका परित्याग करना आवश्यक है। गीताकार की दृष्टि में जो मनुष्य इस शरीर के नाश होने के पहले ही काम और क्रोधसे उत्पन्न आवेगों (संवेगों) को सहन करने में समर्थ है, अर्थात् जो काम एवं क्रोध की भावनाओं से ऊपर उठ गया है, वही योगी है और वही सुखी है। कामक्रोधादि (कषाय-वृत्तियों) से रहित, विजित-चित्त एवं विकाररहित आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी पुरुष सभी ओर से ब्रह्म-निर्वाण में ही निवास करता है, अर्थात् जीवन्मुक्त हो जाता है।
इस प्रकार, हम देखते हैं कि बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों में भी जैनदर्शन के समान क्रोध (आवेश), मान (अहंकार), माया (छिपाने की वृत्ति) और लोभ (संग्रहवृत्ति) आदि आवेगों को वैयक्तिक, आध्यात्मिक-विकास एवं सामाजिक-साबन्धों की
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org