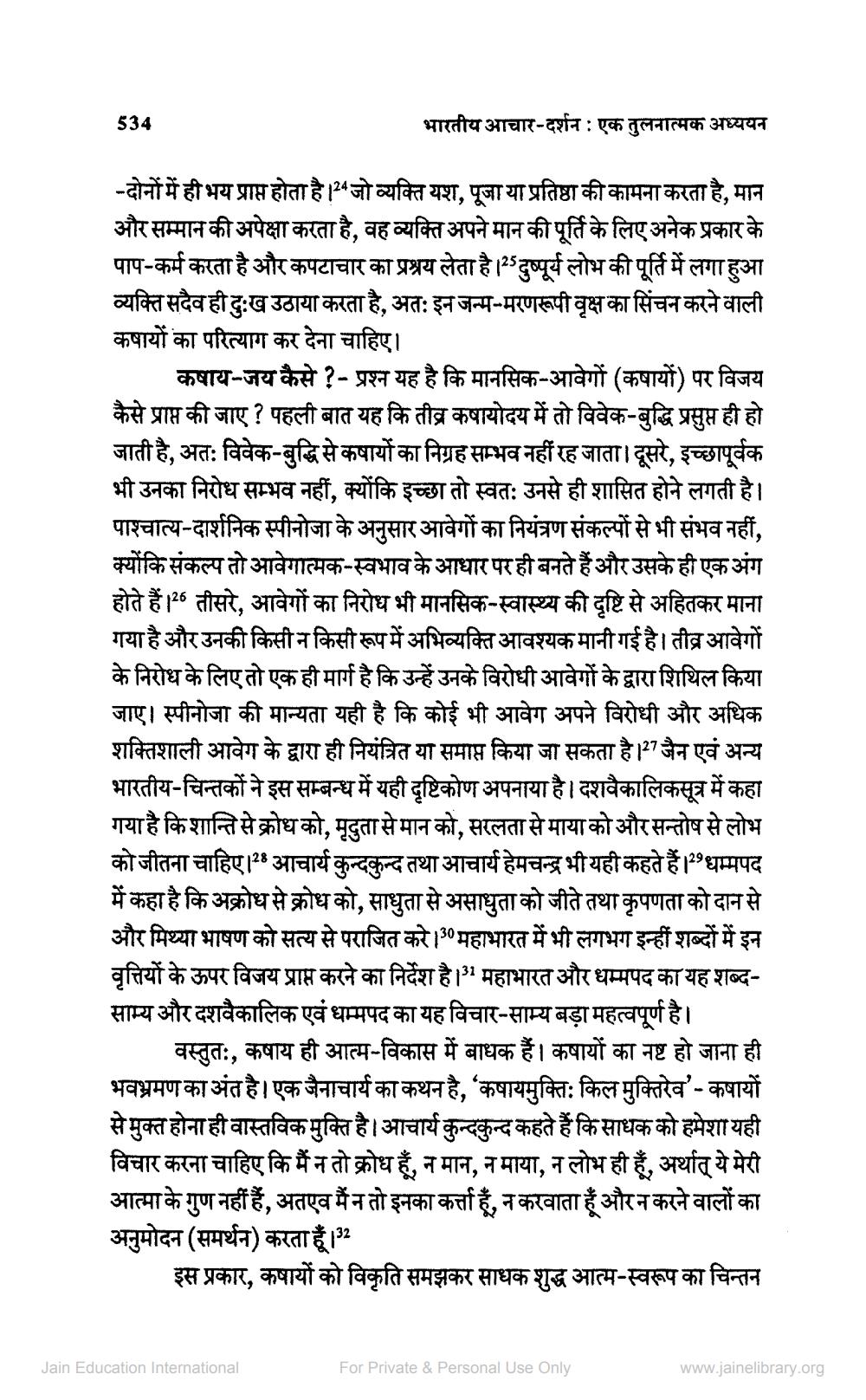________________
भारतीय आचार - दर्शन: एक तुलनात्मक अध्ययन
- दोनों में ही भय प्राप्त होता है। 24 जो व्यक्ति यश, पूजा या प्रतिष्ठा की कामना करता है, मान और सम्मान की अपेक्षा करता है, वह व्यक्ति अपने मान की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के पाप-कर्म करता है और कपटाचार का प्रश्रय लेता है। 25 दुष्पूर्य लोभ की पूर्ति में लगा हुआ व्यक्ति सदैव ही दुःख उठाया करता है, अतः इन जन्म-मरणरूपी वृक्ष का सिंचन करने वाली कषायों का परित्याग कर देना चाहिए।
534
कषाय-जय कैसे ? - प्रश्न यह है कि मानसिक आवेगों (कषायों) पर विजय कैसे प्राप्त की जाए ? पहली बात यह कि तीव्र कषायोदय में तो विवेक-बुद्धि प्रसुप्त ही हो जाती है, अत: विवेक-बुद्धि से कषायों का निग्रह सम्भव नहीं रह जाता। दूसरे, इच्छापूर्वक भी उनका निरोध सम्भव नहीं, क्योंकि इच्छा तो स्वतः उनसे ही शासित होने लगती है। पाश्चात्य-दार्शनिक स्पीनोजा के अनुसार आवेगों का नियंत्रण संकल्पों से भी संभव नहीं, क्योंकि संकल्प तो आवेगात्मक-स्वभाव के आधार पर ही बनते हैं और उसके ही एक अंग होते हैं। 26 तीसरे, आवेगों का निरोध भी मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर माना गया है और उनकी किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति आवश्यक मानी गई है। तीव्र आवेगों
निरोध के लिए तो एक ही मार्ग है कि उन्हें उनके विरोधी आवेगों के द्वारा शिथिल किया जाए। स्पीनोजा की मान्यता यही है कि कोई भी आवेग अपने विरोधी और अधिक शक्तिशाली आवेग के द्वारा ही नियंत्रित या समाप्त किया जा सकता है। 27 जैन एवं अन्य भारतीय-चिन्तकों ने इस सम्बन्ध में यही दृष्टिकोण अपनाया है। दशवैकालिकसूत्र में कहा गया है कि शान्ति से क्रोध को, मृदुता से मान को, सरलता से माया को और सन्तोष से लोभ को जीतना चाहिए ।" आचार्य कुन्दकुन्द तथा आचार्य हेमचन्द्र भी यही कहते हैं । " धम्मपद कहा है कि अक्रोध से क्रोध को, साधुता से असाधुता को जीते तथा कृपणता को दान से और मिथ्या भाषण को सत्य से पराजित करे। 30 महाभारत में भी लगभग इन्हीं शब्दों में इन वृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का निर्देश है। " महाभारत और धम्मपद का यह शब्द - साम्य और दशवैकालिक एवं धम्मपद का यह विचार - साम्य बड़ा महत्वपूर्ण है।
>
वस्तुतः कषाय ही आत्म-विकास में बाधक हैं। कषायों का नष्ट हो जाना ही भवभ्रमण का अंत है। एक जैनाचार्य का कथन है, 'कषायमुक्तिः किल मुक्तिरेव' - कषायों से मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि साधक को हमेशा यही विचार करना चाहिए कि मैं न तो क्रोध हूँ, न मान, न माया, न लोभ ही हूँ, अर्थात् ये मेरी आत्मा के गुण नहीं हैं, अतएव मैं न तो इनका कर्त्ता हूँ, न करवाता हूँ और न करने वालों का अनुमोदन (समर्थन करता हूँ | 32
इस प्रकार, कषायों को विकृति समझकर साधक शुद्ध आत्म-स्वरूप का चिन्तन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org