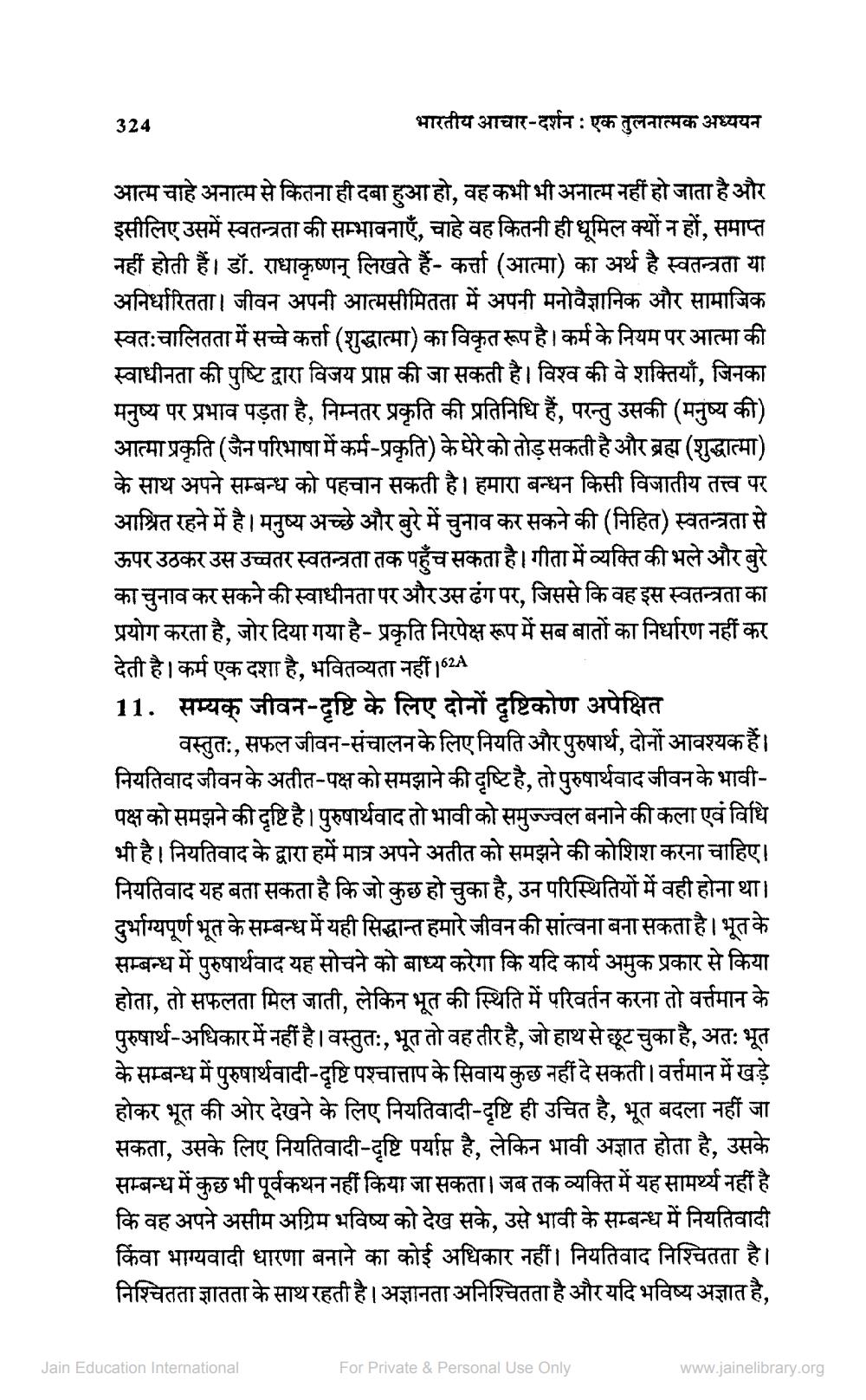________________
भारतीय आचार- दर्शन एक तुलनात्मक अध्ययन
आत्म चाहे अनात्म से कितना ही दबा हुआ हो, वह कभी भी अनात्म नहीं हो जाता है और इसीलिए उसमें स्वतन्त्रता की सम्भावनाएँ, चाहे वह कितनी ही धूमिल क्यों न हों, समाप्त नहीं होती हैं। डॉ. राधाकृष्णन् लिखते हैं- कर्त्ता (आत्मा) का अर्थ है स्वतन्त्रता या अनिर्धारितता । जीवन अपनी आत्मसीमितता में अपनी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्वत:चालितता में सच्चे कर्ता (शुद्धात्मा) का विकृत रूप है। कर्म के नियम पर आत्मा की स्वाधीनता की पुष्टि द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। विश्व की वे शक्तियाँ, जिनका मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, निम्नतर प्रकृति की प्रतिनिधि हैं, परन्तु उसकी (मनुष्य की) आत्मा प्रकृति (जैन परिभाषा में कर्म - प्रकृति) के घेरे को तोड़ सकती है और ब्रह्म (शुद्धात्मा) के साथ अपने सम्बन्ध को पहचान सकती है। हमारा बन्धन किसी विजातीय तत्त्व पर आश्रित रहने में है। मनुष्य अच्छे और बुरे में चुनाव कर सकने की (निहित ) स्वतन्त्रता से ऊपर उठकर उस उच्चतर स्वतन्त्रता तक पहुँच सकता है। गीता में व्यक्ति की भले और बुरे का चुनाव कर सकने की स्वाधीनता पर और उस ढंग पर, जिससे कि वह इस स्वतन्त्रता का प्रयोग करता है, जोर दिया गया है- प्रकृति निरपेक्ष रूप में सब बातों का निर्धारण नहीं कर देती है। कर्म एक दशा है, भवितव्यता नहीं 1024
324
11. सम्यक् जीवन-दृष्टि के लिए दोनों दृष्टिकोण अपेक्षित
वस्तुत:, सफल जीवन - संचालन के लिए नियति और पुरुषार्थ, दोनों आवश्यक हैं। नियतिवाद जीवन के अतीत पक्ष को समझाने की दृष्टि है, तो पुरुषार्थवाद जीवन के भावीपक्ष को समझने की दृष्टि है । पुरुषार्थवाद तो भावी को समुज्ज्वल बनाने की कला एवं विधि भी है । नियतिवाद के द्वारा हमें मात्र अपने अतीत को समझने की कोशिश करना चाहिए। नियतिवाद यह बता सकता है कि जो कुछ हो चुका है, उन परिस्थितियों में वही होना था। दुर्भाग्यपूर्ण भूत के सम्बन्ध में यही सिद्धान्त हमारे जीवन की सांत्वना बना सकता है । भूत के सम्बन्ध में पुरुषार्थवाद यह सोचने को बाध्य करेगा कि यदि कार्य अमुक प्रकार से किया होता, तो सफलता मिल जाती, लेकिन भूत की स्थिति में परिवर्तन करना तो वर्तमान के पुरुषार्थ - अधिकार में नहीं है। वस्तुतः, भूत तो वह तीर है, जो हाथ से छूट चुका है, अत: भूत सम्बन्ध में पुरुषार्थवादी दृष्टि पश्चात्ताप के सिवाय कुछ नहीं दे सकती। वर्त्तमान में खड़े
भूत की ओर देखने के लिए नियतिवादी दृष्टि ही उचित है, भूत बदला नहीं जा सकता, उसके लिए नियतिवादी दृष्टि पर्याप्त है, लेकिन भावी अज्ञात होता है, उसके सम्बन्ध में कुछ भी पूर्वकथन नहीं किया जा सकता। जब तक व्यक्ति में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने असीम अग्रिम भविष्य को देख सके, उसे भावी के सम्बन्ध में नियतिवादी किंवा भाग्यवादी धारणा बनाने का कोई अधिकार नहीं । नियतिवाद निश्चितता है। निश्चितता ज्ञाता के साथ रहती है। अज्ञानता अनिश्चितता है और यदि भविष्य अज्ञात है,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org