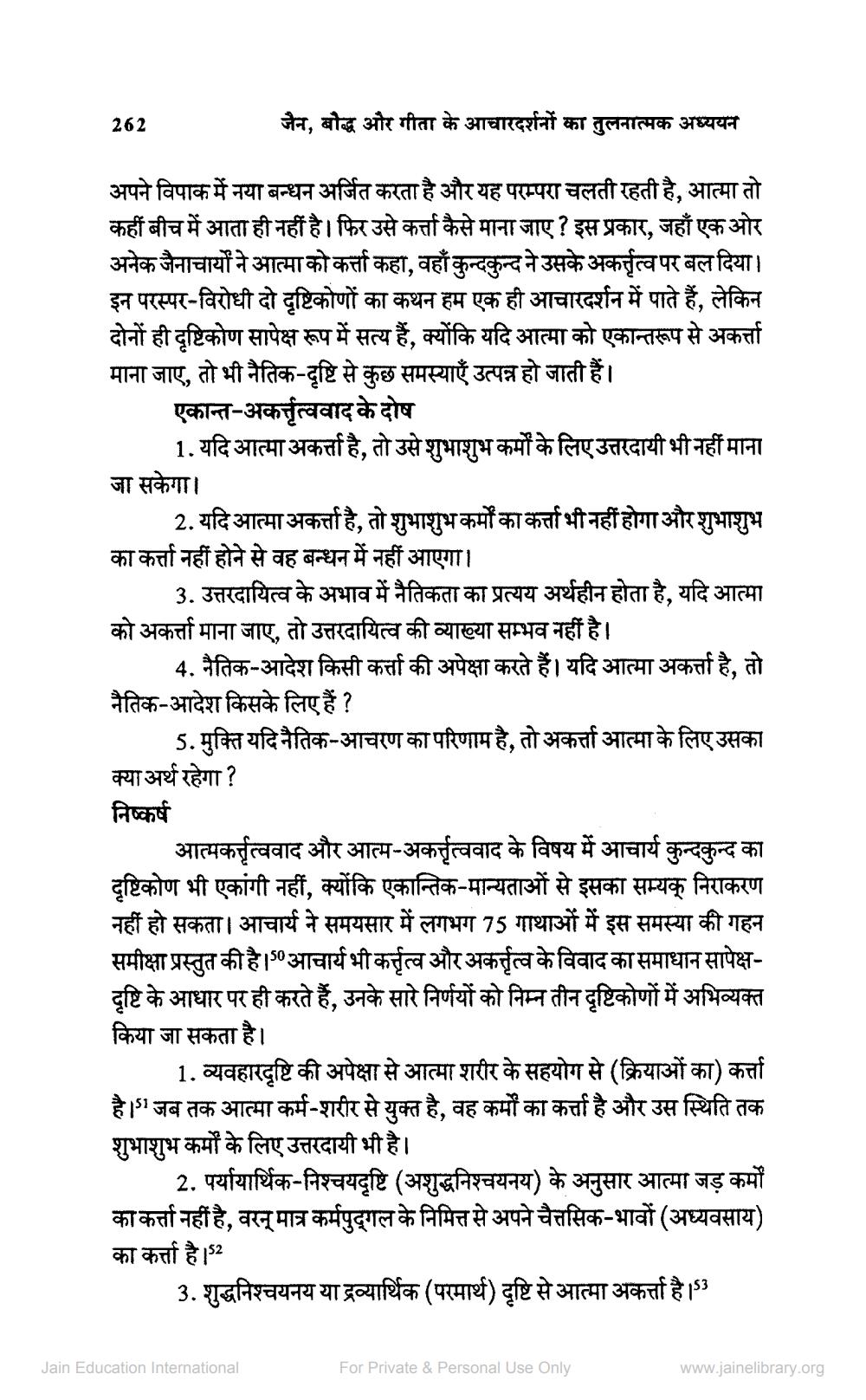________________
262
जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
अपने विपाक में नया बन्धन अर्जित करता है और यह परम्परा चलती रहती है, आत्मा तो कहीं बीच में आता ही नहीं है। फिर उसे कर्ता कैसे माना जाए? इस प्रकार, जहाँ एक ओर अनेक जैनाचार्यों ने आत्माको कर्ता कहा, वहाँ कुन्दकुन्द ने उसके अकर्तृत्व पर बल दिया। इन परस्पर-विरोधी दो दृष्टिकोणों का कथन हम एक ही आचारदर्शन में पाते हैं, लेकिन दोनों ही दृष्टिकोण सापेक्ष रूप में सत्य हैं, क्योंकि यदि आत्मा को एकान्तरूप से अकर्ता माना जाए, तो भी नैतिक-दृष्टि से कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।
एकान्त-अकर्तृत्ववाद के दोष
1. यदि आत्मा अकर्ता है, तो उसे शुभाशुभ कर्मों के लिए उत्तरदायी भी नहीं माना जा सकेगा।
2. यदिआत्माअकर्ता है, तो शुभाशुभ कर्मों का कर्ता भी नहीं होगा और शुभाशुभ का कर्ता नहीं होने से वह बन्धन में नहीं आएगा।
3. उत्तरदायित्व के अभाव में नैतिकता का प्रत्यय अर्थहीन होता है, यदि आत्मा को अकर्ता माना जाए, तो उत्तरदायित्व की व्याख्या सम्भव नहीं है।
4. नैतिक-आदेश किसी कर्ता की अपेक्षा करते हैं। यदि आत्मा अकर्ता है, तो नैतिक-आदेश किसके लिए हैं ?
5. मुक्ति यदिनैतिक-आचरण का परिणाम है, तो अकर्ता आत्मा के लिए उसका क्या अर्थ रहेगा? निष्कर्ष
_आत्मकर्तृत्ववाद और आत्म-अकर्तृत्ववाद के विषय में आचार्य कुन्दकुन्द का दृष्टिकोण भी एकांगी नहीं, क्योंकि एकान्तिक-मान्यताओं से इसका सम्यक् निराकरण नहीं हो सकता। आचार्य ने समयसार में लगभग 75 गाथाओं में इस समस्या की गहन समीक्षा प्रस्तुत की है। आचार्य भी कर्तृत्व और अकर्तृत्व के विवाद का समाधान सापेक्षदृष्टि के आधार पर ही करते हैं, उनके सारे निर्णयों को निम्न तीन दृष्टिकोणों में अभिव्यक्त किया जा सकता है।
1. व्यवहारदृष्टि की अपेक्षा से आत्मा शरीर के सहयोग से (क्रियाओं का) कर्ता है। जब तक आत्मा कर्म-शरीर से युक्त है, वह कर्मों का कर्ता है और उस स्थिति तक शुभाशुभ कर्मों के लिए उत्तरदायी भी है।
2. पर्यायार्थिक-निश्चयदृष्टि (अशुद्धनिश्चयनय) के अनुसार आत्मा जड़ कर्मों काकर्ता नहीं है, वरन् मात्र कर्मपुद्गल के निमित्त से अपने चैतसिक-भावों (अध्यवसाय) का कर्ता है।
3. शुद्धनिश्चयनय या द्रव्यार्थिक (परमार्थ) दृष्टि से आत्मा अकर्ता है।"
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org