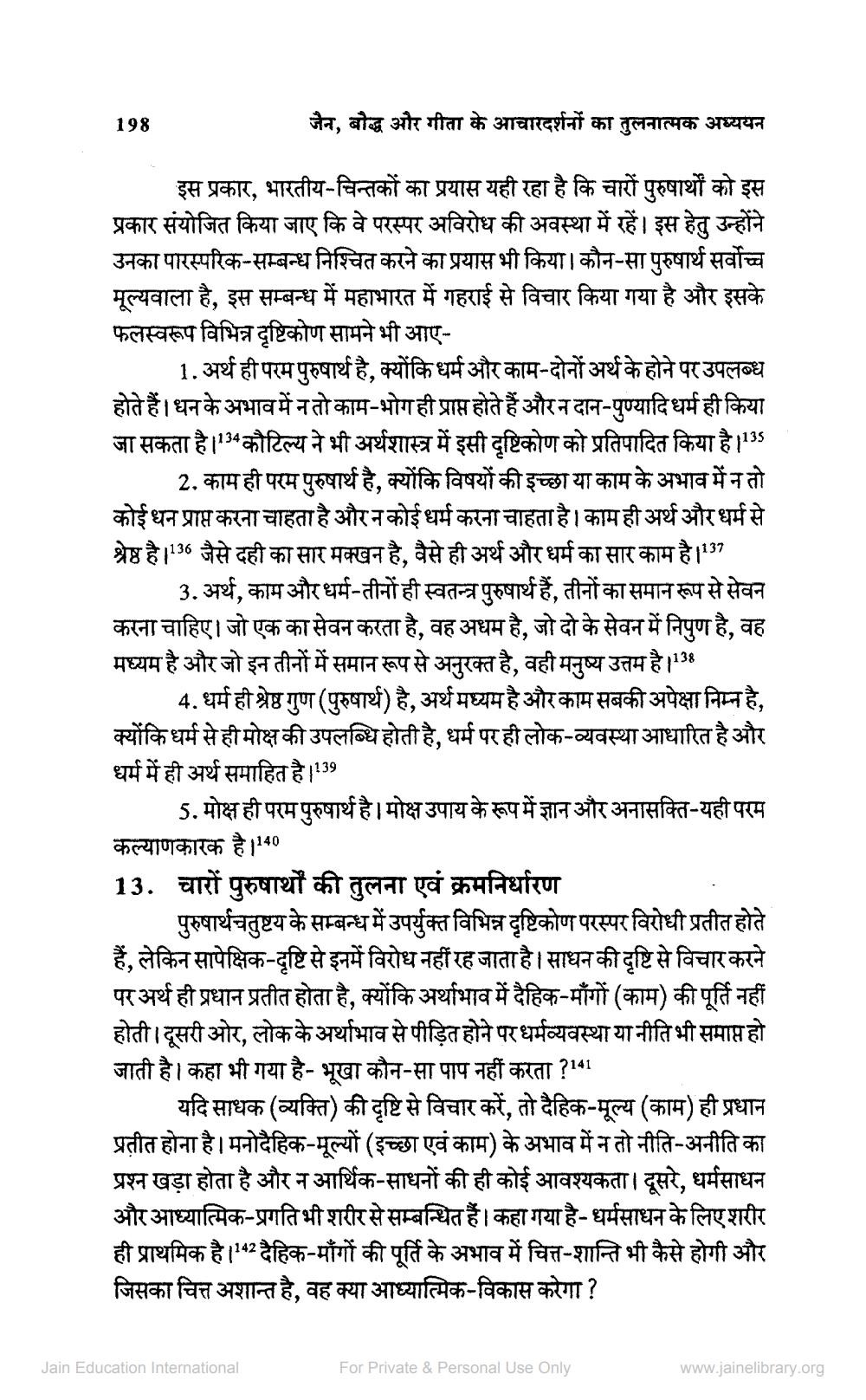________________
जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
इस प्रकार, भारतीय-चिन्तकों का प्रयास यही रहा है कि चारों पुरुषार्थों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि वे परस्पर अविरोध की अवस्था में रहें। इस हेतु उन्होंने उनका पारस्परिक-सम्बन्ध निश्चित करने का प्रयास भी किया। कौन-सा पुरुषार्थ सर्वोच्च मूल्यवाला है, इस सम्बन्ध में महाभारत में गहराई से विचार किया गया है और इसके फलस्वरूप विभिन्न दृष्टिकोण सामने भी आए
198
1. अर्थ ही परम पुरुषार्थ है, क्योंकि धर्म और काम-दोनों अर्थ के होने पर उपलब्ध होते हैं। धन के अभाव में न तो काम भोग ही प्राप्त होते हैं और न दान-पुण्यादि धर्म ही किया सकता है। 134 ने भी अर्थशास्त्र में इसी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। 135
2. काम ही परम पुरुषार्थ है, क्योंकि विषयों की इच्छा या काम के अभाव में न तो कोई धन प्राप्त करना चाहता है और न कोई धर्म करना चाहता है। काम ही अर्थ और धर्म से श्रेष्ठ है । 136 जैसे दही का सार मक्खन है, वैसे ही अर्थ और धर्म का सार काम है । 137
3. अर्थ, काम और धर्म - तीनों ही स्वतन्त्र पुरुषार्थ हैं, तीनों का समान रूप से सेवन करना चाहिए। जो एक का सेवन करता है, वह अधम है, जो दो के सेवन में निपुण है, वह मध्यम है और जो इन तीनों में समान रूप से अनुरक्त है, वही मनुष्य उत्तम है। 13
4. धर्म ही श्रेष्ठ गुण (पुरुषार्थ) है, अर्थ मध्यम है और काम सबकी अपेक्षा निम्न है, क्योंकि धर्म से ही मोक्ष की उपलब्धि होती है, धर्म पर ही लोक-व्यवस्था आधारित है और धर्म में ही अर्थ समाहित है । 139
5. मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। मोक्ष उपाय के रूप में ज्ञान और अनासक्ति यही परम कल्याणकारक है। 140
13. चारों पुरुषार्थों की तुलना एवं क्रमनिर्धारण
पुरुषार्थचतुष्टय के सम्बन्ध में उपर्युक्त विभिन्न दृष्टिकोण परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन सापेक्षिक दृष्टि से इनमें विरोध नहीं रह जाता है। साधन की दृष्टि से विचार करने पर अर्थ ही प्रधान प्रतीत होता है, क्योंकि अर्थाभाव में दैहिक - माँगों (काम) की पूर्ति नहीं होती। दूसरी ओर, लोक के अर्थाभाव से पीड़ित होने पर धर्मव्यवस्था या नीति भी समाप्त हो जाती है। कहा भी गया है- भूखा कौन-सा पाप नहीं करता ?141
यदि साधक (व्यक्ति) की दृष्टि से विचार करें, तो दैहिक - मूल्य (काम) ही प्रधान प्रतीत होना है। मनोदैहिक मूल्यों (इच्छा एवं काम) के अभाव में न तो नीति-अनीति का प्रश्न खड़ा होता है और न आर्थिक-साधनों की ही कोई आवश्यकता। दूसरे, धर्मसाधन और आध्यात्मिक प्रगति भी शरीर से सम्बन्धित हैं। कहा गया है- धर्मसाधन के लिए शरीर ही प्राथमिक है । 142 दैहिक - माँगों की पूर्ति के अभाव में चित्त - शान्ति भी कैसे होगी और जिसका चित्त अशान्त है, वह क्या आध्यात्मिक विकास करेगा ?
Jain Education International
-
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org