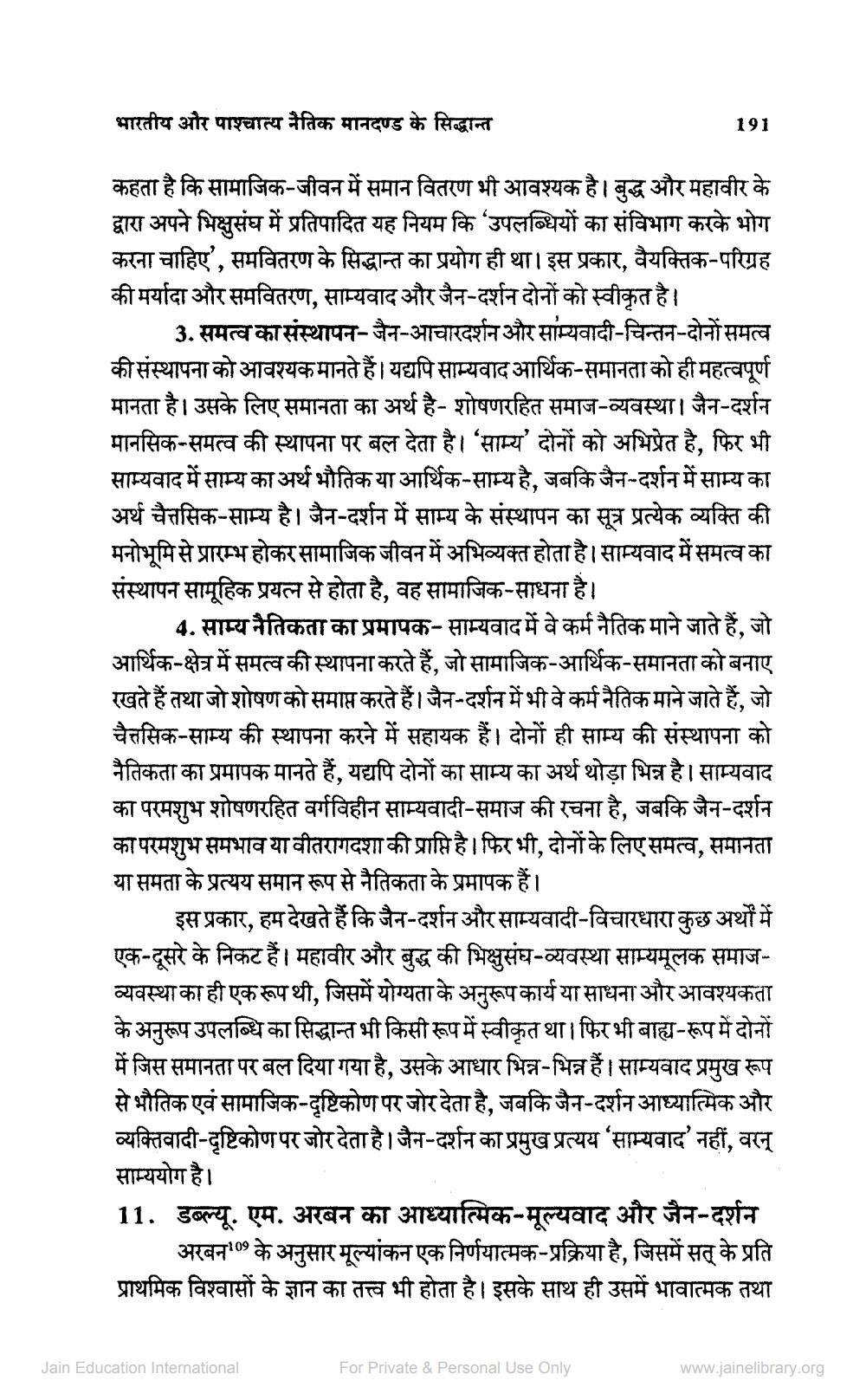________________
भारतीय और पाश्चात्य नैतिक मानदण्ड के सिद्धान्त
191
कहता है कि सामाजिक-जीवन में समान वितरण भी आवश्यक है। बुद्ध और महावीर के द्वारा अपने भिक्षुसंघ में प्रतिपादित यह नियम कि 'उपलब्धियों का संविभाग करके भोग करना चाहिए', समवितरण के सिद्धान्त का प्रयोग ही था। इस प्रकार, वैयक्तिक-परिग्रह की मर्यादा और समवितरण, साम्यवाद और जैन-दर्शन दोनों को स्वीकृत है।
3. समत्व कासंस्थापन-जैन-आचारदर्शन और साम्यवादी-चिन्तन-दोनों समत्व की संस्थापना को आवश्यकमानते हैं। यद्यपि साम्यवाद आर्थिक-समानता को ही महत्वपूर्ण मानता है। उसके लिए समानता का अर्थ है- शोषणरहित समाज-व्यवस्था। जैन-दर्शन मानसिक-समत्व की स्थापना पर बल देता है। 'साम्य' दोनों को अभिप्रेत है. फिर भी साम्यवाद में साम्य काअर्थ भौतिक या आर्थिक-साम्य है, जबकि जैन-दर्शन में साम्य का अर्थ चैत्तसिक-साम्य है। जैन-दर्शन में साम्य के संस्थापन का सूत्र प्रत्येक व्यक्ति की मनोभूमि से प्रारम्भ होकर सामाजिक जीवन में अभिव्यक्त होता है। साम्यवाद में समत्वका संस्थापन सामूहिक प्रयत्न से होता है, वह सामाजिक-साधना है।
4. साम्य नैतिकता का प्रमापक- साम्यवाद में वे कर्म नैतिक माने जाते हैं, जो आर्थिक-क्षेत्र में समत्व की स्थापना करते हैं, जो सामाजिक-आर्थिक-समानता को बनाए रखते हैं तथा जोशोषणको समाप्त करते हैं। जैन-दर्शन में भी वे कर्म नैतिक माने जाते हैं, जो
चैत्तसिक-साम्य की स्थापना करने में सहायक हैं। दोनों ही साम्य की संस्थापना को नैतिकता का प्रमापक मानते हैं, यद्यपि दोनों का साम्य का अर्थ थोड़ा भिन्न है। साम्यवाद का परमशुभ शोषणरहित वर्गविहीन साम्यवादी-समाज की रचना है, जबकि जैन-दर्शन का परमशुभ समभाव यावीतरागदशा की प्राप्ति है। फिर भी, दोनों के लिए समत्व, समानता या समता के प्रत्यय समान रूप से नैतिकता के प्रमापक हैं।
इस प्रकार, हम देखते हैं कि जैन-दर्शन और साम्यवादी-विचारधारा कुछ अर्थों में एक-दूसरे के निकट हैं। महावीर और बुद्ध की भिक्षुसंघ-व्यवस्था साम्यमूलक समाजव्यवस्था का ही एक रूप थी, जिसमें योग्यता के अनुरूप कार्य या साधना और आवश्यकता के अनुरूप उपलब्धि का सिद्धान्त भी किसी रूप में स्वीकृत था। फिर भी बाह्य-रूप में दोनों में जिस समानता पर बल दिया गया है, उसके आधार भिन्न-भिन्न हैं। साम्यवाद प्रमुख रूप से भौतिक एवं सामाजिक-दृष्टिकोण पर जोर देता है, जबकि जैन-दर्शन आध्यात्मिक और व्यक्तिवादी-दृष्टिकोण पर जोर देता है। जैन-दर्शन का प्रमुख प्रत्यय साम्यवाद' नहीं, वरन् साम्ययोग है। 11. डब्ल्यू. एम. अरबन का आध्यात्मिक-मूल्यवाद और जैन-दर्शन
___ अरबन10 के अनुसार मूल्यांकन एक निर्णयात्मक-प्रक्रिया है, जिसमें सत् के प्रति प्राथमिक विश्वासों के ज्ञान का तत्त्व भी होता है। इसके साथ ही उसमें भावात्मक तथा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org