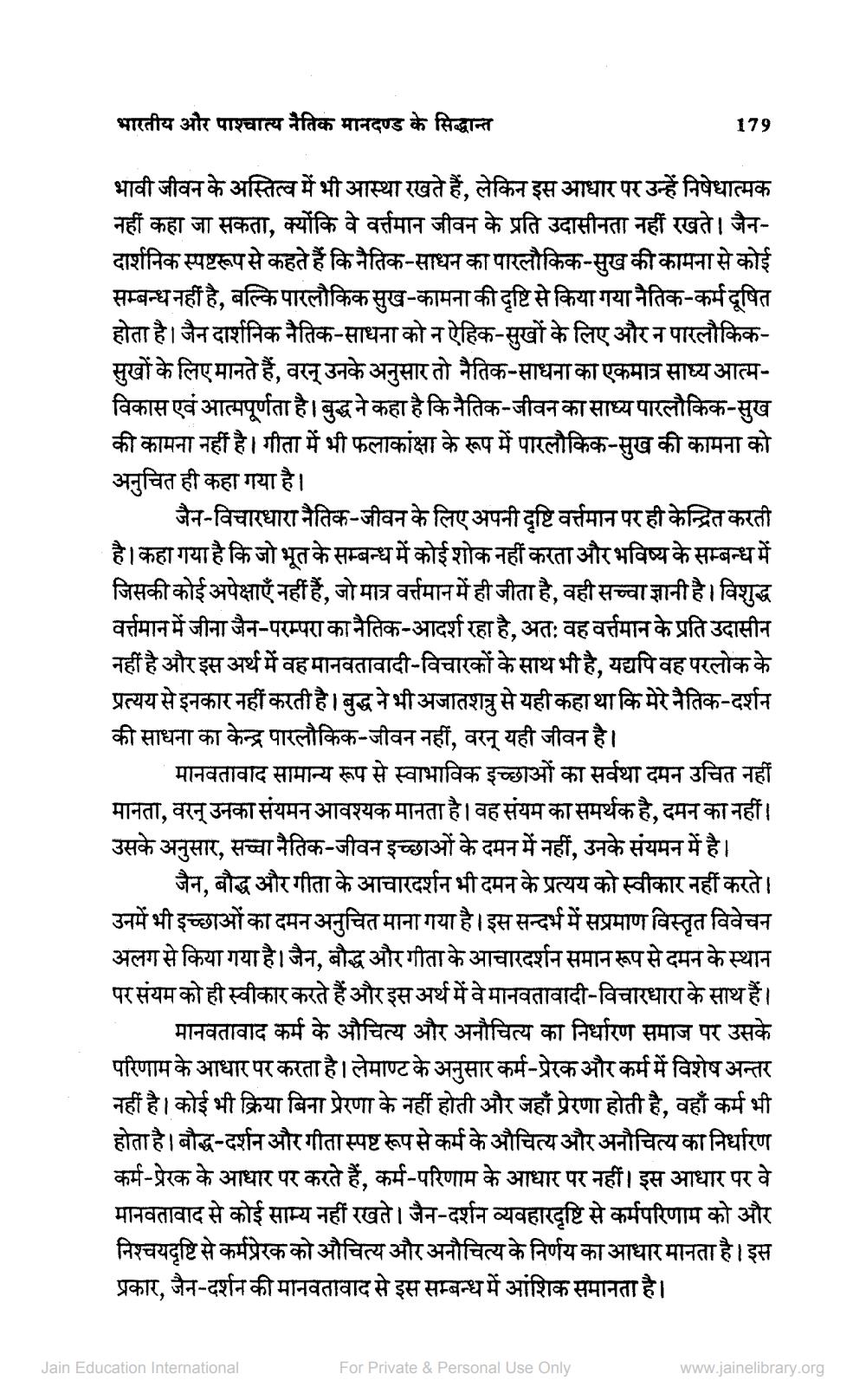________________
भारतीय और पाश्चात्य नैतिक मानदण्ड के सिद्धान्त
179
भावी जीवन के अस्तित्व में भी आस्था रखते हैं, लेकिन इस आधार पर उन्हें निषेधात्मक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे वर्तमान जीवन के प्रति उदासीनता नहीं रखते। जैनदार्शनिक स्पष्टरूप से कहते हैं कि नैतिक-साधन का पारलौकिक-सुख की कामना से कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि पारलौकिक सुख-कामना की दृष्टि से किया गया नैतिक-कर्म दूषित होता है। जैन दार्शनिक नैतिक-साधना को न ऐहिक-सुखों के लिए और न पारलौकिकसुखों के लिए मानते हैं, वरन् उनके अनुसार तो नैतिक-साधना का एकमात्र साध्य आत्मविकास एवं आत्मपूर्णता है। बुद्ध ने कहा है कि नैतिक-जीवन का साध्य पारलौकिक-सुख की कामना नहीं है। गीता में भी फलाकांक्षा के रूप में पारलौकिक-सुख की कामना को अनुचित ही कहा गया है।
जैन-विचारधारा नैतिक-जीवन के लिए अपनी दृष्टि वर्तमान पर ही केन्द्रित करती है। कहा गया है कि जो भूत के सम्बन्ध में कोई शोक नहीं करता और भविष्य के सम्बन्ध में जिसकी कोई अपेक्षाएँ नहीं हैं, जो मात्र वर्तमान में ही जीता है, वही सच्चा ज्ञानी है। विशुद्ध वर्तमान में जीना जैन-परम्पराकानैतिक-आदर्श रहा है, अत: वह वर्तमान के प्रति उदासीन नहीं है और इस अर्थ में वह मानवतावादी-विचारकों के साथ भी है, यद्यपि वह परलोक के प्रत्यय से इनकार नहीं करती है। बुद्ध ने भी अजातशत्रु से यही कहा था कि मेरे नैतिक-दर्शन की साधना का केन्द्र पारलौकिक-जीवन नहीं, वरन् यही जीवन है।
मानवतावाद सामान्य रूप से स्वाभाविक इच्छाओं का सर्वथा दमन उचित नहीं मानता, वरन् उनकासंयमन आवश्यक मानता है। वह संयम का समर्थक है, दमन का नहीं। उसके अनुसार, सच्चा नैतिक-जीवन इच्छाओं के दमन में नहीं, उनके संयमन में है।
जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शन भी दमन के प्रत्यय को स्वीकार नहीं करते। उनमें भी इच्छाओं का दमन अनुचित माना गया है। इस सन्दर्भ में सप्रमाण विस्तृत विवेचन अलग से किया गया है। जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शन समान रूप से दमन के स्थान पर संयम को ही स्वीकार करते हैं और इस अर्थ में वेमानवतावादी-विचारधारा के साथ हैं।
मानवतावाद कर्म के औचित्य और अनौचित्य का निर्धारण समाज पर उसके परिणाम के आधार पर करता है। लेमाण्ट के अनुसार कर्म-प्रेरक और कर्म में विशेष अन्तर नहीं है। कोई भी क्रिया बिना प्रेरणा के नहीं होती और जहाँ प्रेरणा होती है, वहाँ कर्म भी होता है। बौद्ध-दर्शन और गीतास्पष्ट रूपसे कर्म के औचित्य और अनौचित्य का निर्धारण कर्म-प्रेरक के आधार पर करते हैं, कर्म-परिणाम के आधार पर नहीं। इस आधार पर वे मानवतावाद से कोई साम्य नहीं रखते। जैन-दर्शन व्यवहारदृष्टि से कर्मपरिणाम को और निश्चयदृष्टि से कर्मप्रेरकको औचित्य और अनौचित्य के निर्णय का आधार मानता है। इस प्रकार, जैन-दर्शन की मानवतावाद से इस सम्बन्ध में आंशिक समानता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org