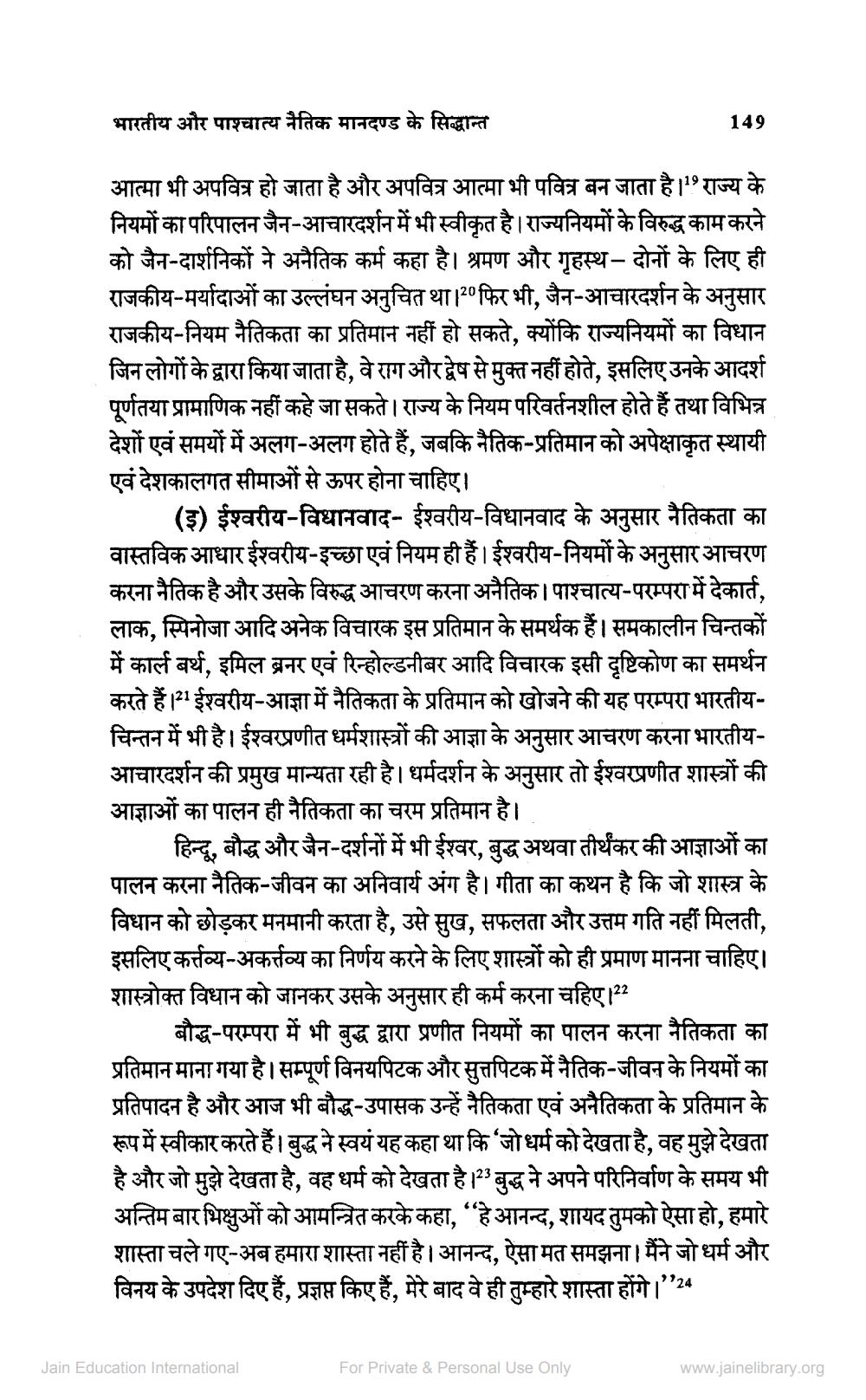________________
भारतीय और पाश्चात्य नैतिक मानदण्ड के सिद्धान्त
149
आत्मा भी अपवित्र हो जाता है और अपवित्र आत्मा भी पवित्र बन जाता है। राज्य के नियमों का परिपालन जैन-आचारदर्शन में भी स्वीकृत है। राज्यनियमों के विरुद्ध काम करने को जैन-दार्शनिकों ने अनैतिक कर्म कहा है। श्रमण और गृहस्थ- दोनों के लिए ही राजकीय-मर्यादाओं का उल्लंघन अनुचित था। फिर भी, जैन-आचारदर्शन के अनुसार राजकीय-नियम नैतिकता का प्रतिमान नहीं हो सकते, क्योंकि राज्यनियमों का विधान जिन लोगों के द्वारा किया जाता है, वे राग और द्वेष से मुक्त नहीं होते, इसलिए उनके आदर्श पूर्णतया प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते। राज्य के नियम परिवर्तनशील होते हैं तथा विभिन्न देशों एवं समयों में अलग-अलग होते हैं, जबकि नैतिक-प्रतिमान को अपेक्षाकृत स्थायी एवं देशकालगत सीमाओं से ऊपर होना चाहिए।
(इ) ईश्वरीय-विधानवाद- ईश्वरीय-विधानवाद के अनुसार नैतिकता का वास्तविक आधार ईश्वरीय-इच्छा एवं नियम ही हैं। ईश्वरीय-नियमों के अनुसार आचरण करना नैतिक है और उसके विरुद्ध आचरण करना अनैतिक। पाश्चात्य-परम्परा में देकार्त, लाक, स्पिनोजा आदि अनेक विचारक इस प्रतिमान के समर्थक हैं। समकालीन चिन्तकों में कार्ल बर्थ, इमिल ब्रनर एवं रिन्होल्डनीबर आदि विचारक इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। ईश्वरीय-आज्ञा में नैतिकता के प्रतिमान को खोजने की यह परम्परा भारतीयचिन्तन में भी है। ईश्वरप्रणीत धर्मशास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आचरण करना भारतीयआचारदर्शन की प्रमुख मान्यता रही है। धर्मदर्शन के अनुसार तो ईश्वरप्रणीत शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन ही नैतिकता का चरम प्रतिमान है।
हिन्दू, बौद्ध और जैन-दर्शनों में भी ईश्वर, बुद्ध अथवा तीर्थंकर की आज्ञाओं का पालन करना नैतिक-जीवन का अनिवार्य अंग है। गीता का कथन है कि जो शास्त्र के विधान को छोड़कर मनमानी करता है, उसे सुख, सफलता और उत्तम गति नहीं मिलती, इसलिए कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए। शास्त्रोक्त विधान को जानकर उसके अनुसार ही कर्म करना चहिए।22
बौद्ध-परम्परा में भी बुद्ध द्वारा प्रणीत नियमों का पालन करना नैतिकता का प्रतिमान माना गया है। सम्पूर्ण विनयपिटक और सुत्तपिटक में नैतिक-जीवन के नियमों का प्रतिपादन है और आज भी बौद्ध-उपासक उन्हें नैतिकता एवं अनैतिकता के प्रतिमान के रूप में स्वीकार करते हैं। बुद्ध ने स्वयं यह कहा था कि 'जोधर्म को देखता है, वह मुझे देखता है और जो मुझे देखता है, वह धर्म को देखता है। बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण के समय भी अन्तिम बार भिक्षुओं को आमन्त्रित करके कहा, “हे आनन्द, शायद तुमको ऐसा हो, हमारे शास्ता चले गए-अब हमारा शास्ता नहीं है। आनन्द, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय के उपदेश दिए हैं, प्रज्ञप्त किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे।"24
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org