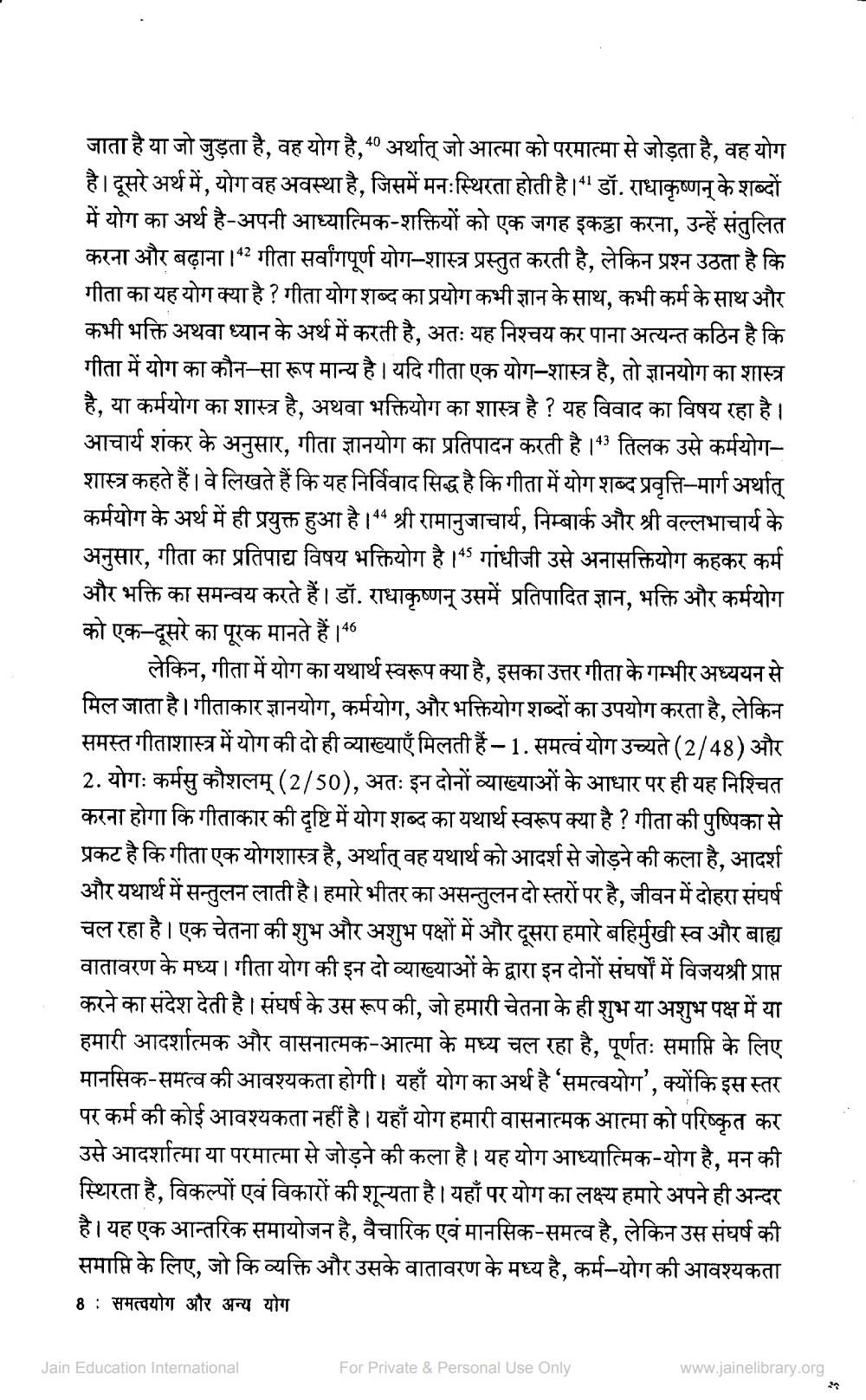________________
जाता है या जो जुड़ता है, वह योग है,40 अर्थात् जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, वह योग है। दूसरे अर्थ में, योग वह अवस्था है, जिसमें मनःस्थिरता होती है।" डॉ. राधाकृष्णन् के शब्दों में योग का अर्थ है-अपनी आध्यात्मिक-शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना। गीता सर्वांगपूर्ण योग-शास्त्र प्रस्तुत करती है, लेकिन प्रश्न उठता है कि गीता का यह योग क्या है ? गीता योगशब्द का प्रयोग कभी ज्ञान के साथ, कभी कर्म के साथ और कभी भक्ति अथवा ध्यान के अर्थ में करती है, अतः यह निश्चय कर पाना अत्यन्त कठिन है कि गीता में योग का कौन-सा रूप मान्य है। यदि गीता एक योग-शास्त्र है, तो ज्ञानयोग का शास्त्र है, या कर्मयोग का शास्त्र है, अथवा भक्तियोग का शास्त्र है ? यह विवाद का विषय रहा है। आचार्य शंकर के अनुसार, गीता ज्ञानयोग का प्रतिपादन करती है।43 तिलक उसे कर्मयोगशास्त्र कहते हैं। वे लिखते हैं कि यह निर्विवाद सिद्ध है कि गीता में योग शब्द प्रवृत्ति-मार्ग अर्थात् कर्मयोग के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। 44 श्री रामानुजाचार्य, निम्बार्क और श्री वल्लभाचार्य के अनुसार, गीता का प्रतिपाद्य विषय भक्तियोग है।45 गांधीजी उसे अनासक्तियोग कहकर कर्म
और भक्ति का समन्वय करते हैं। डॉ. राधाकृष्णन् उसमें प्रतिपादित ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग को एक-दूसरे का पूरक मानते हैं।
लेकिन, गीता में योग का यथार्थ स्वरूप क्या है, इसका उत्तर गीता के गम्भीर अध्ययन से मिल जाता है। गीताकार ज्ञानयोग, कर्मयोग, और भक्तियोग शब्दों का उपयोग करता है, लेकिन समस्त गीताशास्त्र में योग की दो ही व्याख्याएँ मिलती हैं- 1. समत्वं योग उच्यते (2/48) और 2. योगः कर्मसु कौशलम् (2/50), अतः इन दोनों व्याख्याओं के आधार पर ही यह निश्चित करना होगा कि गीताकार की दृष्टि में योग शब्द का यथार्थ स्वरूप क्या है ? गीता की पुष्पिका से प्रकट है किगीता एक योगशास्त्र है, अर्थात् वह यथार्थ को आदर्श से जोड़ने की कला है, आदर्श
और यथार्थ में सन्तुलन लाती है। हमारे भीतर का असन्तुलन दो स्तरों पर है, जीवन में दोहरा संघर्ष चल रहा है। एक चेतना की शुभ और अशुभ पक्षों में और दूसरा हमारे बहिर्मुखी स्व और बाह्य वातावरण के मध्य । गीता योग की इन दो व्याख्याओं के द्वारा इन दोनों संघर्षों में विजयश्री प्राप्त करने का संदेश देती है। संघर्ष के उस रूप की, जो हमारी चेतना के ही शुभ या अशुभ पक्ष में या हमारी आदर्शात्मक और वासनात्मक-आत्मा के मध्य चल रहा है, पूर्णतः समाप्ति के लिए मानसिक-समत्व की आवश्यकता होगी। यहाँ योग का अर्थ है 'समत्वयोग', क्योंकि इस स्तर पर कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ योग हमारी वासनात्मक आत्मा को परिष्कृत कर उसे आदर्शात्मा या परमात्मा से जोड़ने की कला है। यह योग आध्यात्मिक-योग है, मन की स्थिरता है, विकल्पों एवं विकारों की शून्यता है। यहाँ पर योग का लक्ष्य हमारे अपने ही अन्दर है। यह एक आन्तरिक समायोजन है, वैचारिक एवं मानसिक-समत्व है, लेकिन उस संघर्ष की समाप्ति के लिए, जो कि व्यक्ति और उसके वातावरण के मध्य है, कर्म-योग की आवश्यकता 8 : समत्वयोग और अन्य योग
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org