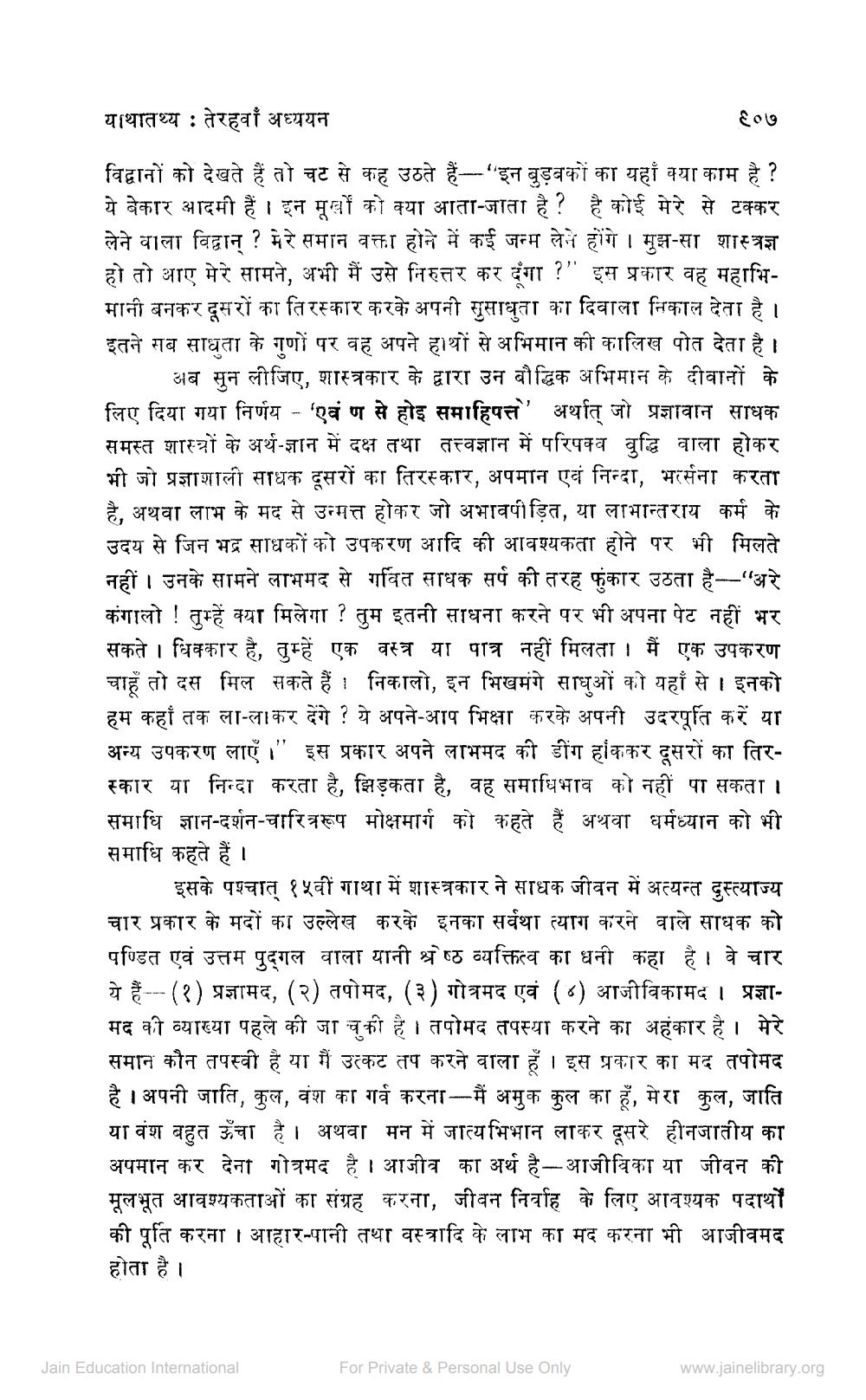________________
याथातथ्य : तेरहवां अध्ययन
विद्वानों को देखते हैं तो चट से कह उठते हैं- "इन बुड़बकों का यहाँ क्या काम है ? ये बेकार आदमी हैं । इन मूखों को क्या आता-जाता है ? है कोई मेरे से टक्कर लेने वाला विद्वान् ? मेरे समान वक्ता होने में कई जन्म लेने होंगे । मुझ-सा शास्त्रज्ञ हो तो आए मेरे सामने, अभी मैं उसे निरुत्तर कर दूंगा ?" इस प्रकार वह महाभिमानी बनकर दूसरों का तिरस्कार करके अपनी सुसाधुता का दिवाला निकाल देता है । इतने सब साधुता के गुणों पर वह अपने हाथों से अभिमान की कालिख पोत देता है।
अब सुन लीजिए, शास्त्रकार के द्वारा उन बौद्धिक अभिमान के दीवानों के लिए दिया गया निर्णय -- 'एवं ण से होइ समाहिपत्त' अर्थात् जो प्रज्ञावान साधक समस्त शास्त्रों के अर्थ-ज्ञान में दक्ष तथा तत्त्वज्ञान में परिपक्व बुद्धि वाला होकर भी जो प्रज्ञाशाली साधक दूसरों का तिरस्कार, अपमान एवं निन्दा, भर्सना करता है, अथवा लाभ के मद से उन्मत्त होकर जो अभावपीडित, या लाभान्तराय कर्म के उदय से जिन भद्र साधकों को उपकरण आदि की आवश्यकता होने पर भी मिलते नहीं। उनके सामने लाभमद से गर्वित साधक सर्प की तरह फुकार उठता है- "अरे कंगालो ! तुम्हें क्या मिलेगा ? तुम इतनी साधना करने पर भी अपना पेट नहीं भर सकते । धिक्कार है, तुम्हें एक वस्त्र या पात्र नहीं मिलता। मैं एक उपकरण चाहूँ तो दस मिल सकते हैं ! निकालो, इन भिखमंगे साधुओं को यहाँ से । इनको हम कहाँ तक ला-ला कर देंगे ? ये अपने-आप भिक्षा करके अपनी उदरपूर्ति करें या अन्य उपकरण लाएँ।" इस प्रकार अपने लाभमद की डींग हाँककर दूसरों का तिरस्कार या निन्दा करता है, झिड़कता है, वह समाधिभाव को नहीं पा सकता। समाधि ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप मोक्षमार्ग को कहते हैं अथवा धर्मध्यान को भी समाधि कहते हैं ।
___ इसके पश्चात् १५वीं गाथा में शास्त्रकार ने साधक जीवन में अत्यन्त दुस्त्याज्य चार प्रकार के मदों का उल्लेख करके इनका सर्वथा त्याग करने वाले साधक को पण्डित एवं उत्तम पुद्गल वाला यानी श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी कहा है। वे चार ये हैं --- (१) प्रज्ञामद, (२) तपोमद, (३) गोत्रमद एवं (४) आजीविकामद । प्रज्ञामद की व्याख्या पहले की जा चुकी है । तपोमद तपस्या करने का अहंकार है। मेरे समान कौन तपस्वी है या मैं उत्कट तप करने वाला हूँ । इस प्रकार का मद तपोमद है । अपनी जाति, कुल, वंश का गर्व करना-मैं अमुक कुल का हूँ, मेरा कुल, जाति या वंश बहुत ऊँचा है। अथवा मन में जात्य भिभान लाकर दूसरे हीनजातीय का अपमान कर देना गोत्रमद है । आजीव का अर्थ है-आजीविका या जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का संग्रह करना, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थों की पूर्ति करना । आहार-पानी तथा वस्त्रादि के लाभ का मद करना भी आजीवमद होता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org