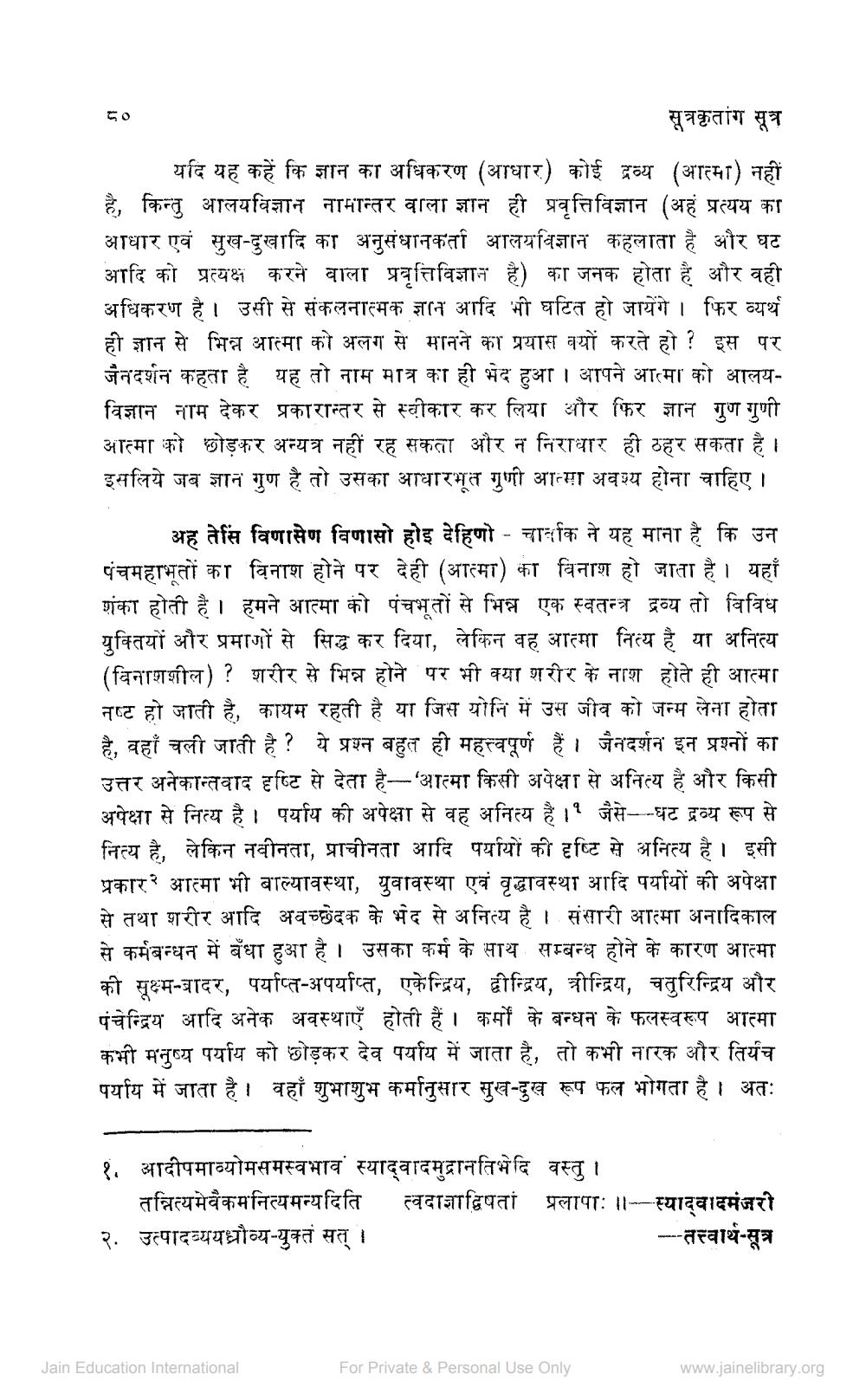________________
८०
सूत्रकृतांग सूत्र यदि यह कहें कि ज्ञान का अधिकरण (आधार) कोई द्रव्य (आत्मा) नहीं है, किन्तु आलयविज्ञान नामान्तर वाला ज्ञान ही प्रवृत्ति विज्ञान (अहं प्रत्यय का आधार एवं सुख-दुःखादि का अनुसंधानकर्ता आलयाविज्ञान कहलाता है और घट आदि को प्रत्यक्ष करने वाला प्रवृत्तिविज्ञान है) का जनक होता है और वही अधिकरण है। उसी से संकलनात्मक ज्ञान आदि भी घटित हो जायेंगे। फिर व्यर्थ ही ज्ञान से भिन्न आत्मा को अलग से मानने का प्रयास क्यों करते हो? इस पर जैनदर्शन कहता है यह तो नाम मात्र का ही भेद हुआ। आपने आत्मा को आलयविज्ञान नाम देकर प्रकारान्तर से स्वीकार कर लिया और फिर ज्ञान गुण गुणी आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता और न निराधार ही ठहर सकता है। इसलिये जब ज्ञान गुण है तो उसका आधारभूत गुणी आत्मा अवश्य होना चाहिए।
अह तेसि विणासेण विणासो होइ देहिणो - चार्वाक ने यह माना है कि उन पंचमहाभूतों का विनाश होने पर देही (आत्मा) का विनाश हो जाता है। यहाँ शंका होती है। हमने आत्मा को पंचभूतों से भिन्न एक स्वतन्त्र द्रव्य तो विविध युक्तियों और प्रमाणों से सिद्ध कर दिया, लेकिन वह आत्मा नित्य है या अनित्य (विनाशशील) ? शरीर से भिन्न होने पर भी क्या शरीर के नाश होते ही आत्मा नष्ट हो जाती है, कायम रहती है या जिस योनि में उस जीव को जन्म लेना होता है, वहाँ चली जाती है ? ये प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। जैनदर्शन इन प्रश्नों का उत्तर अनेकान्तवाद दृष्टि से देता है-'आत्मा किसी अपेक्षा से अनित्य है और किसी अपेक्षा से नित्य है। पर्याय की अपेक्षा से वह अनित्य है। जैसे--घट द्रव्य रूप से नित्य है, लेकिन नवीनता, प्राचीनता आदि पर्यायों की दृष्टि से अनित्य है। इसी प्रकार आत्मा भी बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था आदि पर्यायों की अपेक्षा से तथा शरीर आदि अवच्छेदक के भेद से अनित्य है । संसारी आत्मा अनादिकाल से कर्मबन्धन में बँधा हुआ है। उसका कर्म के साथ सम्बन्ध होने के कारण आत्मा की सूक्ष्म-बादर, पर्याप्त-अपर्याप्त, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय आदि अनेक अवस्थाएँ होती हैं। कर्मों के बन्धन के फलस्वरूप आत्मा कभी मनुष्य पर्याय को छोड़कर देव पर्याय में जाता है, तो कभी नारक और तिर्यच पर्याय में जाता है। वहाँ शुभाशुभ कर्मानुसार सुख-दुख रूप फल भोगता है। अतः
१. आदीपमाव्योमसमस्वभाव स्याद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु ।
तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वदाज्ञा द्विषतां प्रलापाः ॥-स्याद्वादमंजरी २. उत्पादब्ययध्रौव्य-युक्तं सत् ।
----तत्वार्थ-सूत्र
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org