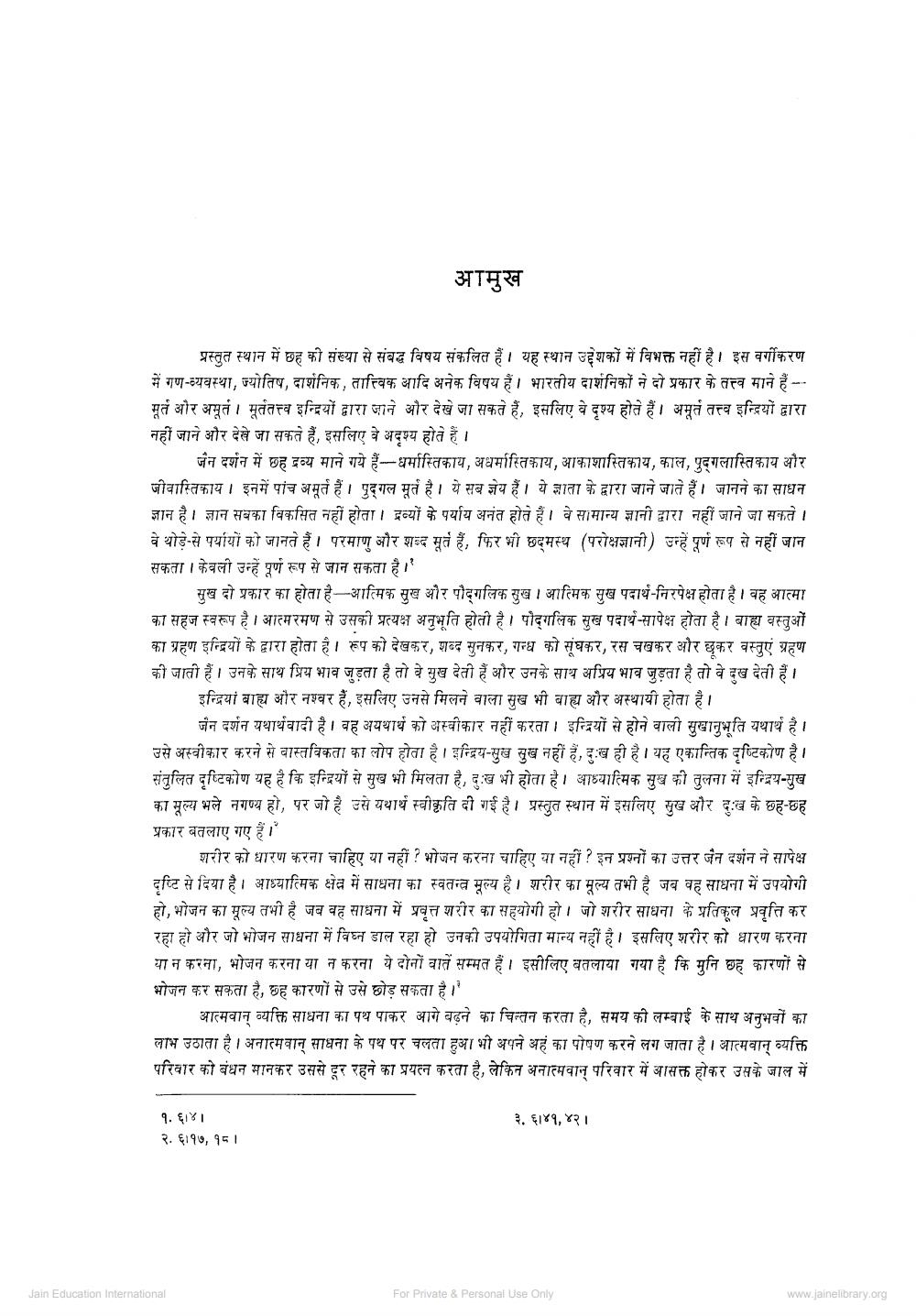________________
आमुख
प्रस्तुत स्थान में छह की संख्या से संबद्ध विषय संकलित हैं। यह स्थान उद्देशकों में विभक्त नहीं है। इस वर्गीकरण में गण-व्यवस्था, ज्योतिष, दार्शनिक, तात्त्विक आदि अनेक विषय हैं। भारतीय दार्शनिकों ने दो प्रकार के तत्त्व माने हैं ... मूर्त और अमूर्त । मूर्ततत्त्व इन्द्रियों द्वारा जाने और देखे जा सकते हैं, इसलिए वे दृश्य होते हैं। अमूर्त तत्त्व इन्द्रियों द्वारा नहीं जाने और देखे जा सकते हैं, इसलिए वे अदृश्य होते हैं।
जैन दर्शन में छह दव्य माने गये हैं-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय । इनमें पांच अमूर्त हैं। पुद्गल मूर्त है। ये सब ज्ञेय हैं। ये ज्ञाता के द्वारा जाने जाते हैं। जानने का साधन ज्ञान है। ज्ञान सबका विकसित नहीं होता। द्रव्यों के पर्याय अनंत होते हैं। वे सामान्य ज्ञानी द्वारा नहीं जाने जा सकते । वे थोड़े-से पर्यायों को जानते हैं। परमाणु और शब्द मूर्त हैं, फिर भी छद्मस्थ (परोक्षज्ञानी) उन्हें पूर्ण रूप से नहीं जान सकता । केवली उन्हें पूर्ण रूप से जान सकता है।
सुख दो प्रकार का होता है-आत्मिक सुख और पौद्गलिक सुख । आत्मिक सुख पदार्थ-निरपेक्ष होता है। वह आत्मा का सहज स्वरूप है । आत्मरमण से उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। पौद्गलिक सुख पदार्थ-सापेक्ष होता है। बाह्य वस्तुओं का ग्रहण इन्द्रियों के द्वारा होता है। रूप को देखकर, शब्द सुनकर, गन्ध को सूंघकर, रस चखकर और छूकर वस्तुएं ग्रहण की जाती हैं। उनके साथ प्रिय भाव जुड़ता है तो वे सुख देती हैं और उनके साथ अप्रिय भाव जुड़ता है तो वे दुख देती हैं।
इन्द्रियां बाह्य और नश्वर हैं, इसलिए उनसे मिलने वाला सुख भी बाह्य और अस्थायी होता है।
जैन दर्शन यथार्थवादी है। वह अयथार्थ को अस्वीकार नहीं करता। इन्द्रियों से होने वाली सुखानुभूति यथार्थ है । उसे अस्वीकार करने से वास्तविकता का लोप होता है । इन्द्रिय-सुख सुख नहीं हैं, दुःख ही है। यह एकान्तिक दृष्टिकोण है। संतुलित दृष्टिकोण यह है कि इन्द्रियों से सुख भी मिलता है, दुःख भी होता है। आध्यात्मिक सुख की तुलना में इन्द्रिय-सुख का मूल्य भले नगण्य हो, पर जो है उसे यथार्थ स्वीकृति दी गई है। प्रस्तुत स्थान में इसलिए सुख और दुःख के छह-छह प्रकार बतलाए गए हैं।
___ शरीर को धारण करना चाहिए या नहीं ? भोजन करना चाहिए या नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर जैन दर्शन ने सापेक्ष दृष्टि से दिया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना का स्वतन्त्र मूल्य है। शरीर का मूल्य तभी है जब वह साधना में उपयोगी हो, भोजन का मूल्य तभी है जब वह साधना में प्रवृत्त शरीर का सहयोगी हो। जो शरीर साधना के प्रतिकूल प्रवृत्ति कर रहा हो और जो भोजन साधना में विघ्न डाल रहा हो उनकी उपयोगिता मान्य नहीं है। इसलिए शरीर को धारण करना या न करना, भोजन करना या न करना ये दोनों वातें सम्मत हैं। इसीलिए बतलाया गया है कि मुनि छह कारणों से भोजन कर सकता है, छह कारणों से उसे छोड़ सकता है।
आत्मवान् व्यक्ति साधना का पथ पाकर आगे बढ़ने का चिन्तन करता है, समय की लम्बाई के साथ अनुभवों का लाभ उठाता है । अनात्मवान् साधना के पथ पर चलता हुआ भी अपने अहं का पोषण करने लग जाता है । आत्मवान् व्यक्ति परिवार को बंधन मानकर उससे दूर रहने का प्रयत्न करता है, लेकिन अनात्मवान् परिवार में आसक्त होकर उसके जाल में
३.६।४१,४२।
१.६।४। २. ६।१७, १८ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org