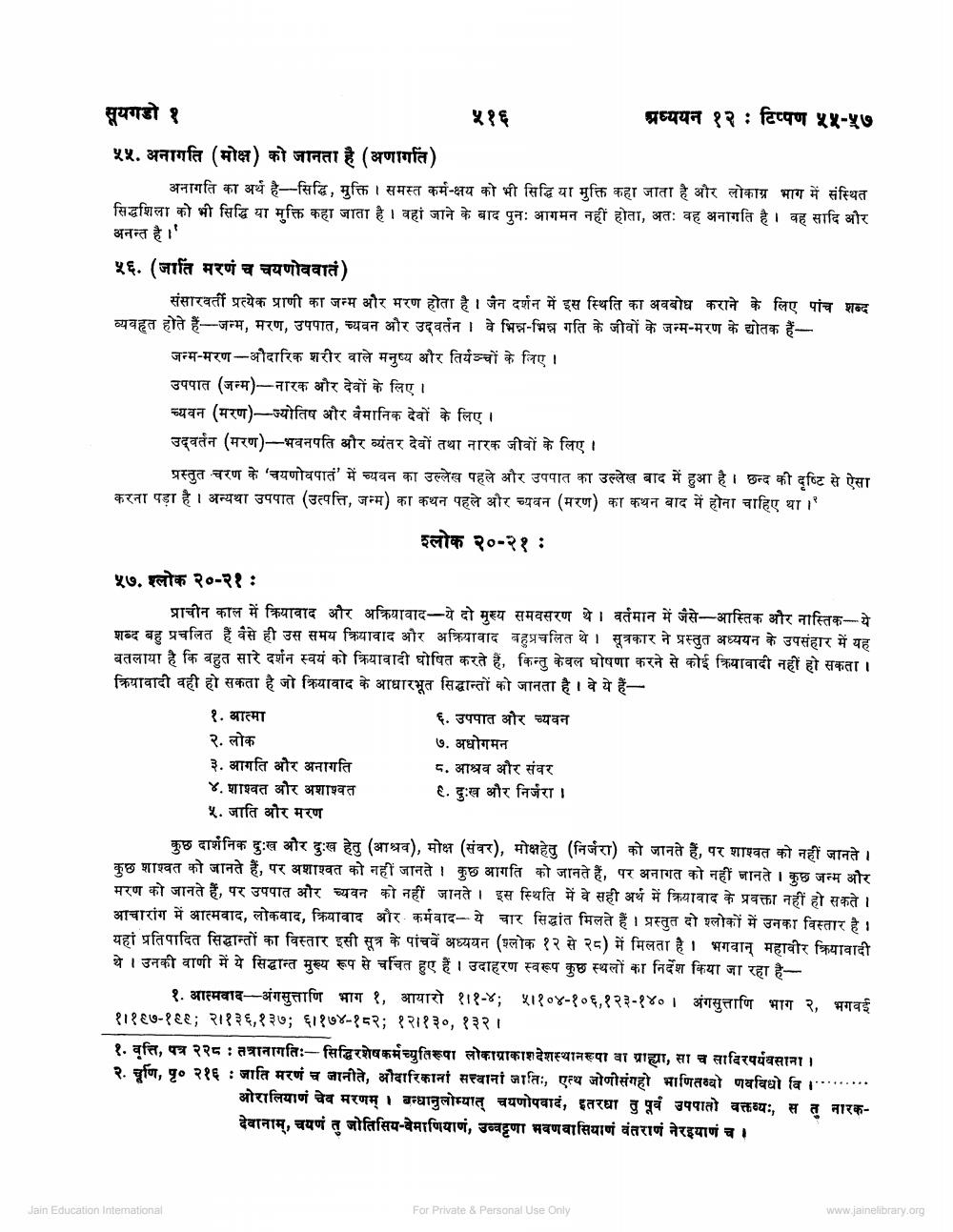________________
सूयगडो १
५५. अनागति (मोक्ष) को जानता है (अणागत)
अनागति का अर्थ है - सिद्धि, मुक्ति । समस्त कर्म-क्षय को भी सिद्धि या मुक्ति कहा जाता है और लोकाग्र भाग में संस्थित सिद्धशिला को भी सिद्धि या मुक्ति कहा जाता है। वहां जाने के बाद पुनः आगमन नहीं होता, अतः वह अनागति है। वह सादि और अनन्त है ।"
५१६
५६. ( जाति मरणं च चयणोववातं)
संसारवर्ती प्रत्येक प्राणी का जन्म और मरण होता है। जैन दर्शन में इस स्थिति का अवबोध कराने के लिए पांच शब्द व्यवहृत होते हैं- जन्म, मरण, उपपात, च्यवन और उद्वर्तन। वे भिन्न-भिन्न गति के जीवों के जन्म-मरण के द्योतक हैं
जन्म-मरण - औदारिक शरीर वाले मनुष्य और तिर्यञ्चों के लिए ।
उपपात (जन्म) - नारक और देवों के लिए ।
च्यवन ( मरण) ज्योतिष और वैमानिक देवों के लिए।
उर्तन (मरण) धवनपति और व्यंतर देवों तथा नारक जीवों के लिए।
प्रस्तुत चरण के 'चयणोवपातं' में च्यवन का उल्लेख पहले और उपपात का उल्लेख बाद में हुआ है । छन्द की दृष्टि से ऐसा करना पड़ा है । अन्यथा उपपात (उत्पत्ति, जन्म) का कथन पहले और च्यवन ( मरण) का कथन बाद में होना चाहिए था । श्लोक २०-२१ :
५७. श्लोक २०-२१ :
प्राचीन काल में क्रियावाद और अक्रियावाद - ये दो मुख्य समवसरण थे। वर्तमान में जैसे - आस्तिक और नास्तिक ये शब्द बहु प्रचलित हैं वैसे ही उस समय क्रियावाद और अक्रियावाद बहुप्रचलित थे। सूत्रकार ने प्रस्तुत अध्ययन के उपसंहार में यह बतलाया है कि बहुत सारे दर्शन स्वयं को क्रियावादी घोषित करते हैं, किन्तु केवल घोषणा करने से कोई क्रियावादी नहीं हो सकता । क्रियावादी वही हो सकता है जो क्रियावाद के आधारभूत सिद्धान्तों को जानता है । वे ये हैं
१. आत्मा २. लोक
३. आगति और अनागति
४. शाश्वत और अशाश्वत
५. जाति ओर मरण
Jain Education International
६. उपपात और च्यवन ७. अधोगमन
अध्ययन १२ टिप्पण ५५-५७
८. आश्रव और संवर
६. दुःख और निर्जरा ।
कुछ
दार्शनिक दुःख ओर दुःख हेतु (आव) मोदा (संबर), मोहेतु (निर्जरा) को जानते हैं, पर शाश्वत को नहीं जानते । कुछ शाश्वत को जानते हैं, पर अशाश्वत को नहीं जानते । कुछ आगति को जानते हैं, पर अनागत को नहीं जानते । कुछ जन्म और मरण को जानते हैं, पर उपपात और च्यवन को नहीं जानते । इस स्थिति में वे सही अर्थ में क्रियावाद के प्रवक्ता नहीं हो सकते । आचारांग में आत्मवाद, लोकवाद, क्रियावाद और कर्मवाद - ये चार सिद्धांत मिलते हैं । प्रस्तुत दो श्लोकों में उनका विस्तार है । यहां प्रतिपादित सिद्धान्तों का विस्तार इसी सूत्र के पांचवें अध्ययन (श्लोक १२ से २८) में मिलता है। भगवान् महावीर क्रियावादी थे । उनकी वाणी में ये सिद्धान्त मुख्य रूप से चर्चित हुए हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ स्थलों का निर्देश किया जा रहा है
५१०४-१०६, १२३-१४० । अंगसुत्ताणि भाग २, भगवई
१. आत्मवाद - अंगसुत्ताणि भाग १ आयारो १११-४; १११६७ १६६ २११३६, १३७, ६।१७४ -१८२; १२/१३०, १३२ ।
१. वृत्ति, पत्र २२८ : तत्रानागतिः- सिद्धिरशेषकर्मच्युतिरूपा लोकाग्राकाश देशस्थानरूपा वा ग्राह्या, सा च सादिरपर्यवसाना 1 २. चूर्ण, पृ० २१६ : जाति मरणं च जानीते, औदारिकानां सत्वानां जातिः, एत्थ जोणीसंगहो भाणितव्यो णवविधो वि । ओरालियागं चैव मरणम् अन्धानुलोम्यात् चयणोषवार्थ इतरथा तु पूर्व उपपालो बत्तव्यः स तु नारक देवानाम्, चयणं तु जोतिसिय-वैमाणियाणं, उचट्टणा भगवारियागं वंतराणं नराणं च ।
1
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org