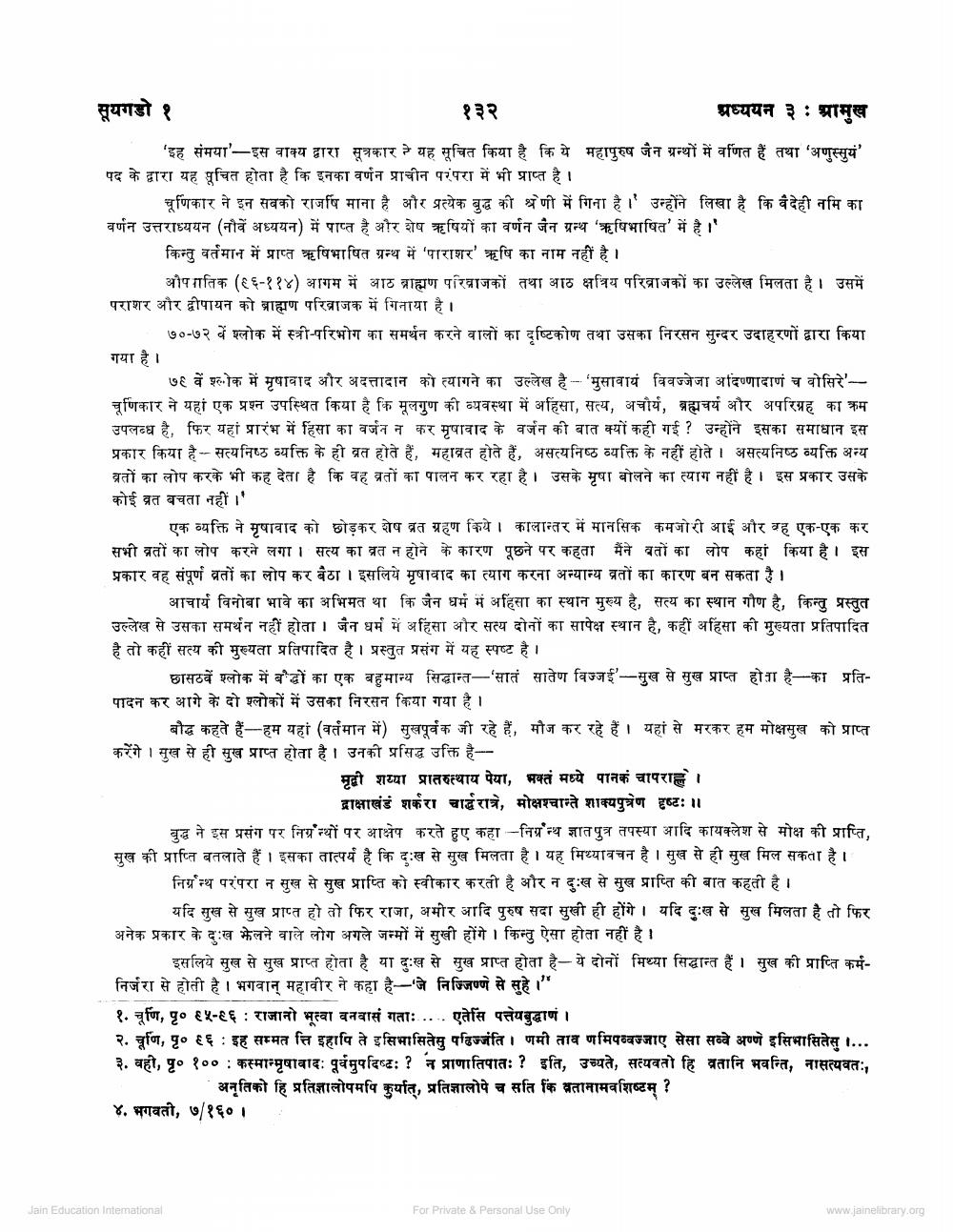________________
सूयगडो १
१३२
अध्ययन ३ : प्रामुख
_ 'इह संमया'-इस वाक्य द्वारा सूत्रकार ने यह सूचित किया है कि ये महापुरुष जैन ग्रन्थों में वर्णित हैं तथा 'अणुस्सुयं' पद के द्वारा यह पूचित होता है कि इनका वर्णन प्राचीन परंपरा में भी प्राप्त है।
चूर्णिकार ने इन सबको राजर्षि माना है और प्रत्येक बुद्ध की श्रेणी में गिना है।' उन्होंने लिखा है कि वैदेही नमि का वर्णन उत्तराध्ययन (नौवें अध्ययन) में प्राप्त है और शेष ऋषियों का वर्णन जैन ग्रन्थ 'ऋषिभाषित' में है।'
किन्तु वर्तमान में प्राप्त ऋषिभाषित ग्रन्थ में 'पाराशर' ऋषि का नाम नहीं है।
औपपातिक (९६-११४) आगम में आठ ब्राह्मण परिव्राजकों तथा आठ क्षत्रिय परिव्राजकों का उल्लेख मिलता है। उसमें पराशर और द्वीपायन को ब्राह्मण परिव्राजक में गिनाया है।
७०-७२ वें श्लोक में स्त्री-परिभोग का समर्थन करने वालों का दृष्टिकोण तथा उसका निरसन सुन्दर उदाहरणों द्वारा किया गया है।
७६ वें श्लोक में मृषावाद और अदत्तादान को त्यागने का उल्लेख है- 'मुसावायं विवज्जेजा अदिण्णादाणं च वोसिरे'चूणिकार ने यहां एक प्रश्न उपस्थित किया है कि मूलगुण की व्यवस्था में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का क्रम उपलब्ध है, फिर यहां प्रारंभ में हिंसा का वर्जन न कर मृषावाद के वर्जन की बात क्यों कही गई ? उन्होंने इसका समाधान इस प्रकार किया है- सत्यनिष्ठ व्यक्ति के ही व्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं, असत्यनिष्ठ व्यक्ति के नहीं होते। असत्यनिष्ठ व्यक्ति अन्य व्रतों का लोप करके भी कह देता है कि वह व्रतों का पालन कर रहा है। उसके मृषा बोलने का त्याग नहीं है। इस प्रकार उसके कोई व्रत बचता नहीं।'
एक व्यक्ति ने मृषावाद को छोड़कर शेष व्रत ग्रहण किये। कालान्तर में मानसिक कमजोरी आई और वह एक-एक कर सभी व्रतों का लोप करने लगा। सत्य का व्रत न होने के कारण पूछने पर कहता मैंने बतों का लोप कहां किया है। इस प्रकार वह संपूर्ण व्रतों का लोप कर बैठा । इसलिये मृषावाद का त्याग करना अन्यान्य व्रतों का कारण बन सकता है।
आचार्य विनोबा भावे का अभिमत था कि जैन धर्म में अहिंसा का स्थान मुख्य है, सत्य का स्थान गौण है, किन्तु प्रस्तुत उल्लेख से उसका समर्थन नहीं होता। जैन धर्म में अहिंसा और सत्य दोनों का सापेक्ष स्थान है, कहीं अहिंसा की मुख्यता प्रतिपादित है तो कहीं सत्य की मुख्यता प्रतिपादित है। प्रस्तुत प्रसंग में यह स्पष्ट है।
छासठवें श्लोक में बद्धों का एक बहुमान्य सिद्धान्त–'सातं सातेण विज्जई-सुख से सुख प्राप्त होता है-का प्रतिपादन कर आगे के दो श्लोकों में उसका निरसन किया गया है।
बौद्ध कहते हैं हम यहां (वर्तमान में) सुखपूर्वक जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। यहां से मरकर हम मोक्षसुख को प्राप्त करेंगे । सुख से ही सुख प्राप्त होता है। उनकी प्रसिद्ध उक्ति है--
मृद्वी शय्या प्रातरुत्थाय पेया, भक्तं मध्ये पानकं चापराले।
द्राक्षाखंडं शर्करा चार्द्धरात्रे, मोक्षश्चान्ते शाक्यपुत्रेण दृष्टः॥ बुद्ध ने इस प्रसंग पर निग्रन्थों पर आक्षेप करते हुए कहा -निग्रन्थ ज्ञात पुत्र तपस्या आदि कायक्लेश से मोक्ष की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति बतलाते हैं । इसका तात्पर्य है कि दुःख से सुख मिलता है । यह मिथ्यावचन है । सुख से ही सुख मिल सकता है।
निर्ग्रन्थ परंपरा न सुख से सुख प्राप्ति को स्वीकार करती है और न दुःख से सुख प्राप्ति की बात कहती है ।
यदि सुख से सुख प्राप्त हो तो फिर राजा, अमीर आदि पुरुष सदा सुखी ही होंगे। यदि दुःख से सुख मिलता है तो फिर अनेक प्रकार के दुःख झेलने वाले लोग अगले जन्मों में सुखी होंगे। किन्तु ऐसा होता नहीं है।
___ इसलिये सुख से सुख प्राप्त होता है या दुःख से सुख प्राप्त होता है- ये दोनों मिथ्या सिद्धान्त हैं। सुख की प्राप्ति कर्मनिर्जरा से होती है । भगवान् महावीर ने कहा है-'जे निज्जिण्णे से सुहे।" १. चूणि, पृ० ६५-६६ : राजानो भूत्वा वनवासं गताः .... एतेसि पत्तेयबुद्धाणं । २. चूणि, पृ०६६ : इह सम्मत त्ति इहापि ते इसिभासितेसु पढिज्जंति। णमी ताव णमिपब्वज्जाए सेसा सव्वे अण्णे इसिभासितेसु ।... ३. वही, पृ० १०० : कस्मान्मृषावादः पूर्वमुपदिष्टः ? न प्राणातिपातः? इति, उच्यते, सत्यवतो हि व्रतानि भवन्ति, नासत्यवतः,
अनृतिको हि प्रतिज्ञालोपमपि कुर्यात्, प्रतिज्ञालोपे च सति किं बतानामवशिष्टम् ? ४. भगवती, ७/१६० ।
Jain Education Intemational
Education International
For Private & Personal Use Only
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org