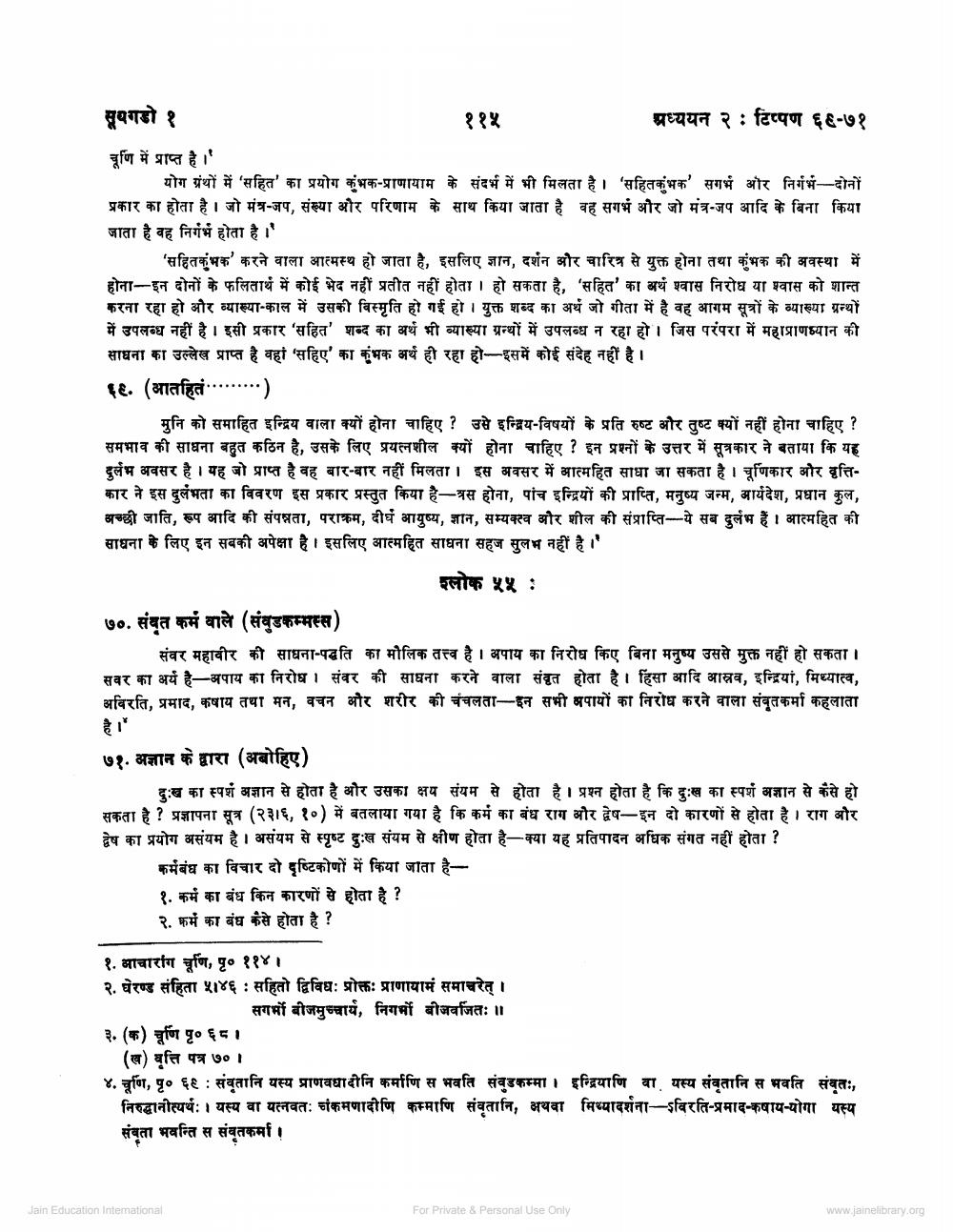________________
सूयगडो १
११५
अध्ययन २ : टिप्पण ६९-७१ चूणि में प्राप्त है।
योग ग्रंथों में 'सहित' का प्रयोग कुंभक-प्राणायाम के संदर्भ में भी मिलता है। 'सहितकुंभक' सगर्भ और निर्गर्भ-दोनों प्रकार का होता है । जो मंत्र-जप, संख्या और परिणाम के साथ किया जाता है वह सगभं और जो मंत्र-जप आदि के बिना किया जाता है वह निर्गर्भ होता है।'
'सहितकुंभक' करने वाला आत्मस्थ हो जाता है, इसलिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र से युक्त होना तथा कुंभक की अवस्था में होना-इन दोनों के फलितार्थ में कोई भेद नहीं प्रतीत नहीं होता। हो सकता है, 'सहित' का अर्थ श्वास निरोध या श्वास को शान्त करना रहा हो और व्याख्या-काल में उसकी विस्मृति हो गई हो । युक्त शब्द का अर्थ जो गीता में है वह आगम सूत्रों के व्याख्या ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार 'सहित' शब्द का अर्थ भी व्याख्या ग्रन्थों में उपलब्ध न रहा हो। जिस परंपरा में महाप्राणध्यान की साधना का उल्लेख प्राप्त है वहां 'सहिए' का कुंभक अर्थ ही रहा हो-इसमें कोई संदेह नहीं है। ६६. (आतहितं.........)
मुनि को समाहित इन्द्रिय वाला क्यों होना चाहिए ? उसे इन्द्रिय-विषयों के प्रति रुष्ट और तुष्ट क्यों नहीं होना चाहिए ? समभाव की साधना बहुत कठिन है, उसके लिए प्रयत्नशील क्यों होना चाहिए ? इन प्रश्नों के उत्तर में सूत्रकार ने बताया कि यह दुर्लभ अवसर है । यह जो प्राप्त है वह बार-बार नहीं मिलता। इस अवसर में आत्महित साधा जा सकता है । चूर्णिकार और वृत्तिकार ने इस दुर्लभता का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है-स होना, पांच इन्द्रियों की प्राप्ति, मनुष्य जन्म, आर्यदेश, प्रधान कुल, अच्छी जाति, रूप आदि की संपन्नता, पराक्रम, दीर्घ आयुष्य, ज्ञान, सम्यक्त्व और शील की संप्राप्ति-ये सब दुर्लभ हैं । आत्महित की साधना के लिए इन सबकी अपेक्षा है। इसलिए आत्महित साधना सहज सुलभ नहीं है।'
श्लोक ५५ : ७०. संवृत कर्म वाले (संवुडकम्मस्स)
संवर महावीर की साधना-पद्धति का मौलिक तत्त्व है । अपाय का निरोध किए बिना मनुष्य उससे मुक्त नहीं हो सकता। सवर का अर्थ है-अपाय का निरोध। संवर की साधना करने वाला संवृत होता है। हिंसा आदि आस्रव, इन्द्रियां, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा मन, वचन और शरीर की चंचलता-इन सभी अपायों का निरोध करने वाला संवृतकर्मा कहलाता
७१. अज्ञान के द्वारा (अबोहिए)
दुःख का स्पर्श अज्ञान से होता है और उसका क्षय संयम से होता है। प्रश्न होता है कि दुःख का स्पर्श अज्ञान से कैसे हो सकता है ? प्रज्ञापना सूत्र (२३१६, १०) में बतलाया गया है कि कर्म का बंध राग और द्वेष-इन दो कारणों से होता है। राग और द्वेष का प्रयोग असंयम है । असंयम से स्पृष्ट दुःख संयम से क्षीण होता है क्या यह प्रतिपादन अधिक संगत नहीं होता ?
कर्मबंध का विचार दो दृष्टिकोणों में किया जाता है१. कर्म का बंध किन कारणों से होता है ? २. फर्म का बंध कैसे होता है ?
१. आचारांग चूणि, पृ० ११४ । २. घेरण्ड संहिता ५१४६ : सहितो द्विविधः प्रोक्तः प्राणायाम समाचरेत् ।
सगो बीजमुच्चार्य, निगर्भो बीजवजितः ॥ ३. (क) चूणि पृ०६८।
(ख) वृत्ति पत्र ७०। ४. चूर्णि, पृ० ६६ : संवृतानि यस्य प्राणवधादीनि कर्माणि स भवति संवुडकम्मा। इन्द्रियाणि वा यस्य संवृतानि स भवति संवृतः, निरुद्धानीत्यर्थः । यस्य वा यत्नवतः चकमणादीणि कम्माणि संवृतानि, अथवा मिथ्यादर्शना-विरति-प्रमाद-कषाय-योगा यस्य संवृता भवन्ति स संवृतकर्मा ।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org