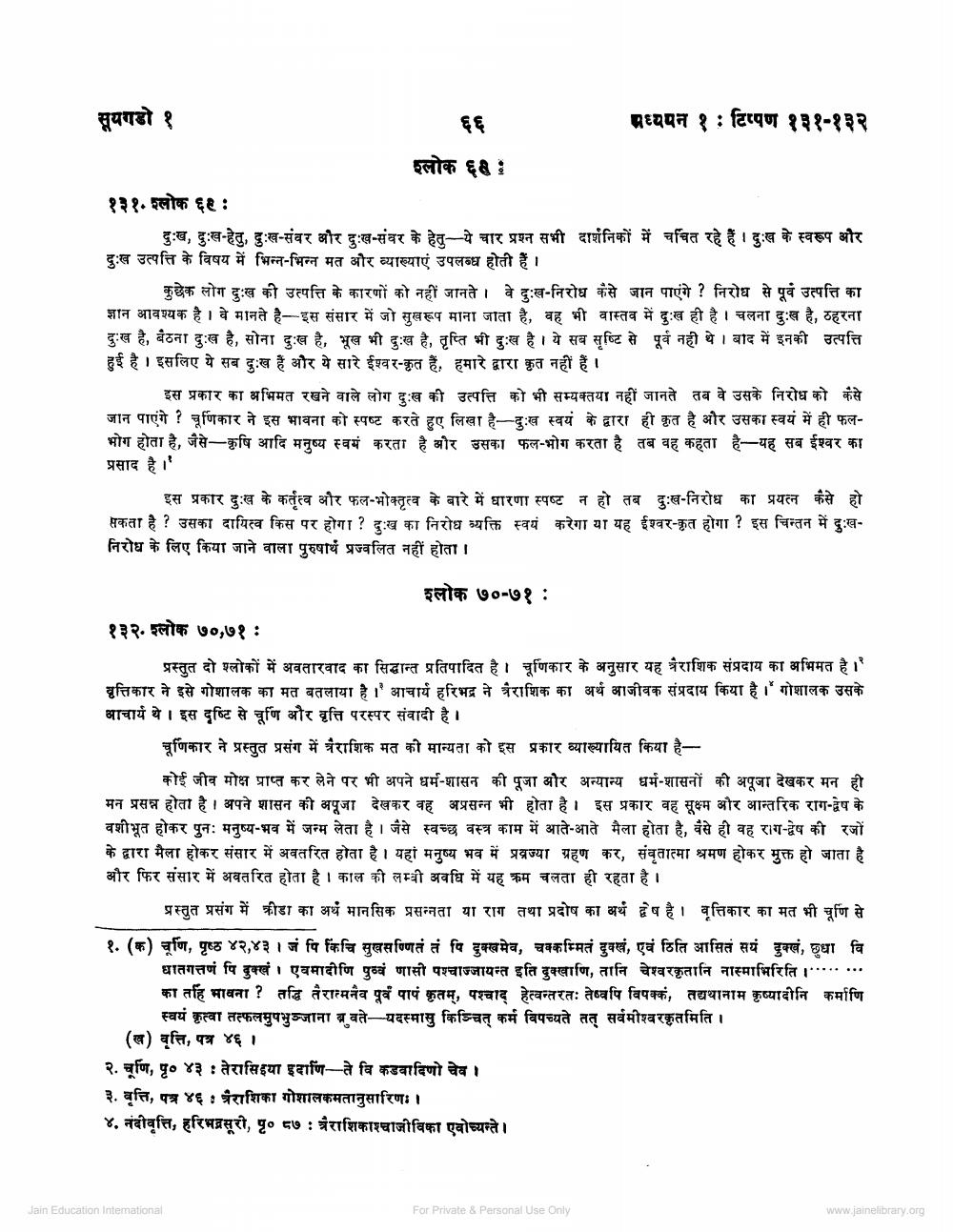________________
सूयगडो १
मध्ययन १ : टिप्पण १३१-१३२
श्लोक ६: १३१. श्लोक ६९:
दुःख, दुःख-हेतु, दुःख-संवर और दुःख-संवर के हेतु-ये चार प्रश्न सभी दार्शनिकों में चचित रहे हैं । दुःख के स्वरूप और दुःख उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न मत और व्याख्याएं उपलब्ध होती हैं।
कुछेक लोग दुःख की उत्पत्ति के कारणों को नहीं जानते। वे दुःख-निरोध कैसे जान पाएंगे ? निरोध से पूर्व उत्पत्ति का ज्ञान आवश्यक है । वे मानते है-इस संसार में जो सुखरूप माना जाता है, वह भी वास्तव में दुःख ही है । चलना दुःख है, ठहरना दुःख है, बैठना दुःख है, सोना दुःख है, भूख भी दुःख है, तृप्ति भी दुःख है। ये सब सृष्टि से पूर्व नही थे। बाद में इनकी उत्पत्ति हुई है । इसलिए ये सब दुःख हैं और ये सारे ईश्वर-कृत हैं, हमारे द्वारा कृत नहीं हैं ।
इस प्रकार का अभिमत रखने वाले लोग दुःख की उत्पत्ति को भी सम्यक्तया नहीं जानते तब वे उसके निरोध को कैसे जान पाएंगे? चूर्णिकार ने इस भावना को स्पष्ट करते हुए लिखा है-दुःख स्वयं के द्वारा ही कृत है और उसका स्वयं में ही फलभोग होता है, जैसे-कृषि आदि मनुष्य स्वयं करता है और उसका फल-भोग करता है तब वह कहता है-यह सब ईश्वर का प्रसाद है।
इस प्रकार दुःख के कर्तृत्व और फल-भोक्तृत्व के बारे में धारणा स्पष्ट न हो तब दुःख-निरोध का प्रयत्न कैसे हो सकता है ? उसका दायित्व किस पर होगा? दुःख का निरोध व्यक्ति स्वयं करेगा या यह ईश्वर-कृत होगा? इस चिन्तन में दुःखनिरोध के लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ प्रज्वलित नहीं होता।
श्लोक ७०-७१:
१३२. श्लोक ७०,७१
प्रस्तुत दो श्लोकों में अवतारवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित है। चूणिकार के अनुसार यह राशिक संप्रदाय का अभिमत है। वृत्तिकार ने इसे गोशालक का मत बतलाया है। आचार्य हरिभद्र ने त्रैराशिक का अर्थ आजीवक संप्रदाय किया है। गोशालक उसके आचार्य थे। इस दृष्टि से चूणि और वृत्ति परस्पर संवादी है।
चूर्णिकार ने प्रस्तुत प्रसंग में त्रैराशिक मत को मान्यता को इस प्रकार व्याख्यायित किया है
कोई जीव मोक्ष प्राप्त कर लेने पर भी अपने धर्म-शासन की पूजा और अन्यान्य धर्म-शासनों की अपूजा देखकर मन ही मन प्रसन्न होता है । अपने शासन की अपूजा देखकर वह अप्रसन्न भी होता है। इस प्रकार वह सूक्ष्म और आन्तरिक राग-द्वेष के वशीभूत होकर पुनः मनुष्य-भव में जन्म लेता है। जैसे स्वच्छ वस्त्र काम में आते-आते मैला होता है, वैसे ही वह राग-द्वेष की रजों के द्वारा मैला होकर संसार में अवतरित होता है। यहां मनुष्य भव में प्रव्रज्या ग्रहण कर, संवृतात्मा श्रमण होकर मुक्त हो जाता है और फिर संसार में अवतरित होता है । काल की लम्बी अवधि में यह क्रम चलता ही रहता है।
प्रस्तुत प्रसंग में क्रीडा का अर्थ मानसिक प्रसन्नता या राग तथा प्रदोष का अर्थ द्वेष है। वृत्तिकार का मत भी चूणि से १. (क) चूणि, पृष्ठ ४२,४३ । जं पि किंचि सुखसणितं तं पि दुक्खमेव, चक्कम्मितं दुवखं, एवं ठिति आसितं सयं दुक्खं, छुधा वि
धातगत्तणं पि दुक्खं । एवमादीणि पुव्वं णासी पश्चाज्जायन्त इति दुक्खाणि, तानि चेश्वरकृतानि नास्माभिरिति ।....." का तर्हि भावना ? तद्धि तैरात्मनैव पूर्व पापं कृतम्, पश्चाद् हेत्वन्तरतः तेष्वपि विपक्कं, तद्यथानाम कृष्यादीनि कर्माणि
स्वयं कृत्वा तत्फलमुपभुजाना ब्रुवते यदस्मासु किञ्चित् कर्म विपच्यते तत् सर्वमीश्वरकृतमिति । (ख) वृत्ति, पत्र ४६ । २. चूणि, पृ० ४३: तेरासिइया इदाणि-ते वि कडवादिणो चेव । ३. वृत्ति, पत्र ४६ राशिका गोशालकमतानुसारिणः। ४. नंदीवृत्ति, हरिभद्रसूरी, पृ० ८७ : त्रैराशिकाश्चाजीविका एवोच्यन्ते।
Jain Education Intemational
For Private & Personal use only
www.jainelibrary.org