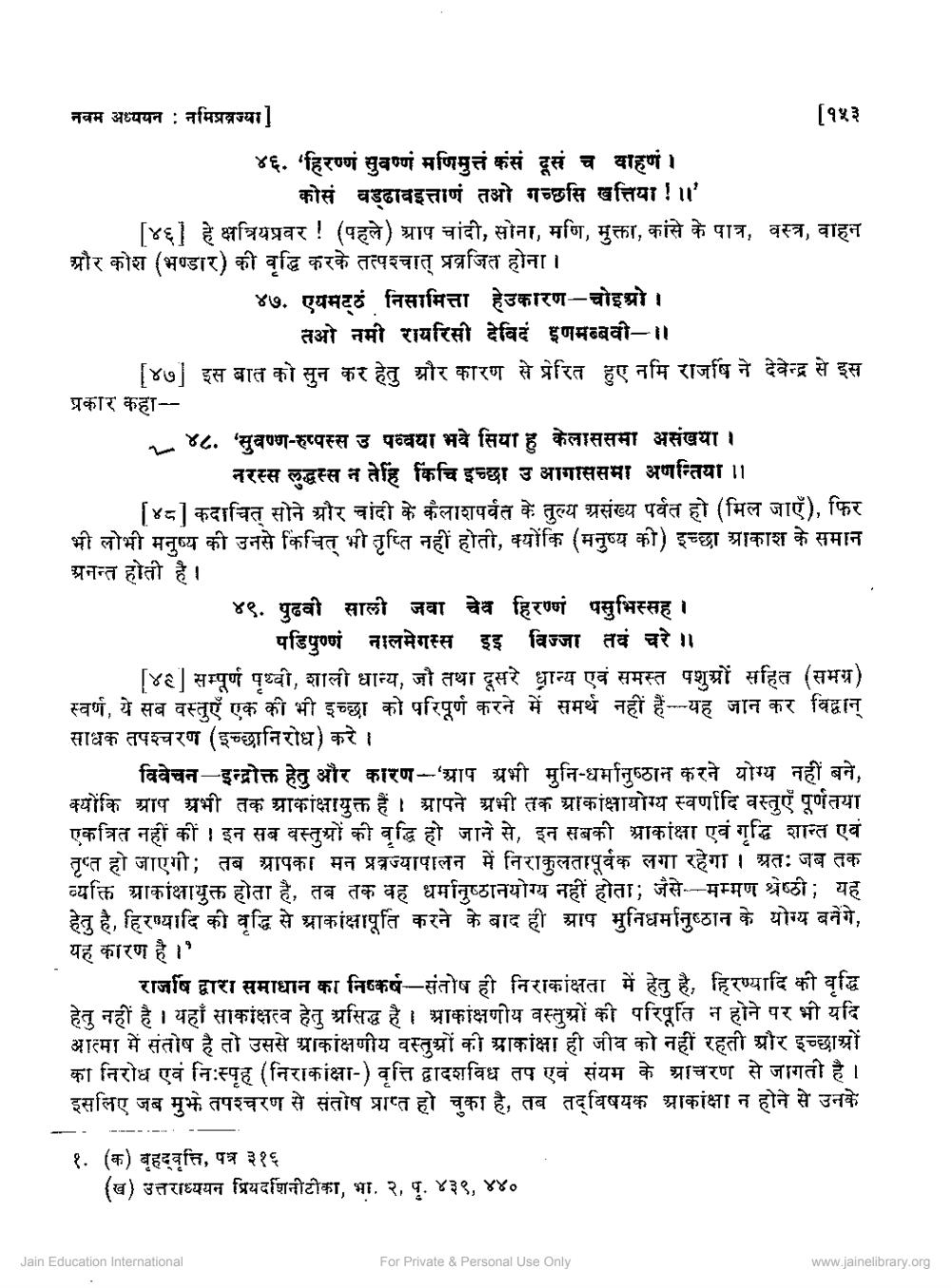________________ नवम अध्ययन : नमिप्रव्रज्या] [153 46. 'हिरण्णं सुवण्णं मणिमुत्तं कसं दूसं च वाहणं / कोसं बड्ढावइत्ताणं तओ गच्छसि खत्तिया!।' [46] हे क्षत्रियप्रवर ! (पहले) पाप चांदी, सोना, मणि, मुक्ता, कांसे के पात्र, वस्त्र, वाहन और कोश (भण्डार) की वृद्धि करके तत्पश्चात् प्रवजित होना।। 47. एयमढें निसामित्ता हेउकारण-चोइयो। तओ नमी रायरिसी देविदं इणमब्बवी-॥ [47] इस बात को सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजर्षि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा 48. 'सुवण्ण-रुप्पस्स उ पव्वया भवे सिया हु केलाससमा असंखया। नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि इच्छा उ आगाससमा अणन्तिया / / [48] कदाचित् सोने और चांदी के कैलाशपर्वत के तुल्य असंख्य पर्वत हो (मिल जाएँ), फिर भी लोभी मनुष्य की उनसे किंचित् भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि (मनुष्य की) इच्छा आकाश के समान अनन्त होती है। 49. पुढवी साली जवा चेव हिरण्णं पसुभिस्सह / पडिपुण्णं नालमेगस्स इइ विज्जा तवं चरे // [46 ] सम्पूर्ण पृथ्वी, शाली धान्य, जौ तथा दूसरे धान्य एवं समस्त पशुओं सहित (समग्र) स्वर्ण, ये सब वस्तुएँ एक की भी इच्छा को परिपूर्ण करने में समर्थ नहीं हैं यह जान कर विद्वान् साधक तपश्चरण (इच्छानिरोध) करे / विवेचनइन्द्रोक्त हेतु और कारण-'आप अभी मुनि-धर्मानुष्ठान करने योग्य नहीं बने, क्योंकि आप अभी तक आकांक्षायुक्त हैं। आपने अभी तक आकांक्षायोग्य स्वर्णादि वस्तुएँ पूर्णतया एकत्रित नहीं की। इन सब वस्तुओं की वृद्धि हो जाने से, इन सबकी आकांक्षा एवं गृद्धि शान्त एवं तृप्त हो जाएगी; तब अापका मन प्रव्रज्यापालन में निराकुलतापूर्वक लगा रहेगा / अतः जब तक व्यक्ति अाकांक्षायुक्त होता है, तब तक वह धर्मानुष्ठानयोग्य नहीं होता; जैसे--मम्मण श्रेष्ठी ; यह हेतु है, हिरण्यादि की वृद्धि से आकांक्षापूर्ति करने के बाद ही आप मुनिधर्मानुष्ठान के योग्य बनेंगे, यह कारण है।' राजर्षि द्वारा समाधान का निष्कर्ष-संतोष ही निराकांक्षता में हेतु है, हिरण्यादि की वृद्धि हेतु नहीं है / यहाँ साकांक्षत्व हेतु असिद्ध है। आकांक्षणीय वस्तुओं की परिपूर्ति न होने पर भी यदि आत्मा में संतोष है तो उससे अाकांक्षणीय वस्तुओं की आकांक्षा ही जीव को नहीं रहती और इच्छाओं का निरोध एवं निःस्पृह (निराकांक्षा-) वृत्ति द्वादशविध तप एवं संयम के आचरण से जागती है / इसलिए जब मुझे तपश्चरण से संतोष प्राप्त हो चका है, तब तदविषयक आकांक्षा न होने से उनके 1. (क) बृहद्वृत्ति, पत्र 316 (ख) उत्तराध्ययन प्रियदशिनीटीका, भा. 2, पृ. 439, 440 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org