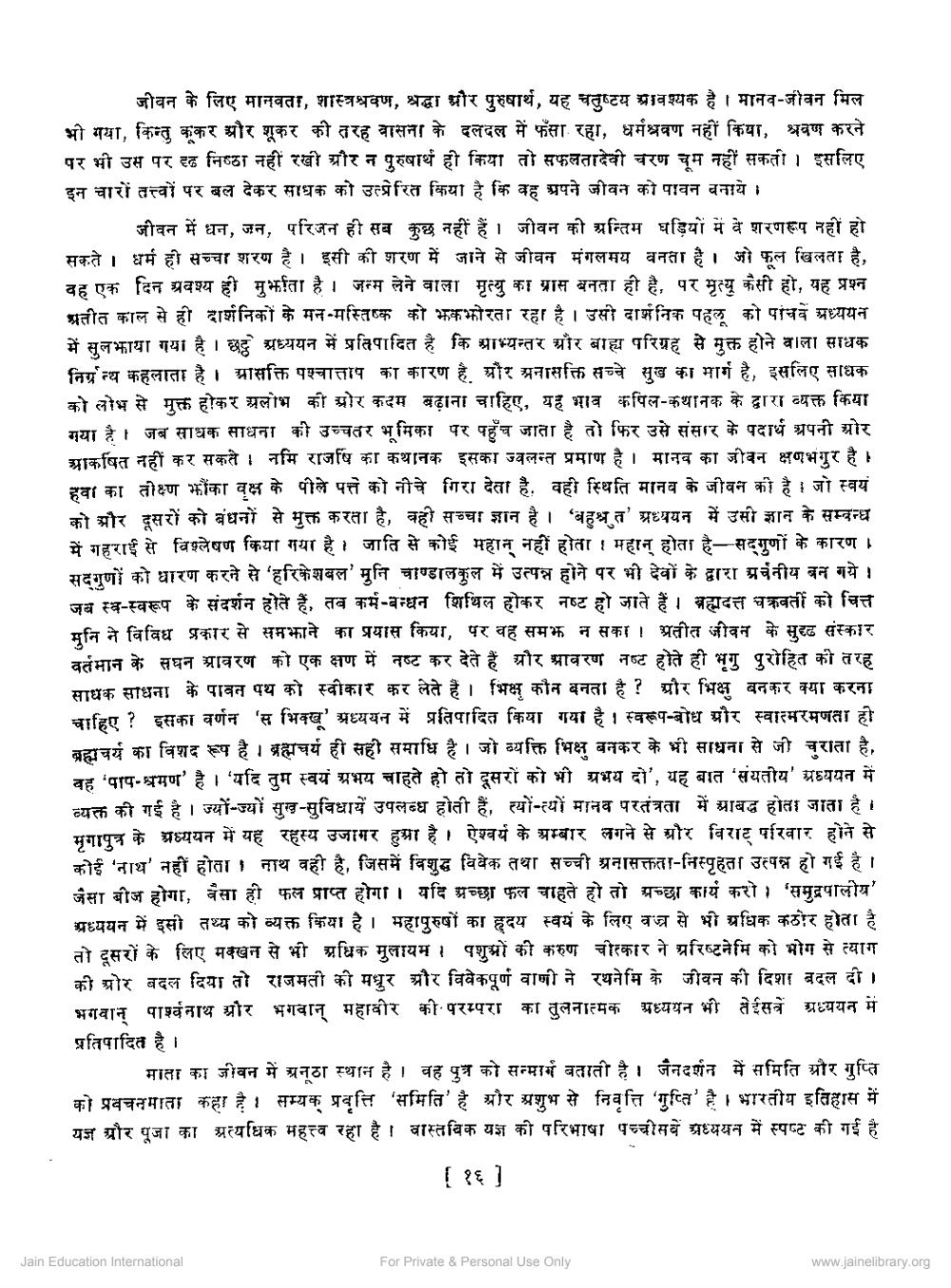________________ जीवन के लिए मानवता, शास्त्रश्रवण, श्रद्धा और पुरुषार्थ, यह चतुष्टय आवश्यक है / मानव-जीवन मिल भी गया, किन्तु ककर और शूकर की तरह वासना के दलदल में फंसा रहा, धर्मश्रवण नहीं किया, श्रवण करने पर भी उस पर दृढ निष्ठा नहीं रखी और न पुरुषार्थ ही किया तो सफलतादेवी चरण चूम नहीं सकती। इसलिए इन चारों तत्त्वों पर बल देकर साधक को उत्प्रेरित किया है कि वह अपने जीवन को पावन बनाये। जीवन में धन, जन, परिजन ही सब कुछ नहीं हैं। जीवन को अन्तिम घड़ियों में वे शरणरूप नहीं हो सकते। धर्म ही सच्चा शरण है। इसी की शरण में जाने से जीवन मंगलमय बनता है। जो फल खिलता है, वह एक दिन अवश्य ही मुझर्भाता है। जन्म लेने वाला मृत्यु का ग्रास बनता ही है, पर मृत्यू कैसी हो, यह प्रश्न प्रतीत काल से ही दार्शनिकों के मन-मस्तिष्क को झकझोरता रहा है। उसी दार्शनिक पहल को पांचवें अध्ययन में सुलझाया गया है। छ? अध्ययन में प्रतिपादित है कि प्राभ्यन्तर और बाह्य परिग्रह से मुक्त होने वाला साधक निर्ग्रन्थ कहलाता है। ग्रासक्ति पश्चात्ताप का कारण है. और अनासक्ति सच्चे सुख का मार्ग है, इसलि को लोभ से मुक्त होकर अलोभ की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, यह भाव कपिल-कथानक के द्वारा व्यक्त किया गया है। जब साधक साधना की उच्चतर भूमिका पर पहुँच जाता है तो फिर उसे संसार के पदार्थ अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते / नमि राजर्षि का कथानक इसका ज्वलन्त प्रमाण है। मानव का जीवन क्षणभगुर है। हवा का तीक्ष्ण झौंका वृक्ष के पीले पत्ते को नीचे गिरा देता है. वही स्थिति मानव के जीवन की है। जो स्वयं को और दूसरों को बंधनों से मुक्त करता है, वही सच्चा ज्ञान है। 'बहुश्रुत' अध्ययन में उसी ज्ञान के सम्बन्ध में गहराई से विश्लेषण किया गया है। जाति से कोई महान नहीं होता / महान होता है-सद्गुणों के कारण / सदगुणों को धारण करने से 'हरिकेशबल' मुनि चाण्डालकुल में उत्पन्न होने पर भी देवों के द्वारा अर्चनीय बन गये। जब स्व-स्वरूप के संदर्शन होते हैं, तब कर्म-बन्धन शिथिल होकर नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को चित्त मनिने विविध प्रकार से समझाने का प्रयास किया, पर वह समझ न सका। अतीत जीवन के सुदृढ वर्तमान के सघन आवरण को एक क्षण में नष्ट कर देते हैं और प्रावरण नष्ट होते ही भृगु पुरोहित की तरह साधक साधना के पावन पथ को स्वीकार कर लेते हैं / भिक्षु कौन बनता है ? और भिक्षु बनकर क्या करना चाहिए? इसका वर्णन 'स भिक्खू' अध्ययन में प्रतिपादित किया गया है / स्वरूप-बोध और स्वात्मरमणता ही ब्रह्मचर्य का विशद रूप है। ब्रह्मचर्य ही सही समाधि है। जो व्यक्ति भिक्षु बनकर के भी साधना से जी चुराता है, वह 'पाप-श्रमण' है / 'यदि तुम स्वयं अभय चाहते हो तो दूसरों को भी अभय दो', यह बात 'संयतीय' अध्ययन में व्यक्त की गई है। ज्यों-ज्यों सुख-सुविधायें उपलब्ध होती हैं, त्यों-त्यों मानव परतंत्रता में प्राबद्ध होता जाता है। मगापूत्र के अध्ययन में यह रहस्य उजागर हुआ है। ऐश्वर्य के अम्बार लगने से और विराट परिवार होने से कोई 'नाथ' नहीं होता। नाथ वही है, जिसमें विशुद्ध विवेक तथा सच्ची अनासक्तता-निस्पृहता उत्पन्न हो गई है। जैसा बीज होगा, वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि अच्छा फल चाहते हो तो अच्छा कार्य करो। 'समुद्रपालीय' अध्ययन में इसी तथ्य को व्यक्त किया है। महापुरुषों का हृदय स्वयं के लिए वज्र से भी अधिक कठोर होता है को दसरों के लिए मक्खन से भी अधिक मुलायम / पशुओं की करुण चीत्कार ने अरिष्टनेमि को भोग से त्याग की पोर बदल दिया तो राजमती की मधुर और विवेकपूर्ण वाणी ने रथनेमि के जीवन की दिशा बदल दी। भगवान पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर की परम्परा का तुलनात्मक अध्ययन भी तेईसवें अध्ययन में प्रतिपादित है। माता का जीवन में अनूठा स्थान है। वह पुत्र को सन्मार्ग बताती है। जैनदर्शन में समिति और गुप्ति को प्रवचनमाता कहा है। सम्यक प्रवृत्ति 'समिति' है और अशुभ से निवृत्ति 'गुप्ति' है। भारतीय इतिहास में यज्ञ और पुजा का अत्यधिक महत्त्व रहा है। वास्तविक यज्ञ की परिभाषा पच्चीसवें अध्ययन में स्पष्ट की गई है Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org