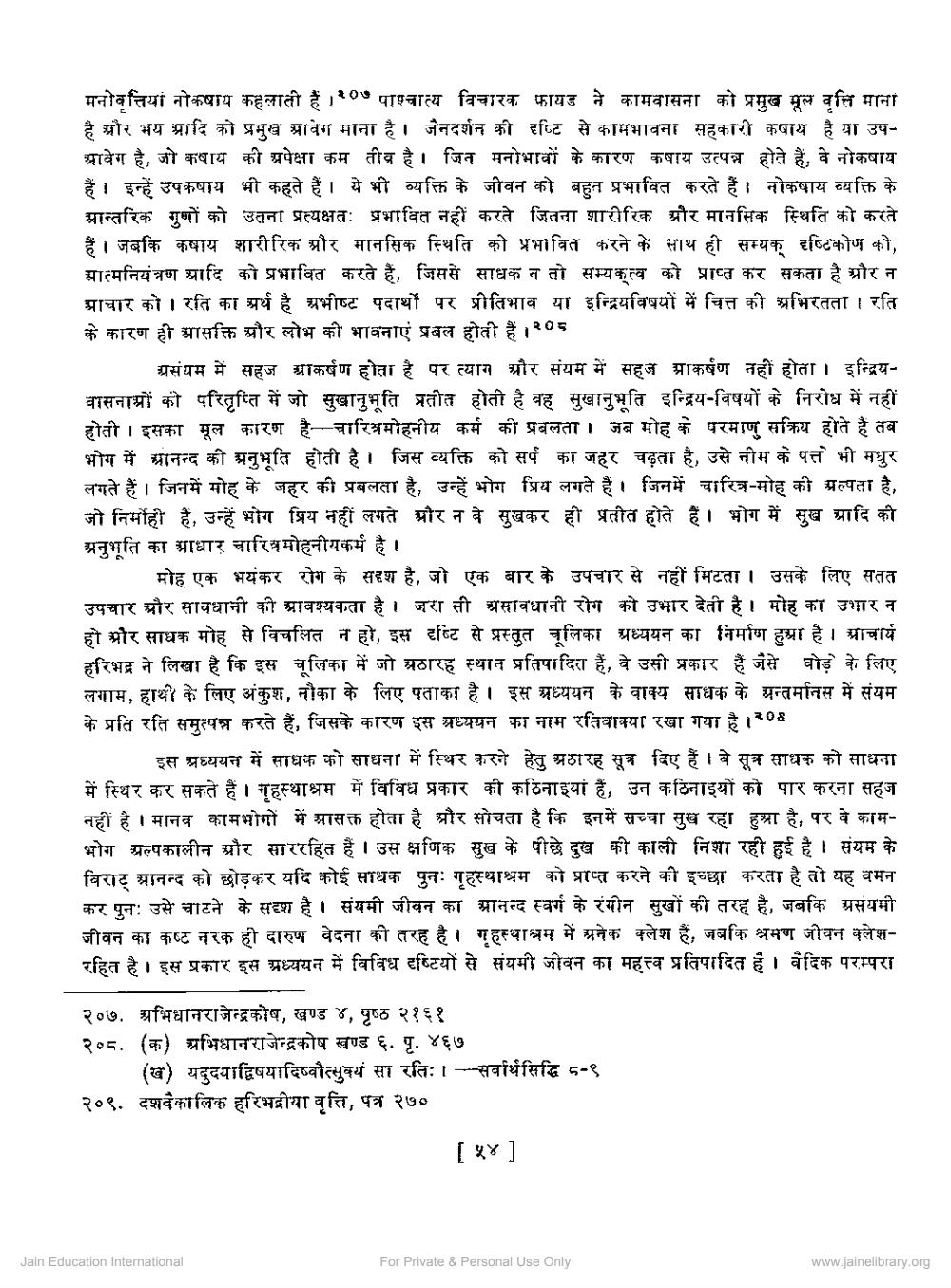________________ मनोवत्तियां नोकषाय कहलाती हैं / 20deg पाश्चात्य विचारक फायड ने कामवासना को प्रमुख मूल वृत्ति माना है और भय आदि को प्रमुख आवेग माना है। जैनदर्शन की दृष्टि से कामभावना सहकारी कषाय है या उपआवेग है, जो कषाय की अपेक्षा कम तीव्र है। जिन मनोभावों के कारण कषाय उत्पन्न होते हैं, वे नोकषाय हैं। इन्हें उपकषाय भी कहते हैं। ये भी व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। नोकषाय व्यक्ति के आन्तरिक गुणों को उतना प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करते जितना शारीरिक और मानसिक स्थिति को करते हैं। जबकि कषाय शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करने के साथ ही सम्यक दृष्टिकोण को, आत्मनियंत्रण आदि को प्रभावित करते हैं, जिससे साधक न तो सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है और न प्राचार को / रति का अर्थ है अभीष्ट पदार्थों पर प्रीतिभाव या इन्द्रियविषयों में चित्त की अभिरतता। रति के कारण ही आसक्ति और लोभ की भावनाएं प्रबल होती हैं / 206 असंयम में सहज आकर्षण होता है पर त्याग और संयम में सहज आकर्षण नहीं होता। इन्द्रियवासनामों को परितृप्ति में जो सुखानुभूति प्रतीत होती है वह सुखानुभूति इन्द्रिय-विषयों के निरोध में नहीं होती / इसका मूल कारण है-चारित्रमोहनीय कर्म की प्रबलता। जब मोह के परमाणु सक्रिय होते हैं तब भोग में प्रानन्द की अनुभूति होती है। जिस व्यक्ति को सर्प का जहर चढ़ता है, उसे नीम के पत्ते भी मधुर लगते हैं। जिनमें मोह के जहर की प्रबलता है, उन्हें भोग प्रिय लगते हैं। जिनमें चारित्र-मोह की अल्पता है, जो निर्मोही हैं, उन्हें भोग प्रिय नहीं लगते और न वे सुखकर ही प्रतीत होते हैं। भोग में सुख प्रादि की अनुभति का आधार चारित्रमोहनीयकर्म है। मोह एक भयंकर रोग के सहश है, जो एक बार के उपचार से नहीं मिटता / उसके लिए सतत उपचार और सावधानी की आवश्यकता है। जरा सी असावधानी रोग को उभार देती है। मोह का उभार न हो और साधक मोह से विचलित न हो, इस दृष्टि से प्रस्तुत चूलिका अध्ययन का निर्माण हुआ है। प्राचार्य हरिभद्र ने लिखा है कि इस चुलिका में जो अठारह स्थान प्रतिपादित हैं, वे उसी प्रकार हैं जैसे-घोड़े के लिए लगाम, हाथी के लिए अंकुश, नौका के लिए पताका है। इस अध्ययन के वाक्य साधक के अन्तर्मानस में संयम के प्रति रति समुत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इस अध्ययन का नाम रतिवाक्या रखा गया है / 204 इस अध्ययन में साधक को साधना में स्थिर करने हेतु अठारह सूत्र दिए हैं / वे सूत्र साधक को साधना में स्थिर कर सकते हैं। गहस्थाश्रम में विविध प्रकार की कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को पार करना सहज नहीं है / मानव कामभोगों में आसक्त होता है और सोचता है कि इनमें सच्चा सुख रहा हुया है, पर वे कामभोग अल्पकालीन और साररहित हैं / उस क्षणिक सुख के पीछे दुख की काली निशा रही हुई है। संयम के विराट अानन्द को छोड़कर यदि कोई साधक पुनः गृहस्थाश्रम को प्राप्त करने की इच्छा करता है तो यह वमन कर पुनः उसे चाटने के सदृश है। संयमी जीवन का आनन्द स्वर्ग के रंगीन सुखों की तरह है, जबकि असंयमी जीवन का कष्ट नरक ही दारुण वेदना की तरह है। गहस्थाश्रम में अनेक क्लेश हैं, जबकि श्रमण जीवन क्लेशरहित है। इस प्रकार इस अध्ययन में विविध दृष्टियों से संयमी जीवन का महत्त्व प्रतिपादित है। वैदिक परम्परा 207. अभिधानराजेन्द्रकोष, खण्ड 4, पृष्ठ 2161 208. (क) अभिधानराजेन्द्रकोष खण्ड 6. पृ. 467 (ख) यदुदयाद्विषयादिष्वौत्सुक्यं सा रतिः / सर्वार्थसिद्धि 8-9 209. दशवकालिक हरिभद्रीया वृत्ति, पत्र 270 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org