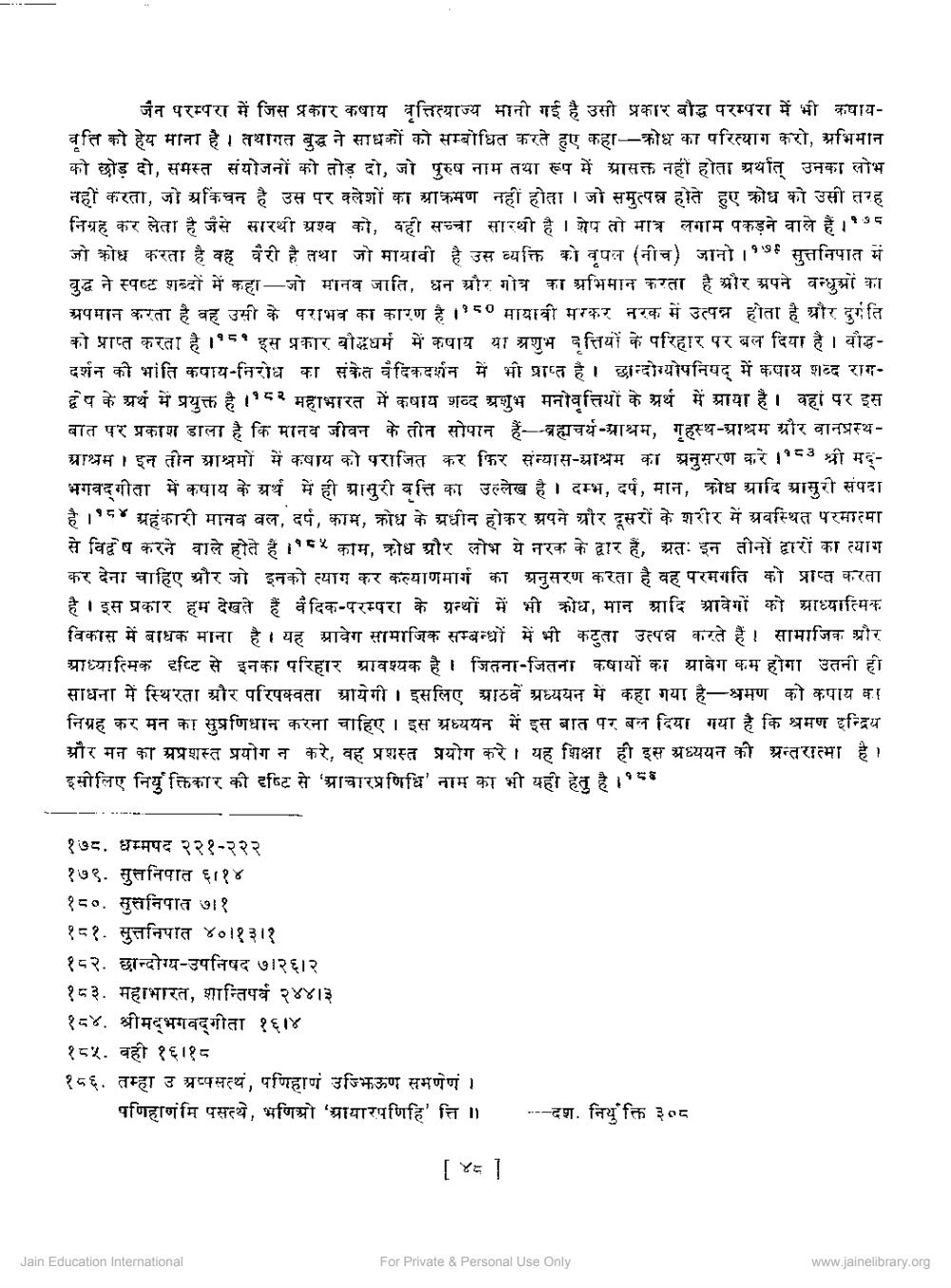________________ जैन परम्परा में जिस प्रकार कषाय वृत्तित्याज्य मानी गई है उसी प्रकार बौद्ध परम्परा में भी कषायबति को हेय माना है। तथागत बुद्ध ने साधकों को सम्बोधित करते हए कहा--क्रोध का परित्याग करो, अभिमान को छोड़ दो, समस्त संयोजनों को तोड़ दो, जो पुरुष नाम तथा रूप में आसक्त नहीं होता अर्थात् उनका लोभ नहीं करता, जो अकिंचन है उस पर क्लेशों का आक्रमण नहीं होता / जो समुत्पन्न होते हुए क्रोध को उसी तरह निग्रह कर लेता है जैसे सारथी अश्व को, वही सच्चा सारथी है / शेष तो मात्र लगाम पकड़ने वाले हैं।'३८ जो क्रोध करता है वह वैरी है तथा जो मायावी है उस व्यक्ति को वपल (नीच) जानो / 176 सुत्तनिपात में बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा—जो मानव जाति, धन और गोत्र का अभिमान करता है और अपने वन्धुओं का अपमान करता है वह उसी के पराभव का कारण है। 180 मायावी मरकर नरक में उत्पन्न होता है और दुर्गति को प्राप्त करता है / 181 इस प्रकार बौद्धधर्म में कषाय या अशुभ वृत्तियों के परिहार पर बल दिया है / बौद्धदर्शन की भांति कपाय-निरोध का संकेत वैदिकदर्शन में भी प्राप्त है। छान्दोग्योपनियद् में कपाय शब्द रामद्वेष के अर्थ में प्रयुक्त है / 82 महाभारत में कषाय शब्द अशुभ मनोवृत्तियों के अर्थ में पाया है। वहां पर इस बात पर प्रकाश डाला है कि मानव जीवन के तीत सोपान हैं--ब्रह्मचर्य-पाश्रम, गृहस्थ-पाश्रम और वानप्रस्थप्राश्रम। इन तीन आश्रमों में कषाय को पराजित कर फिर संन्यास-याश्रम का अनुसरण करे / 183 श्री मद्भगवद्गीता में कषाय के अर्थ में ही आसुरी वत्ति का उल्लेख है। दम्भ, दर्प, मान, क्रोध आदि आसुरी संपदा है / 84 अहंकारी मानव बल, दर्प, काम, क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में अवस्थित परमात्मा से विद्वेष करने वाले होते हैं।'६५ काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं, अतः इन तीनों द्वारों का त्याग कर देना चाहिए और जो इनको त्याग कर कल्याणमार्ग का अनुसरण करता है वह परमगति को प्राप्त करता है / इस प्रकार हम देखते हैं वैदिक-परम्परा के ग्रन्थों में भी क्रोध, मान आदि आवेगों को प्राध्यात्मिक विकास में बाधक माना है। यह आवेग सामाजिक सम्बन्धों में भी कटुता उत्पन्न करते हैं। सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इनका परिहार आवश्यक है। जितना-जितना कषायों का आवेग कम होगा उतनी ही साधना में स्थिरता और परिपक्वता पायेगी। इसलिए आठवें अध्ययन में कहा गया है-श्रमण को कपाय ! निग्रह कर मन का सुप्रणिधान करना चाहिए / इस अध्ययन में इस बात पर बल दिया गया है कि श्रमण इन्द्रिय और मन का अप्रशस्त प्रयोग न करे, वह प्रशस्त प्रयोग करे। यह शिक्षा ही इस अध्ययन की अन्तरात्मा है। इसीलिए नियुक्तिकार की दृष्टि से 'प्राचारप्रणिधि' नाम का भी यही हेतु है। 186 178. धम्मपद 221-222 179. सुत्तनिपात 6 / 14 180. सुत्तनिपात 71 181. सुत्तनिपात 40 / 13 / 1 82. छान्दोग्य-उपनिषद 7 / 26 / 2 183. महाभारत, शान्तिपर्व 244 / 3 184. श्रीमद्भगवद्गीता 16 / 4 185. वही 16 / 18 186. तम्हा उ अप्पमत्थं, पणिहाणं उज्झिऊण समणेणं / पणिहाणंमि पसत्थे, भणियो 'पायारपणिहि' त्ति // ..--दश. नियुक्ति 308 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org