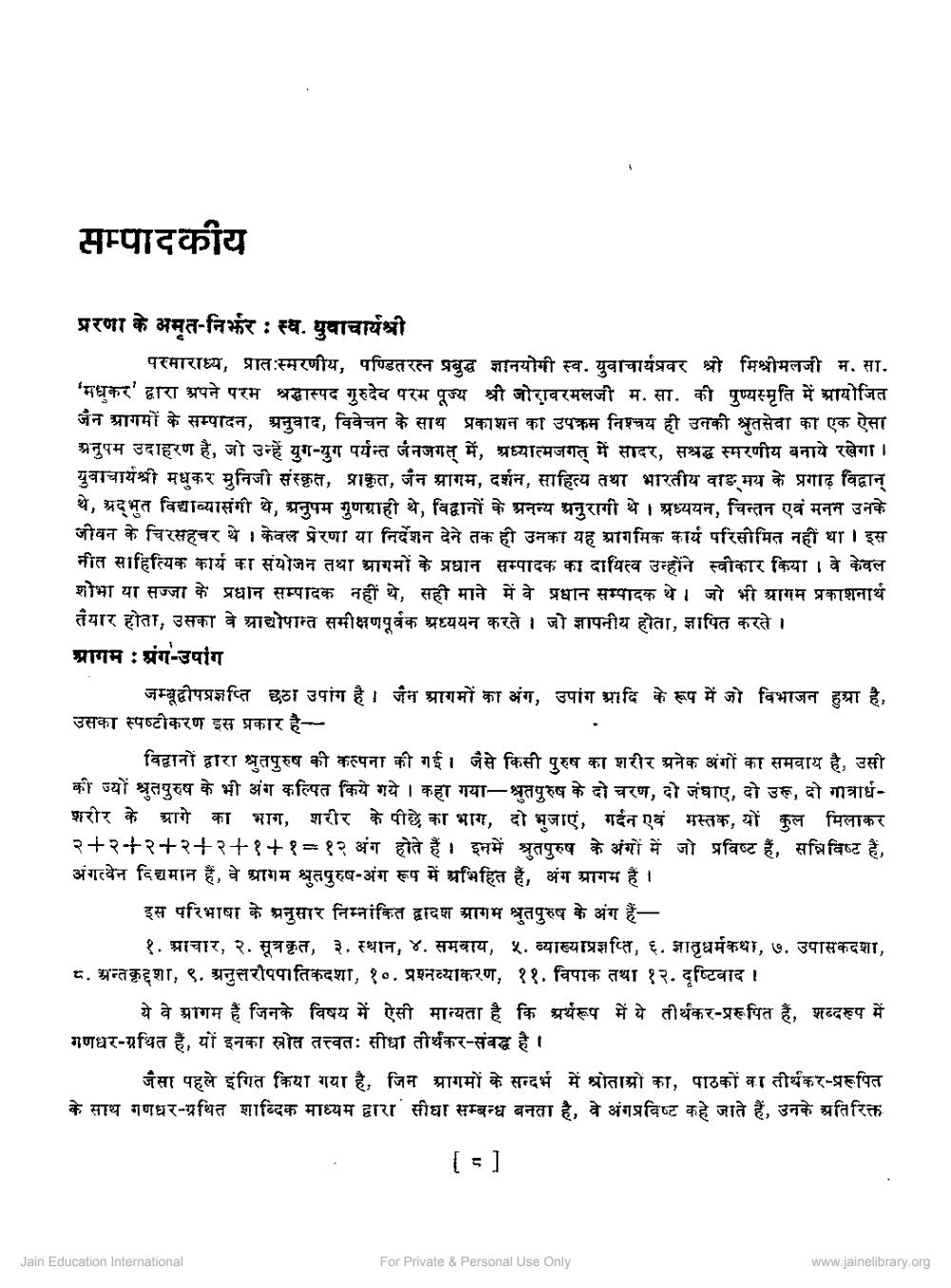________________ सम्पादकीय प्ररणा के अमृत-निर्भर : स्व. युवाचार्यश्री ___ परमाराध्य, प्रातःस्मरणीय, पण्डितरत्न प्रबुद्ध ज्ञानयोगी स्व. युवाचार्यप्रवर श्री मिश्रीमलजी म. सा. 'मधुकर' द्वारा अपने परम श्रद्धास्पद गुरुदेव परम पूज्य श्री जोरावरमलजी म. सा. की पुण्यस्मृति में आयोजित जैन आगमों के सम्पादन, अनुवाद, विवेचन के साथ प्रकाशन का उपक्रम निश्चय ही उनकी श्रुतसेवा का एक ऐसा अनुपम उदाहरण है, जो उन्हें युग-युग पर्यन्त जनजगत् में, अध्यात्मजगत् में सादर, सश्रद्ध स्मरणीय बनाये रखेगा। युवाचार्यश्री मधुकर मुनिजी संस्कृत, प्राकृत, जन प्रागम, दर्शन, साहित्य तथा भारतीय वाङमय के प्रगाढ़ विद्वान् थे, अद्भुत विद्याव्यासंगी थे, अनुपम गुणग्राही थे, विद्वानों के अनन्य अनुरागी थे। अध्ययन, चिन्तन एवं मनन उनके जीवन के चिरसहचर थे। केवल प्रेरणा या निर्देशन देने तक ही उनका यह आगमिक कार्य परिसीमित नहीं था। इस नीत साहित्यिक कार्य का संयोजन तथा आगमों के प्रधान सम्पादक का दायित्व उन्होंने स्वीकार किया। वे केवल शोभा या सज्जा के प्रधान सम्पादक नहीं थे, सही माने में वे प्रधान सम्पादक थे। जो भी आगम प्रकाशनार्थ तैयार होता, उसका वे आद्योपान्त समीक्षणपूर्वक अध्ययन करते। जो ज्ञापनीय होता, ज्ञापित करते। प्रागम : अंग-उपांग जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति छठा उपांग है। जैन आगमों का अंग, उपांग मादि के रूप में जो विभाजन हुया है, उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है विद्वानों द्वारा श्रुतपुरुष की कल्पना की गई। जैसे किसी पुरुष का शरीर अनेक अंगों का समवाय है, उसी की ज्यों श्रुतपुरुष के भी अंग कल्पित किये गये / कहा गया-श्रुतपुरुष के दो चरण, दो जंघाए, दो उरू, दो गात्रार्धशरीर के आगे का भाग, शरीर के पीछे का भाग, दो भुजाएं, गर्दन एवं मस्तक, यों कुल मिलाकर 2+2+2+2+2+1+1=12 अंग होते हैं। इनमें श्रुतपुरुष के अंगों में जो प्रविष्ट हैं, सन्निविष्ट हैं, अंगत्वेन विद्यमान हैं, वे आगम श्रुतपुरुष-अंग रूप में अभिहित हैं, अंग पागम हैं। इस परिभाषा के अनुसार निम्नांकित द्वादश आगम श्रुतपुरुष के अंग हैं 1. प्राचार, 2. सूत्रकृत, 3. स्थान, 4. समवाय, 5. व्याख्याप्रज्ञप्ति, 6. ज्ञातृधर्मकथा, 7. उपासकदशा, 8. अन्तकृद्दशा, 9. अनुत्तरोपपातिकदशा, 10, प्रश्नव्याकरण, 11. विपाक तथा 12. दृष्टिवाद / ये वे आगम हैं जिनके विषय में ऐसी मान्यता है कि अर्थरूप में ये तीर्थंकर-प्ररूपित हैं, शब्दरूप में गणधर-ग्रथित हैं, यों इनका स्रोत तत्त्वतः सीधा तीर्थकर-संबद्ध है। जैसा पहले इंगित किया गया है, जिन प्रागमों के सन्दर्भ में श्रोताओं का, पाठकों का तीर्थकर-प्ररूपित के साथ गणधर-ग्रथित शाब्दिक माध्यम द्वारा सीधा सम्बन्ध बनता है, वे अंगप्रविष्ट कहे जाते हैं, उनके अतिरिक्त [8] Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org