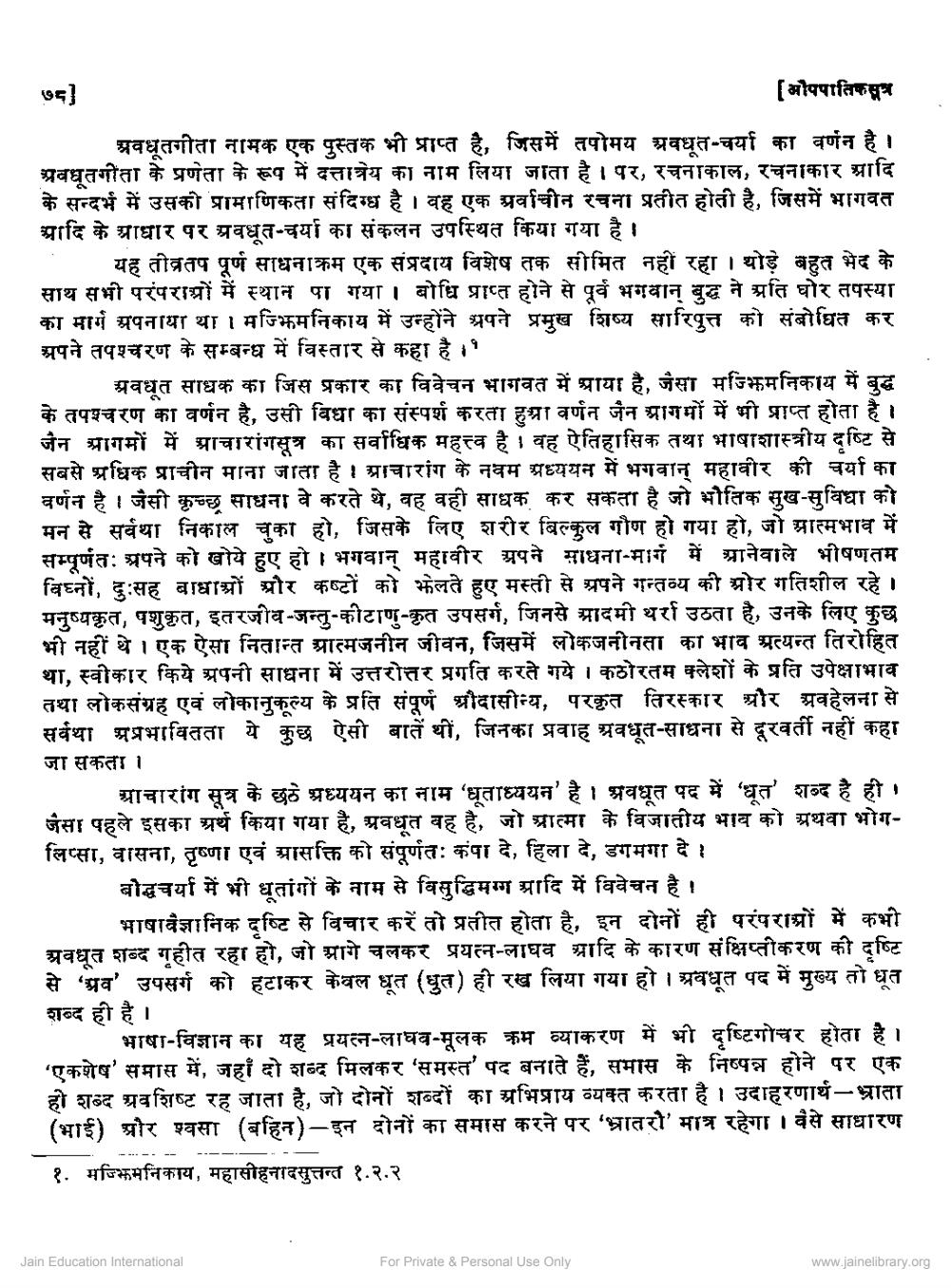________________ [औपपातिकसूत्र अवधूतगीता नामक एक पुस्तक भी प्राप्त है, जिसमें तपोमय अवधूत-चर्या का वर्णन है। अवधूतगीता के प्रणेता के रूप में दत्तात्रेय का नाम लिया जाता है। पर, रचनाकाल, रचनाकार प्रादि के सन्दर्भ में उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है / वह एक अर्वाचीन रचना प्रतीत होती है, जिसमें भागवत आदि के आधार पर अवधूत-चर्या का संकलन उपस्थित किया गया है। यह तीवतप पूर्ण साधनाक्रम एक संप्रदाय विशेष तक सीमित नहीं रहा / थोड़े बहुत भेद के साथ सभी परंपरात्रों में स्थान पा गया। बोधि प्राप्त होने से पूर्व भगवान् बुद्ध ने अति घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। मज्झिमनिकाय में उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य सारिपुत्त को संबोधित कर अपने तपश्चरण के सम्बन्ध में विस्तार से कहा है।' अवधूत साधक का जिस प्रकार का विवेचन भागवत में प्राया है, जैसा मज्झिमनिकाय में बुद्ध के तपश्चरण का वर्णन है, उसी विधा का संस्पर्श करता हुआ वर्णन जैन आगमों में भी प्राप्त होता है। जैन आगमों में प्राचारांगसूत्र का सर्वाधिक महत्त्व है / वह ऐतिहासिक तथा भाषाशास्त्रीय दृष्टि से सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। प्राचारांग के नवम अध्ययन में भगवान महावीर की चर्या का वर्णन है। जैसी कृच्छ साधना वे करते थे, वह वही साधक कर सकता है जो भौतिक सुख-सुविधा को मन से सर्वथा निकाल चुका हो, जिसके लिए शरीर बिल्कुल गौण हो गया हो, जो प्रात्मभाव में सम्पूर्णतः अपने को खोये हुए हो। भगवान् महावीर अपने साधना-मार्ग में आनेवाले भीषणतम विघ्नों, दु:सह बाधाओं और कष्टों को झेलते हुए मस्ती से अपने गन्तव्य की ओर गतिशील रहे। मनूष्यकृत, पशूकृत, इतरजीव-जन्तु-कीटाण-कृत उपसर्ग, जिनसे आदमी थर्रा उठता है, उनके लिए कुछ भी नहीं थे। एक ऐसा नितान्त आत्मजनीन जीवन, जिसमें लोकजनीनता का भाव अत्यन्त तिरोहित था, स्वीकार किये अपनी साधना में उत्तरोत्तर प्रगति करते गये / कठोरतम क्लेशों के प्रति उपेक्षाभाव तथा लोकसंग्रह एवं लोकानुकूल्य के प्रति संपूर्ण औदासीन्य, परकृत तिरस्कार और अवहेलना से सर्वथा अप्रभावितता ये कुछ ऐसी बातें थीं, जिनका प्रवाह अवधूत-साधना से दूरवर्ती नहीं कहा जा सकता। आचारांग सूत्र के छठे अध्ययन का नाम 'धूताध्ययन' है। अवधूत पद में 'धूत' शब्द है ही। जैसा पहले इसका अर्थ किया गया है, अवधूत वह है, जो आत्मा के विजातीय भाव को अथवा भोगलिप्सा, वासना, तृष्णा एवं आसक्ति को संपूर्णत: कंपा दे, हिला दे, डगमगा दे। बौद्धचर्या में भी धूतांगों के नाम से विसुद्धिमग्ग आदि में विवेचन है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो प्रतीत होता है, इन दोनों ही परंपरामों में कभी अवधूत शब्द गृहीत रहा हो, जो आगे चलकर प्रयत्न-लाघव आदि के कारण संक्षिप्तीकरण की दष्टि से 'अव' उपसर्ग को हटाकर केवल धूत (धुत) ही रख लिया गया हो / अवधूत पद में मुख्य तो धूत शब्द ही है। भाषा-विज्ञान का यह प्रयत्न-लाघव-मूलक क्रम व्याकरण में भी दृष्टिगोचर होता है। 'एकशेष' समास में, जहाँ दो शब्द मिलकर 'समस्त पद बनाते हैं, समास के निष्पन्न होने पर एक हो शब्द अवशिष्ट रह जाता है, जो दोनों शब्दों का अभिप्राय व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ-भ्राता (भाई) और श्वसा (बहिन)-इन दोनों का समास करने पर 'भ्रातरौ' मात्र रहेगा / वैसे साधारण 1. मज्झिमनिकाय, महासोहनादसुत्तन्त 1.2.2 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org