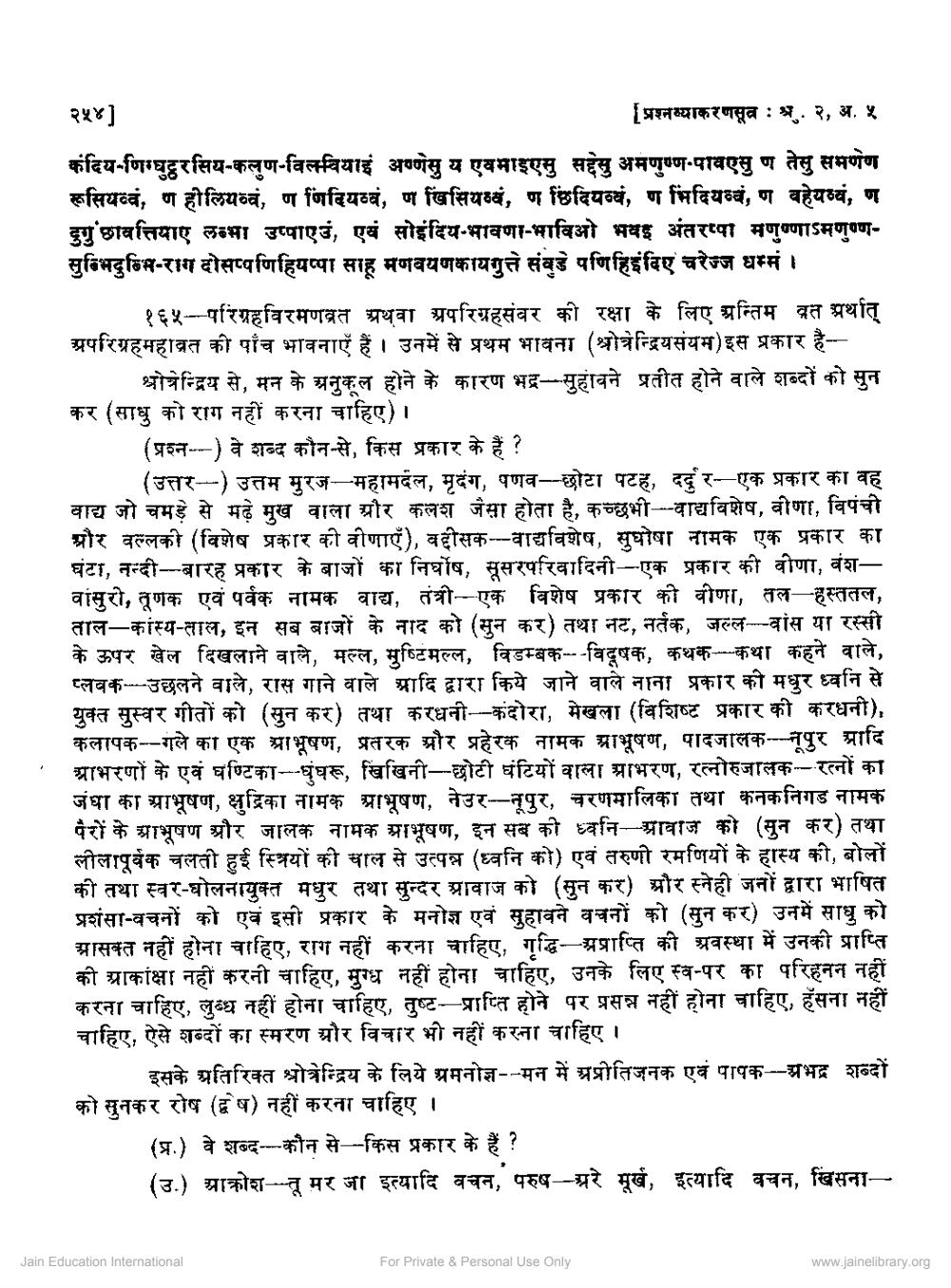________________ 254] [प्रश्नव्याकरणसूत्र : श्रु. 2, अ. 5 कंदिय-णिग्घुटुरसिय-कलुण-विलवियाई अण्णेसु य एवमाइएसु सद्देसु अमणुण्ण-पावएसु ण तेसु समणेण रूसियव्वं, ण हीलियब्वं, ण णिदियव्वं, ण खिसियग्वं, णछिदियग्वं, ण भिदियब्वं, ण बहेयव्वं, ग दुगुछावत्तियाए लम्भा उप्पाएउं, एवं सोइंदिय-भावणा-भाविओ भवइ अंतरप्पा मणुण्णाऽमणुण्णसुभिदुम्मि-राग दोसप्पणिहियप्पा साहू मणवयणकायगुत्ते संवुडे पणिहिइंदिए चरेज्ज धम्म / १६५---परिग्रहविरमणवत अथवा अपरिग्रहसंबर की रक्षा के लिए अन्तिम व्रत अर्थात् अपरिग्रहमहाव्रत की पाँच भावनाएँ हैं। उनमें से प्रथम भावना (श्रोत्रेन्द्रियसंयम) इस प्रकार है श्रोत्रेन्द्रिय से, मन के अनुकूल होने के कारण भद्र-सुहावने प्रतीत होने वाले शब्दों को सुन कर (साधु को राग नहीं करना चाहिए)। (प्रश्न---) वे शब्द कौन-से, किस प्रकार के हैं ? (उत्तर--) उत्तम मुरज-महामर्दल, मृदंग, पणव-छोटा पटह, दर्दुर-एक प्रकार का वह वाद्य जो चमड़े से मढ़े मुख वाला और कलश जैसा होता है, कच्छभी--वाद्यविशेष, बीणा, विपंची और वल्लकी (विशेष प्रकार की वीणाएँ), बद्दीसक-वाद्यविशेष, सुघोषा नामक एक प्रकार का घंटा, नन्दी-बारह प्रकार के बाजों का निर्घोष, सूसरपरिवादिनी-एक प्रकार की वीणा, वंशवांसुरी, तूणक एवं पर्वक नामक वाद्य, तंत्री-एक विशेष प्रकार की वीणा, तल–हस्ततल, ताल-कास्य-ताल, इन सब बाजों के नाद को (सुन कर) तथा नट, नर्तक, जल्ल-वांस या रस्सी के ऊपर खेल दिखलाने वाले, मल्ल, मुष्टिमल्ल, विडम्बक---विदूषक, कथक कथा कहने वाले, प्लवक-उछलने वाले, रास गाने वाले आदि द्वारा किये जाने वाले नाना प्रकार की मधुर ध्वनि से युक्त सुस्वर गीतों को (सुन कर) तथा करधनी-कंदोरा, मेखला (विशिष्ट प्रकार की करधनी), कलापक-गले का एक आभूषण, प्रतरक और प्रहेरक नामक आभूषण, पादजालक-नूपुर आदि आभरणों के एवं घण्टिका-धुंघरू, खिखिनी-छोटी घंटियों वाला पाभरण, रत्नोरुजालक-रत्नों का जंघा का आभूषण, क्षुद्रिका नामक आभूषण, नेउर-नूपुर, चरणमालिका तथा कनकनिगड नामक पैरों के आभूषण और जालक नामक ग्राभूषण, इन सब की ध्वनि-आवाज को (सुन कर) तथा लीलापूर्वक चलती हुई स्त्रियों की चाल से उत्पन्न (ध्वनि को) एवं तरुणी रमणियों के हास्य की, बोलों की तथा स्वर-घोलनायुक्त मधुर तथा सुन्दर अावाज को (सुन कर) और स्नेही जनों द्वारा भाषित प्रशंसा-वचनों को एवं इसी प्रकार के मनोज्ञ एवं सुहावने वचनों को (सुन कर) उनमें साधु को आसक्त नहीं होना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, गृद्धि-अप्राप्ति की अवस्था में उनकी प्राप्ति की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, मुग्ध नहीं होना चाहिए, उनके लिए स्व-पर का परिहनन नहीं करना चाहिए, लुब्ध नहीं होना चाहिए, तुष्ट-प्राप्ति होने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हँसना नहीं चाहिए, ऐसे शब्दों का स्मरण और विचार भी नहीं करना चाहिए / इसके अतिरिक्त श्रोत्रेन्द्रिय के लिये अमनोज्ञ--मन में अप्रीतिजनक एवं पापक-अभद्र शब्दों को सुनकर रोष (द्वेष) नहीं करना चाहिए / (प्र.) वे शब्द--कौन से-किस प्रकार के हैं ? (उ.) आक्रोश-तू मर जा इत्यादि वचन, परुष-अरे मूर्ख, इत्यादि वचन, खिसना Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org