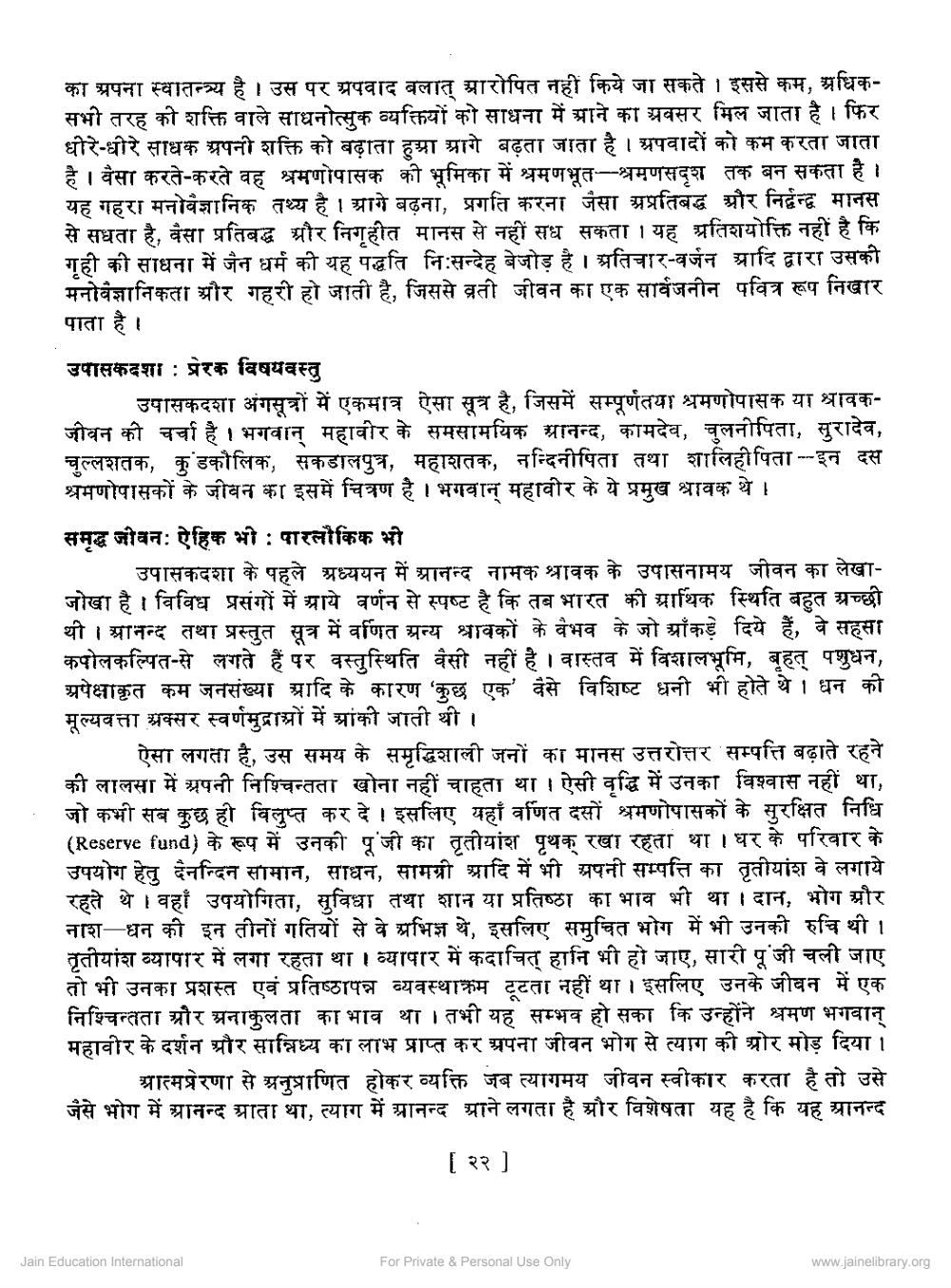________________ का अपना स्वातन्त्र्य है। उस पर अपवाद बलात् आरोपित नहीं किये जा सकते / इससे कम, अधिकसभी तरह की शक्ति वाले साधनोत्सुक व्यक्तियों को साधना में आने का अवसर मिल जाता है / फिर धीरे-धीरे साधक अपनी शक्ति को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता जाता है / अपवादों को कम करता जाता है / वैसा करते-करते वह श्रमणोपासक की भूमिका में श्रमणभूत-श्रमणसदृश तक बन सकता है / यह गहरा मनोवैज्ञानिक तथ्य है / आगे बढ़ना, प्रगति करना जैसा अप्रतिबद्ध और निर्द्वन्द्वः मानस से सधता है, वैसा प्रतिबद्ध और निगृहीत मानस से नहीं सध सकता / यह अतिशयोक्ति नहीं है कि गृही की साधना में जैन धर्म की यह पद्धति निःसन्देह बेजोड़ है / अतिचार-वर्जन आदि द्वारा उसकी मनोवैज्ञानिकता और गहरी हो जाती है, जिससे व्रती जीवन का एक सार्वजनीन पवित्र रूप निखार पाता है। उपासकदशा : प्रेरक विषयवस्तु उपासकदशा अंगसूत्रों में एकमात्र ऐसा सूत्र है, जिसमें सम्पूर्णतया श्रमणोपासक या श्रावकजीवन की चर्चा है / भगवान महावीर के समसामयिक आनन्द, कामदेव, चुलनीपिता, सुरादेव, चुल्लशतक, कुडकौलिक, सकडालपुत्र, महाशतक, नन्दिनीपिता तथा शालिहीपिता--इन दस श्रमणोपासकों के जीवन का इसमें चित्रण है / भगवान् महावीर के ये प्रमुख श्रावक थे। समृद्ध जीवन: ऐहिक भी : पारलौकिक भी उपासकदशा के पहले अध्ययन में आनन्द नामक श्रावक के उपासनामय जीवन का लेखाजोखा है। विविध प्रसंगों में पाये वर्णन से स्पष्ट है कि तब भारत की प्राथिक स्थिति हुत अच्छी थी। आनन्द तथा प्रस्तुत सूत्र में वर्णित अन्य श्रावकों के वैभव के जो आँकड़े दिये हैं, वे सहसा कपोलकल्पित-से लगते हैं पर वस्तुस्थिति वैसी नहीं है / वास्तव में विशालभूमि, बृहत् पशुधन, अपेक्षाकृत कम जनसंख्या आदि के कारण 'कुछ एक' वैसे विशिष्ट धनी भी होते थे। धन की मूल्यवत्ता अक्सर स्वर्णमुद्राओं में की जाती थी। ऐसा लगता है, उस समय के समृद्धिशाली जनों का मानस उत्तरोत्तर सम्पत्ति बढ़ाते रहने की लालसा में अपनी निश्चिन्तता खोना नहीं चाहता था / ऐसी वद्धि में उनका विश्वास नहीं था, जो कभी सब कुछ ही विलुप्त कर दे / इसलिए यहाँ वणित दसों श्रमणोपासकों के सुरक्षित निधि (Reserve fund) के रूप में उनकी पूजी का तृतीयांश पृथक रखा रहता था। घर के परिवार के उपयोग हेतु दैनन्दिन सामान, साधन, सामग्री आदि में भी अपनी सम्पत्ति का तृतीयांश वे लगाये रहते थे। वहाँ उपयोगिता, सुविधा तथा शान या प्रतिष्ठा का भाव भी था / दान, भोग और नाश-धन की इन तीनों गतियों से वे अभिज्ञ थे, इसलिए समुचित भोग में भी उनकी रुचि थी। तृतीयांश व्यापार में लगा रहता था / व्यापार में कदाचित् हानि भी हो जाए, सारी पूजी चली जाए तो भी उनका प्रशस्त एवं प्रतिष्ठापन्न व्यवस्थाक्रम टूटता नहीं था। इसलिए उनके जीवन में एक निश्चितता और अनाकलता का भाव था। तभी यह सम्भव हो सका कि उन्होंने श्रमण भगवान महावीर के दर्शन और सान्निध्य का लाभ प्राप्त कर अपना जीवन भोग से त्याग की ओर मोड़ दिया। आत्मप्रेरणा से अनुप्राणित होकर व्यक्ति जब त्यागमय जीवन स्वीकार करता है तो उसे जैसे भोग में अानन्द प्राता था. त्याग में आनन्द आने लगता है और विशेषता यह है कि यह प्रानन्द [ 22 ] Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org