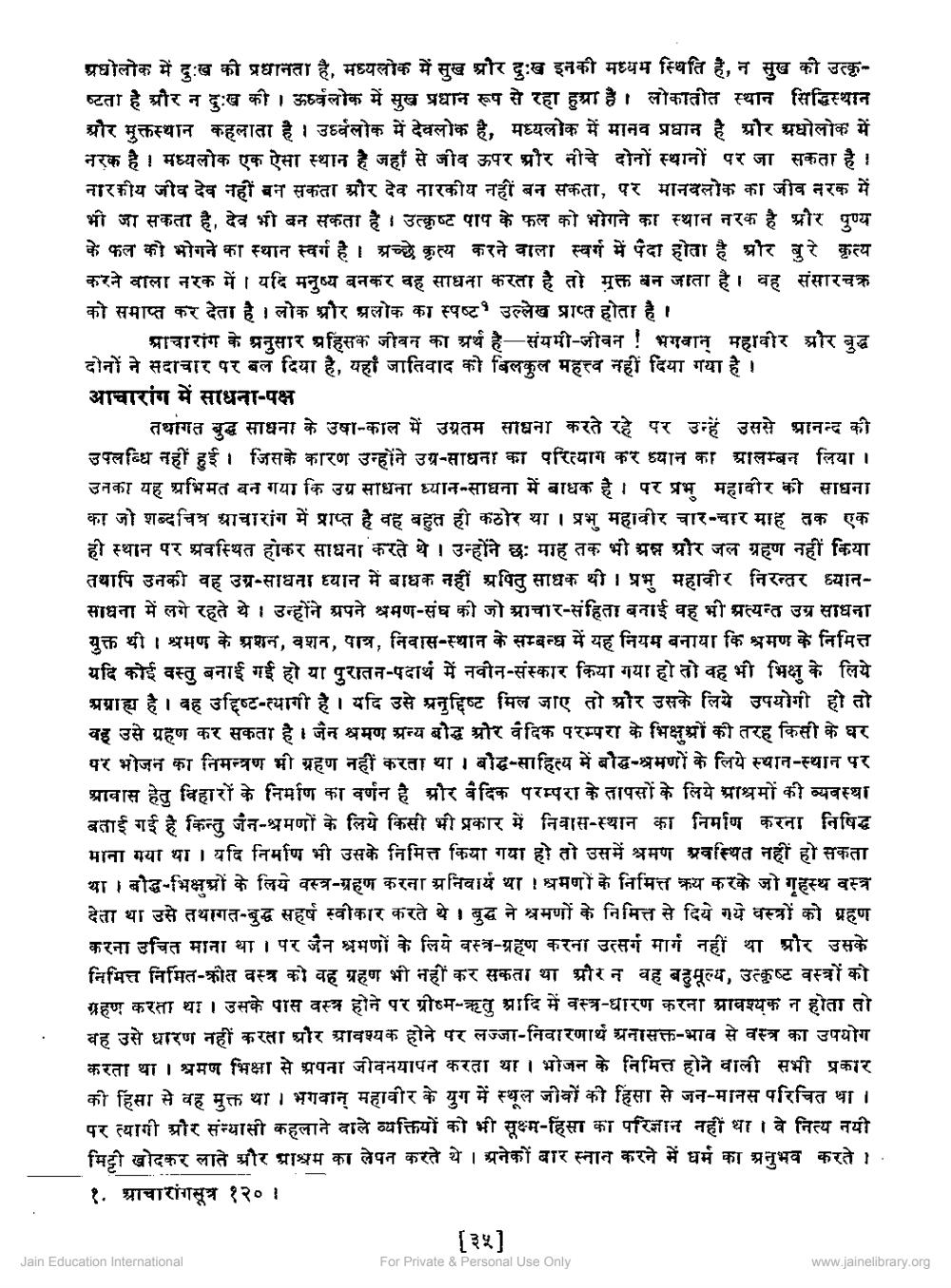________________ अधोलोक में दुःख की प्रधानता है, मध्यलोक में सुख और दुःख इनकी मध्यम स्थिति है, न सुख को उत्कृष्टता है और न दुःख की। ऊर्वलोक में सुख प्रधान रूप से रहा हुआ है। लोकातीत स्थान सिद्धिस्थान और मुक्तस्थान कहलाता है। उर्बलोक में देवलोक है, मध्यलोक में मानव प्रधान है और अधोलोक में नरक है। मध्यलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ से जीव ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर जा सकता है। नारकीय जीव देव नहीं बन सकता और देव नारकीय नहीं बन सकता, पर मानवलोक का जीव नरक में भी जा सकता है, देव भी बन सकता है। उत्कृष्ट पाप के फल को भोगने का स्थान नरक है और पुण्य के फल को भोगने का स्थान स्वर्ग है। अच्छे कृत्य करने वाला स्वर्ग में पैदा होता है और बुरे कृत्य करने वाला नरक में / यदि मनुष्य बनकर वह साधना करता है तो मुक्त बन जाता है। वह संसारचक्र को समाप्त कर देता है। लोक और अलोक का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। प्राचारांग के अनुसार अहिंसक जीवन का अर्थ है-संयमी-जीवन ! भगवान महावीर और बुद्ध दोनों ने सदाचार पर बल दिया है, यहां जातिवाद को बिलकुल महत्त्व नहीं दिया गया है। आचारांग में साधना-पक्ष तथागत बुद्ध साधना के उषा-काल में उग्रतम साधना करते रहे पर उन्हें उससे प्रानन्द की उपलब्धि नहीं हुई। जिसके कारण उन्होंने उग्र-साधना का परित्याग कर ध्यान का पालम्बन लिया। उनका यह अभिमत बन गया कि उग्र साधना ध्यान-साधना में बाधक है। पर प्रभु महावीर की साधना का जो शब्दचित्र प्राचारांग में प्राप्त है वह बहुत ही कठोर था / प्रभु महावीर चार-चार माह तक एक ही स्थान पर अवस्थित होकर साधना करते थे। उन्होंने छ: माह तक भी अन्न और जल ग्रहण नहीं किया तथापि उनकी वह उग्र-साधना ध्यान में बाधक नहीं अपितु साधक थी। प्रभु महावीर निरन्तर ध्यानसाधना में लगे रहते थे। उन्होंने अपने श्रमण-संघ को जो आचार-संहिता बनाई वह भी अत्यन्त उग्र साधना युक्त थी। श्रमण के प्रशन, वशन, पात्र, निवास स्थान के सम्बन्ध में यह नियम बनाया कि श्रमण के निमित्त यदि कोई वस्तु बनाई गई हो या पुरातन-पदार्थ में नवीन-संस्कार किया गया हो तो वह भी भिक्षु के लिये अग्राह्य है / वह उद्दिष्ट-त्यागी है / यदि उसे अनुद्दिष्ट मिल जाए तो और उसके लिये उपयोगी हो तो वह उसे ग्रहण कर सकता है। जैन श्रमण अन्य बौद्ध और वैदिक परम्परा के भिक्षुओं की तरह किसी के घर पर भोजन का निमन्त्रण भी ग्रहण नहीं करता था। बौद्ध-साहित्य में बौद्ध-श्रमणों के लिये स्थान-स्थान पर प्रावास हेतु विहारों के निर्माण का वर्णन है और वैदिक परम्परा के तापसों के लिये पाश्रमों की व्यवस्था बताई गई है किन्तु जैन-श्रमणों के लिये किसी भी प्रकार में निवास स्थान का निर्माण करना निषिद्ध माना गया था। यदि निर्माण भी उसके निमित्त किया गया हो तो उसमें श्रमण अवस्थित नहीं हो सकता था। बौद्ध भिक्षत्रों के लिये वस्त्र-ग्रहण करना अनिवार्य था / श्रमणों के निमित्त क्रय करके जो गृहस्थ वस्त्र देता था उसे तथागत-बुद्ध सहर्ष स्वीकार करते थे। बुद्ध ने श्रमणों के निमित्त से दिये गये वस्त्रों को ग्रहण करना उचित माना था। पर जैन श्रमणों के लिये वस्त्र-ग्रहण करना उत्सर्ग मार्ग नहीं था और उसके निमित्त निमित-क्रीत वस्त्र को वह ग्रहण भी नहीं कर सकता था और न वह बहुमूल्य, उत्कृष्ट वस्त्रों को ग्रहण करता था। उसके पास वस्त्र होने पर ग्रीष्म ऋतु आदि में वस्त्र-धारण करना आवश्यक न होता तो वह उसे धारण नहीं करता और आवश्यक होने पर लज्जा-निवारणार्थ अनासक्त-भाव से वस्त्र का उपयोग करता था। श्रमण भिक्षा से अपना जीवनयापन करता था। भोजन के निमित्त होने वाली सभी प्रकार की हिंसा से वह मुक्त था। भगवान महावीर के युग में स्थल जीवों की हिंसा से जन-मानस परिचित था। पर त्यागी और संन्यासी कहलाने वाले व्यक्तियों को भी सूक्ष्म-हिंसा का परिज्ञान नहीं था। वे नित्य नयी मिट्री खोदकर लाते और प्राश्रम का लेपन करते थे / अनेकों बार स्नान करने में धर्म का अनुभव करते। . 1. प्राचारांगसूत्र 120 / Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org