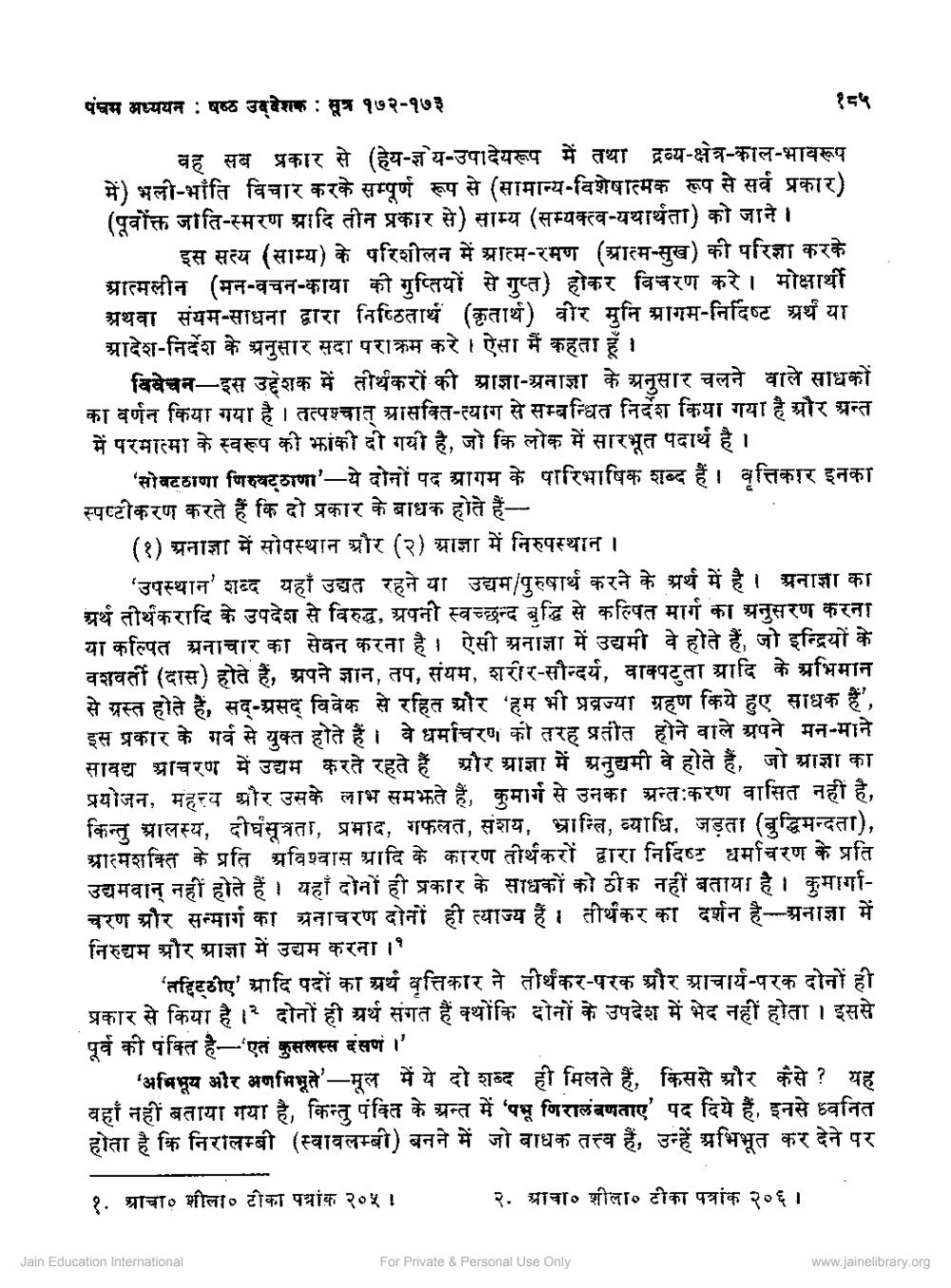________________ पंचम अध्ययन : षष्ठ उद्देशक : सूत्र 172-173 185 वह सब प्रकार से (हेय-ज्ञय-उपादेयरूप में तथा द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप में) भली-भांति विचार करके सम्पूर्ण रूप से (सामान्य-विशेषात्मक रूप से सर्व प्रकार) (पूर्वोक्त जाति-स्मरण आदि तीन प्रकार से) साम्य (सम्यक्त्व-यथार्थता) को जाने / इस सत्य (साम्य) के परिशीलन में आत्म-रमण (आत्म-सुख) की परिज्ञा करके आत्मलीन (मन-वचन-काया की गुप्तियों से गुप्त) होकर विचरण करे। मोक्षार्थी अथवा संयम-साधना द्वारा निष्ठितार्थ (कृतार्थ) वीर मुनि आगम-निर्दिष्ट अर्थ या आदेश-निर्देश के अनुसार सदा पराक्रम करे / ऐसा मैं कहता हूँ। विवेचन-इस उद्देशक में तीर्थंकरों की आज्ञा-अनाज्ञा के अनुसार चलने वाले साधकों का वर्णन किया गया है / तत्पश्चात् आसक्ति-त्याग से सम्बन्धित निर्देश किया गया है और अन्त में परमात्मा के स्वरूप की झांकी दी गयी है, जो कि लोक में सारभूत पदार्थ है। _ 'सोवटठाणा णिस्वट्ठाणा'-ये दोनों पद आगम के पारिभाषिक शब्द हैं। वृत्तिकार इनका स्पष्टीकरण करते हैं कि दो प्रकार के बाधक होते हैं (1) अनाज्ञा में सोपस्थान और (2) आज्ञा में निरुपस्थान / 'उपस्थान' शब्द यहाँ उद्यत रहने या उद्यम पुरुषार्थ करने के अर्थ में है। अनाज्ञा का अर्थ तीर्थंकरादि के उपदेश से विरुद्ध, अपनी स्वच्छन्द बुद्धि से कल्पित मार्ग का अनुसरण करना या कल्पित अनाचार का सेवन करना है। ऐसी अनाज्ञा में उद्यमी वे होते हैं, जो इन्द्रियों के वशवर्ती (दास) होते हैं, अपने ज्ञान, तप, संयम, शरीर-सौन्दर्य, वाक्पटुता आदि के अभिमान से ग्रस्त होते हैं, सद्-असद् विवेक से रहित और हम भी प्रव्रज्या ग्रहण किये हुए साधक हैं', इस प्रकार के गर्व से युक्त होते हैं। वे धर्माचरण की तरह प्रतीत होने वाले अपने मन-माने सावध आचरण में उद्यम करते रहते हैं और आज्ञा में अनुद्यमी वे होते हैं, जो आज्ञा का प्रयोजन, महत्व और उसके लाभ समझते हैं, कुमार्ग से उनका अन्तःकरण वासित नहीं है, किन्तु पालस्य, दीर्घसूत्रता, प्रमाद, गफलत, संशय, भ्रान्ति, व्याधि, जड़ता (बुद्धिमन्दता), प्रात्मशक्ति के प्रति अविश्वास आदि के कारण तीर्थकरों द्वारा निर्दिष्ट धर्माचरण के प्रति उद्यमवान् नहीं होते हैं। यहाँ दोनों ही प्रकार के साधकों को ठीक नहीं बताया है। कुमार्गाचरण और सन्मार्ग का अनाचरण दोनों ही त्याज्य हैं। तीर्थंकर का दर्शन है-अनाज्ञा में निरुद्यम और प्राज्ञा में उद्यम करना।' तहिटठीए' आदि पदों का अर्थ वृत्तिकार ने तीर्थंकर-परक और प्राचार्य-परक दोनों ही प्रकार से किया है। दोनों ही अर्थ संगत हैं क्योंकि दोनों के उपदेश में भेद नहीं होता। इससे पूर्व की पंक्ति है—'एतं कुसलस्स दसणं / ' 'अभिभूय और अभिभूते'-मूल में ये दो शब्द ही मिलते हैं, किससे और कैसे ? यह वहाँ नहीं बताया गया है, किन्तु पंक्ति के अन्त में 'पभूणिरालंबणताए' पद दिये हैं, इनसे ध्वनित होता है कि निरालम्बी (स्वावलम्बी) बनने में जो बाधक तत्त्व हैं, उन्हें अभिभूत कर देने पर 1. प्राचा० शीला० टीका पत्रांक 205 ! 2. आचा० शीला० टीका पत्रांक 206 / Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org