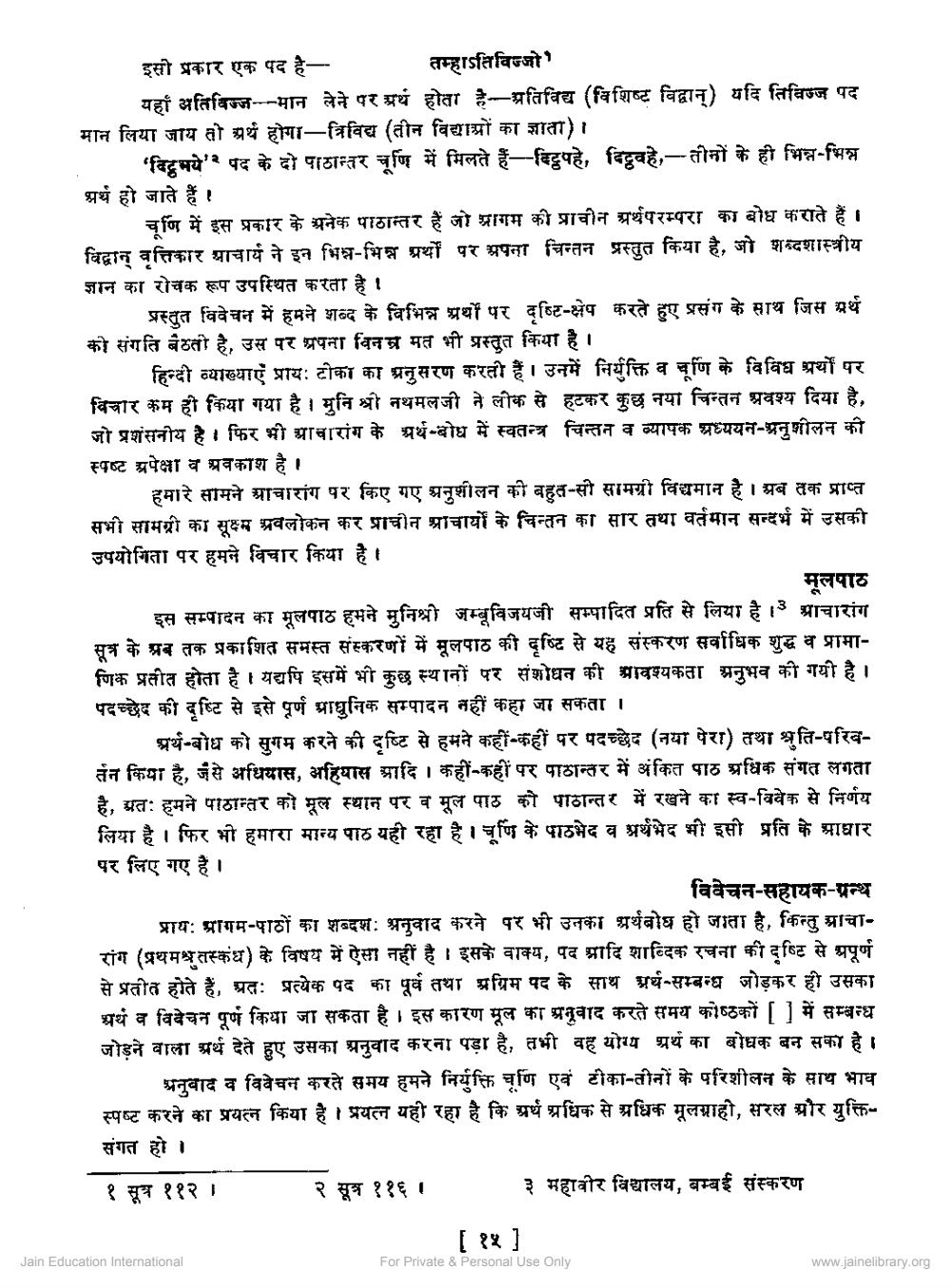________________ इसी प्रकार एक पद है तम्हाऽतिविज्जो' यहाँ अतिविज्ज---मान लेने पर अर्थ होता है-अतिविद्य (विशिष्ट विद्वान्) यदि तिविज्ज पद मान लिया जाय तो अर्थ होगा-त्रिविद्य (तीन विद्याओं का ज्ञाता)। 'विटुभये पद के दो पाठान्तर चूणि में मिलते हैं-विट्ठपहे, दिद्ववहे,-तीनों के ही भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं। चूणि में इस प्रकार के अनेक पाठान्तर हैं जो आगम की प्राचीन अर्थपरम्परा का बोध कराते हैं / विद्वान् वृत्तिकार प्राचार्य ने इन भिन्न-भिन्न अर्थों पर अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है, जो शब्दशास्त्रीय ज्ञान का रोचक रूप उपस्थित करता है। प्रस्तुत विवेचन में हमने शब्द के विभिन्न अर्थों पर दृष्टि-क्षेप करते हुए प्रसंग के साथ जिस अर्थ को संगति बैठती है, उस पर अपना विनम्र मत भी प्रस्तुत किया है। हिन्दी व्याख्याएँ प्रायः टोका का अनुसरण करती हैं। उनमें नियुक्ति व चूणि के विविध अर्थों पर विचार कम ही किया गया है। मुनि श्री नथमलजी ने लीक से हटकर कुछ नया चिन्तन अवश्य दिया है, जो प्रशंसनीय है। फिर भी आचारांग के अर्थ-बोध में स्वतन्त्र चिन्तन व व्यापक अध्ययन-अनुशीलन की स्पष्ट अपेक्षा व अवकाश है। हमारे सामने आचारांग पर किए गए अनुशीलन की बहत-सी सामग्री विद्यमान है। अब तक प्राप्त सभी सामग्री का सूक्ष्म अवलोकन कर प्राचीन प्राचार्यों के चिन्तन का सार तथा वर्तमान सन्दर्भ में उसकी उपयोगिता पर हमने विचार किया है। मूलपाठ इस सम्पादन का मूलपाठ हमने मुनिश्री जम्बूविजयजी सम्पादित प्रति से लिया है। प्राचारांग सूत्र के अब तक प्रकाशित समस्त संस्करणों में मूलपाठ की दृष्टि से यह संस्करण सर्वाधिक शुद्ध व प्रामाणिक प्रतीत होता है / यद्यपि इसमें भी कुछ स्थानों पर संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गयी है। पदच्छेद की दृष्टि से इसे पूर्ण आधुनिक सम्पादन नहीं कहा जा सकता / अर्थ-बोध को सुगम करने की दृष्टि से हमने कहीं-कहीं पर पदच्छेद (नया पेरा) तथा श्रुति-परिवतन किया है, जैसे अधियास, अहियास आदि / कहीं-कहीं पर पाठान्तर में अंकित पाठ अधिक संगत लगता है, अतः हमने पाठान्तर को मूल स्थान पर व मूल पाठ को पाठान्तर में रखने का स्व-विवेक से निर्णय लिया है / फिर भी हमारा मान्य पाठ यही रहा है / चूणि के पाठभेद व अर्थभेद भी इसी प्रति के आधार पर लिए गए है। विवेचन-सहायक-ग्रन्थ प्राय: प्रागम-पाठों का शब्दश: अनुवाद करने पर भी उनका अर्थबोध हो जाता है, किन्तु प्राचारांग (प्रथमश्रुतस्कंध) के विषय में ऐसा नहीं है / इसके वाक्य, पद प्रादि शाब्दिक रचना की दृष्टि से अपूर्ण से प्रतीत होते हैं, अतः प्रत्येक पद का पूर्व तथा अग्रिम पद के साथ अर्थ-सम्बन्ध जोड़कर ही उसका अर्थ व विवेचन पूर्ण किया जा सकता है / इस कारण मूल का अनुवाद करते समय कोष्ठकों [ ] में सम्बन्ध जोड़ने वाला अर्थ देते हुए उसका अनुवाद करना पड़ा है, तभी वह योग्य अर्थ का बोधक बन सका है। अनुवाद व विवेचन करते समय हमने नियुक्ति चूणि एवं टीका-तीनों के परिशीलन के साथ भाव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है / प्रयत्न यही रहा है कि अर्थ अधिक से अधिक मूलग्राही, सरल और युक्तिसंगत हो। 1 सूत्र 112 / 2 सूत्र 116 / 3 महावीर विद्यालय, बम्बई संस्करण [15] Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org