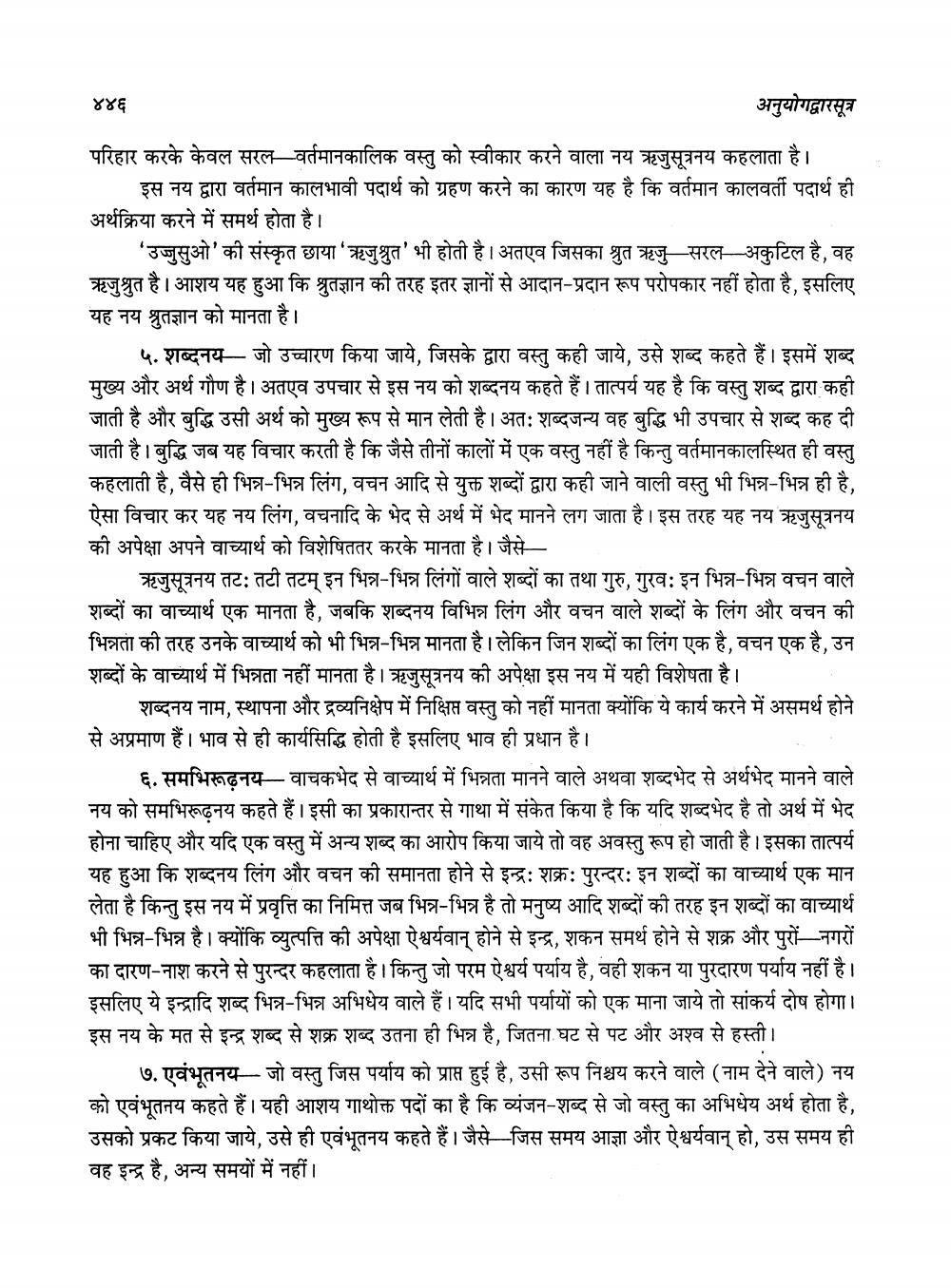________________
४४६
अनुयोगद्वारसूत्र
परिहार करके केवल सरल वर्तमानकालिक वस्तु को स्वीकार करने वाला नय ऋजुसूत्रनय कहलाता है।
इस नय द्वारा वर्तमान कालभावी पदार्थ को ग्रहण करने का कारण यह है कि वर्तमान कालवर्ती पदार्थ ही अर्थक्रिया करने में समर्थ होता है।
__ 'उज्जुसुओ' की संस्कृत छाया 'ऋजुश्रुत' भी होती है। अतएव जिसका श्रुत ऋजु सरल—अकुटिल है, वह ऋजुश्रुत है। आशय यह हुआ कि श्रुतज्ञान की तरह इतर ज्ञानों से आदान-प्रदान रूप परोपकार नहीं होता है, इसलिए यह नय श्रुतज्ञान को मानता है।
५.शब्दनय— जो उच्चारण किया जाये, जिसके द्वारा वस्तु कही जाये, उसे शब्द कहते हैं। इसमें शब्द मुख्य और अर्थ गौण है। अतएव उपचार से इस नय को शब्दनय कहते हैं। तात्पर्य यह है कि वस्तु शब्द द्वारा कही जाती है और बुद्धि उसी अर्थ को मुख्य रूप से मान लेती है। अतः शब्दजन्य वह बुद्धि भी उपचार से शब्द कह दी जाती है। बुद्धि जब यह विचार करती है कि जैसे तीनों कालों में एक वस्तु नहीं है किन्तु वर्तमानकालस्थित ही वस्तु कहलाती है, वैसे ही भिन्न-भिन्न लिंग, वचन आदि से युक्त शब्दों द्वारा कही जाने वाली वस्तु भी भिन्न-भिन्न ही है, ऐसा विचार कर यह नय लिंग, वचनादि के भेद से अर्थ में भेद मानने लग जाता है। इस तरह यह नय ऋजुसूत्रनय की अपेक्षा अपने वाच्यार्थ को विशेषिततर करके मानता है। जैसे
ऋजुसूत्रनय तटः तटी तटम् इन भिन्न-भिन्न लिंगों वाले शब्दों का तथा गुरु, गुरवः इन भिन्न-भिन्न वचन वाले शब्दों का वाच्यार्थ एक मानता है, जबकि शब्दनय विभिन्न लिंग और वचन वाले शब्दों के लिंग और वचन की भिन्नता की तरह उनके वाच्यार्थ को भी भिन्न-भिन्न मानता है। लेकिन जिन शब्दों का लिंग एक है, वचन एक है, उन शब्दों के वाच्यार्थ में भिन्नता नहीं मानता है। ऋजुसूत्रनय की अपेक्षा इस नय में यही विशेषता है।
शब्दनय नाम, स्थापना और द्रव्यनिक्षेप में निक्षिप्त वस्तु को नहीं मानता क्योंकि ये कार्य करने में असमर्थ होने से अप्रमाण हैं। भाव से ही कार्यसिद्धि होती है इसलिए भाव ही प्रधान है।
६. समभिरूढ़नय— वाचकभेद से वाच्यार्थ में भिन्नता मानने वाले अथवा शब्दभेद से अर्थभेद मानने वाले नय को समभिरूढ़नय कहते हैं। इसी का प्रकारान्तर से गाथा में संकेत किया है कि यदि शब्दभेद है तो अर्थ में भेद होना चाहिए और यदि एक वस्तु में अन्य शब्द का आरोप किया जाये तो वह अवस्तु रूप हो जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शब्दनय लिंग और वचन की समानता होने से इन्द्रः शक्रः पुरन्दरः इन शब्दों का वाच्यार्थ एक मान लेता है किन्तु इस नय में प्रवृत्ति का निमित्त जब भिन्न-भिन्न है तो मनुष्य आदि शब्दों की तरह इन शब्दों का वाच्यार्थ भी भिन्न-भिन्न है। क्योंकि व्युत्पत्ति की अपेक्षा ऐश्वर्यवान् होने से इन्द्र, शकन समर्थ होने से शक्र और पुरों—नगरों का दारण-नाश करने से पुरन्दर कहलाता है। किन्तु जो परम ऐश्वर्य पर्याय है, वही शकन या पुरदारण पर्याय नहीं है। इसलिए ये इन्द्रादि शब्द भिन्न-भिन्न अभिधेय वाले हैं। यदि सभी पर्यायों को एक माना जाये तो सांकर्य दोष होगा। इस नय के मत से इन्द्र शब्द से शक्र शब्द उतना ही भिन्न है, जितना घट से पट और अश्व से हस्ती।
७. एवंभूतनय— जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है, उसी रूप निश्चय करने वाले (नाम देने वाले) नय को एवंभूतनय कहते हैं। यही आशय गाथोक्त पदों का है कि व्यंजन-शब्द से जो वस्तु का अभिधेय अर्थ होता है, उसको प्रकट किया जाये, उसे ही एवंभूतनय कहते हैं। जैसे—जिस समय आज्ञा और ऐश्वर्यवान् हो, उस समय ही वह इन्द्र है, अन्य समयों में नहीं।